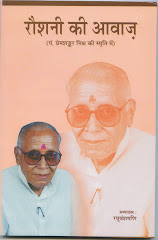डायरी
एक बहादुर युवती की याद
मैं उस युवती को पूरी तरह से भूल चुका था। यदि शिमला जाते वक्त दिल्ली से कालका जाने वाली कालका शताब्दि ट्रेन में वह अखबार न मिला होता तो फिर याद भी न आती। कैसा दुखद है कि हम उन्हें भूल जाते हैं जो अच्छे काम करते हैं। मीडिया भी उन्हें कभी भूले भटके ही याद करता है।
तो वह अखबार था सेक्टर न्यूज और वह अखबार भी सिर्फ चण्डीगढ़ में वितरित होने वाला पाक्षिक। इसमें सूचना थी कि नीरजा भनोत सम्मान चन्दा असानी को दिया गया है। यहीं नीरजा भनोत की याद स्मृति में कौंध गयी जिसने भारत के अपहृत विमान से तमाम लोंगो को बचाया था और अन्त में दो बच्चों को बचाते हुए स्वयं अपहर्ताओं की गोलियों का शिकार हो गयी थीं। यह घटना 1986 की है। और नीरजा को अपने इस वीरता और साहस भरे कारनामें के लिए मरणोंपरांत अशोक चक्र दिया गया था।
भारत के विमान को चार सशस्त्र आतंकियों ने अपहृत कर लिया था। 17 घंटे के तनाव भरे माहौल के बाद अपहरणकर्ताओं ने गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं थी। नीरजा भनोत ने साहस और बुध्दिमत्ता का परिचय देते हुए विमान का आपातकालीन द्वार खोल दिया था जिससे बहुत से यात्री बच निकले थे। मगर अंत में दो बच्चों की जान बचाने में नीरजा दिवंत हुई। वे भारत की पहली महिला थ्ीं जिन्हे अशोक चक्र दिया गया था। यही नहीं पाकिस्तान की ओर से उन्हें तमगा-ए-इन्सानियत दिया गया था। अपनी वीरगति के समय नीरजा भनोत की उम्र 23 साल थी।
31.10.2008
Tuesday, December 09, 2008
Saturday, December 06, 2008
कविता का परिवेश
कविता का परिवेश
रघुवंशमणि
जिस दौर में आज हम कविता की चर्चा कर रहे हैं वह सापेक्षित दृश्टि से तेज परिवर्तनों का समय है। जो परिवर्तन पहले सौ-पचास सालों में होते थे अब वे दो-चार सालों में सम्पन्न हो जाते हैं। आज हम जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रह रहे हैं, शयद उसकी कल्पना हम स्वयं 1970 के आसपास नहीं कर सकते थे। तकनीकी के तीव्र विकास ने जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये है। 1970 के आसपास गॉवों तक ट्रांजिस्टर/रेडियो की भी पहॅुंच नहीं थी। आज वहीं पर विभिन्न मीडियारूप अपने विभिन्न लुभावने रूप-रंगों के साथ पहुँचे हुए हैं। सूचना क्रान्ति ने लोगों को छपे शब्दों के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे साधन दिये हैं जिनकें द्वारा अभिव्यक्ति और संप्रेशण संभव हुए हैं। ऐसे में निष्चित रूप से कवित की हमारे समय में अवस्थिति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। यह मुद्दा हमें स्वाभाविक रूप से कविता की भूमिका से लेकर, कविता की आलोचना और मूल्यांकन के प्रष्नों तक ले जायेगा।
प्रत्येक काल में लोग अपने समय में होने वाले परिवर्तनों के प्रति इस प्रकार की बातें करते रहे हैं। प्रेमचन्द ने भी अपने समय में हो रहे सापेक्षिक रूप से तेज परिवर्तनों की बात की थी। हर युग के विचारषील लोगों को अपना समय पिछले कालों से अधिक तेज परिवर्तनों वाला लगा है। लेकिन यह एक तथ्य है कि विगत बीस-तीस वर्शों में ही परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं कि पिछले समय से गहरा अलगाव महसूस हो। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है इसके भौतिक प्रमाण मौजूद हैं। रेडियो, ट्रांजिस्टर से टी.वी., आकाषीय चैनल, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, टेलीफोन की भौतिक उपस्थिति इसके कुछ प्रमाण है। पारंपरिक मीडियारूपों में भी रूपगत परिवर्तन स्पश्टत: दृश्टिगोचर हुए है। इसी कारण हमारे इस दौर के परिवर्तनों को अभूतपूर्व कहा जा रहा है। यह बात दीगर कि आने वाले समय में परिवर्तन और भी तेज हों, और हमारे बाद की पीढ़ी को हमारा ही समय पिछड़ा हुआ लगे। यह भी संभव है कि ये परिवर्तन किसी ऐसी दिषा मेें फैले कि जीवन षैली पर इसका सीधा प्रभाव कम रहे और आने वाला जीवन इतनी उथल-पुथल से न भरा हो। कुछ लोग इस दौर को संरचनात्मक समायोजन के संक्रमण काल के रूप में भी देखते हैं जिसमें परिवर्तन तेज गति से होते हैं। इस संरचनात्मक समायोजन के बाद संभवत: इस परिवर्तन की गति थोड़ा मंद हो।
फिलहाल विभिन्न मीडिया रूपों मेें कविता क्ी उपस्थिति का सवाल काफी परेषान करने वाला हो सकता है। विषेशकर यदि हम उस पारंपरिक रूमानी सोच के तहत कविता पर विचार करना प्रारंभ करें जिनके तहत कवि, ' भावी का द्रश्टा' और 'विप्लव का स्रश्टा' होता था; या जो 'षाष्वत मूल्यों' की सृश्टि करता था, अथवा जिसके पास 'ईष्वरीय षक्ति' या 'प्रतिभा' होती थी जो पूर्व संस्कारों से प्राप्त होती थी। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को इस प्रकार के भ्रम न होंगे। तथापि 1970 के दशक में कविता की भूमिका की तुलना में यदि आज की कविता को रखें तो यह भूमिका घटी हुई ही लगेगी। कविता के पाठकों की घटती हुई संख्या निरंतर चिन्ता का विशय बनी रही है। इसी सापेक्ष कविता का प्रभावक्षेत्र भी सीमित हुआ है।
कविता को यदि 'मुफलिसों की अंजुमन' तक न भी पहुंचाया जा सके तो उसे कम से कम 'पढ़ी लिखी जनता' तक तो पहुंचाया ही जाना चाहिए। मगर सवाल यह है कि कविता का माध्यम क्या है? कविता स्वयं तो अपना माध्यम होती नहीं। कविता को यथाषक्ति पाठकों तक पहॅुंचाने का कार्य लघु पत्रिकाओं ने ही किया है। मगर हिन्दी के प्रकाशकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं क्योंकि वे अक्सर लाभ के अर्थषास्त्र के चलते कविताओं को पाठकों तक पहुँचाने के बजाय पुस्ताकालयों तक पहुंचाते हैं। डॉ. मैनेजर पाण्डेय ने ठीक ही कहा है कि हिन्दी के प्रकाशक वास्तव में हिन्दी के अंधकारक हैं। इधर हिन्दी कवियों के कविता संग्रहों के संस्करणों की प्रतियाँ भी काफी कम होती गयीं है। कुछ संग्रहों के प्रकाशन संस्करण 500 प्रतियों तक भी सीमित रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हिन्दी में कविताओं के पाठक कई कारणों के चलते कम हुए हैं।
मेरे एक मित्र अक्सर पूछते हैं कि यदि समकालीन हिन्दी कविता का मामला कुछ हजार लोगोें तक ही सीमित है तो फिर उसे लेकर ज्यादा उछल-कूद करने की क्या जरूरत? अगर कविता क्षेत्र में उठने वाले विवाद कुछ ही लोगों तक सीमित है तो फिर उसे ज्यादा महत्व क्यों दिया जाय? कविता को लेकर उठने वाले और उठाये जाने वाले इस प्रकार के प्रष्न अक्सर सिनिकल/नकारात्मक तरीके से सामने आते हैं और उन पर अंग्रेजी की एक कहावत के अनुसार टब के पानी के साथ-साथ बच्चे को भी फेंक देने का आरोप लगाया जायेगा क्योंकि कविता के पाठक कितनें भी कम क्यों न हुए हों, वह चर्चा का विशय बनी रहती है। समाज के एक संकुल में ही क्यों न सही वह गंभीरतापूर्वक समझी जाती है। लेकिन इस तर्क को कविता के पक्ष में आत्ममुग्ध तरीके से या 'संतोशधन' के रूप में नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए।
कविता की इस भौतिक स्थिति के प्रति चिन्ता ऐसा नहीं है कि हिन्दी जगत में व्यक्त नहीं हुई । आलोचकों में तो यह चर्चा रही ही, इसके प्रति कवियों में भी एक सजगता दिखाई देती है। अश्टभुजा षुक्ल और संजय चतुर्वेदी जैसे कवियों ने अपना रास्ता बदलकर नयी षैली अपनायी जो जनसामान्य के लिए ग्राह्य हो। जनगीतों के मार्ग तो प्रषस्त ही रहे। नयी कविता की कठिन और दुर्भेद्य षैली की तुलना मे समकालीन हिन्दी कविता सरलता की ओर बढ़ी है। अज्ञेयवादियों की षैली की तुलना में आज की कविता की षैली काफी सरल है। मगर कविता से कम सम्पर्क रखने वाले लोगों में कविता की कठिनाई का मिथक लगातार बना हुआ है। इसका एक बड़ा कारण यही है कि कविता को पढ़ी-लिखी हिन्दी जनता तक व्यापक रूप से पहुंचाने का कोई प्रभावी और व्यापक माध्यम नहीं है। कविता को जनता तक पहुंचा सकने वाले मंचों का अभाव है। इन प्रष्नों के खड़े होने पर हमेषा एक नवजागरण्ा की माँग की जाती है और हिन्दी जनता को कोसा जाता है। लेखक संघों और साहित्यिक संस्थाओं की गंभीर भागीदारी हो सकती है। जनसंस्कृति मंच के कुछ कवियों ने 'युध्द के विरुध्द कविता' के तहत कुछ समयपूर्व ऐसा प्रयास किया था जो सफल भी था। कई अवसरों पर कविता को लेकर जब भी जनता में जाना पड़ा है तो देखा गया है कि उसका प्रभाव अब भी काफी है। कविता को जनता के बीच ले जाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत है।
(2)
कविता के लिए जैसी भी भौतिक परिस्थितियां हैं उन्हीं के तहत समकालीन हिन्दी कविता को देखना होगा। कविता का यह भौतिक यथार्थ कविता की भूमिका के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। हिन्दी कविता कम लोग पढ़ते हैं इस तथ्य से ही कविता की सीमा को निर्धारित करना फिर भी खतरनाक होगा। कविता के लक्ष्य पाठकों की चर्चा में भी यह तथ्य नहीं भुलाया जाना चाहिए कि कविता के पेषेवर आलोचकों और नियमित पाठकों के अतिरिक्त एक यादृच्छिक पाठक वर्ग भी रहता है जो हमेषा महत्वपूर्ण होता है। फिर मुक्तिबोध के जनता के साहित्य के बारे में व्यक्त यह विचार नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जनता के बारे में लिखा गया साहित्य भी जनता का ही साहित्य है।
इन सारे द्वन्द्वों के बीच मुख्यधारा की कविता की बात बिडम्बनापूर्ण लगती है क्योंकि समकालीन हिन्दी कविता स्वयं मुख्यधारा से अलग हैं। मुख्यधारा में तो फिल्मी गीत, ग़जलें और बाजारू संगीत आयेगा जिसका धन्धा अभी भी लाभप्रद है। हिन्दी में कविता लिखकर यष:प्रार्थी तो हुआ जा सकता है पर धनपषु नहीं। समकालीन हिन्दी कविता (जैसा कि बार-बार कहा जाता रहा है) प्रतिरोध और विकल्पों की कविता है और विकल्पों की यह तलाष जारी रहनी चाहिए क्योंकि इन विकल्पों के ठोस, सार्थक और परिवर्तनकारी रूप अभी समाज/संस्कृति में दिखलाई नहीं पड़ते। समकालीन हिन्दी कविता विभिन्न संस्तरों पर लिखी जा रही है और विभिन्नताएं ऐसी हैं कि किसी भी आलोचक को परेषानी में डाल दे। ये कविताएँ अपने वर्चस्व विरोध और सत्ताा प्रतिरोध मे ही अपनी इयत्ताा तलाषती है। पूरी कविता के लिए किया गया सामान्यीकरण 'समकालीन' स्वयं में तमाम तत्वों का एक समुच्च है जिसे पारिभाशित करने में सैकड़ों पन्ने काले किये जा चुके है। यहाँ यदि कई पीढ़ियाँ एक साथ सृजनरत हैं तो एक ही पीढ़ी के कई कवि कई-कई तरह से लिख रहे हैं। इसलिए मुख्यधारा का कोई भी सवाल अपने जवाब मे बेहद सामान्यीकृत और भोथड़ा होगा। उम्रदराज होते कवियों जैसे उदय प्रकाश, स्वप्निल श्रीवास्तव, ज्ञानेन्द्रपति, राजेश जोषी और विनोद कुमार षुक्ल मे ही समानता की तलाश कितनी कठिन होगी।
समकालीन हिन्दी कविता का यही वह यथार्थ है जो आलोचकों के लिए एक चुनौती बनता है। कवि की अपनी अवस्थिति कविता मे अन्तर करने योग्य तत्व पैदा कर देती है। गुजरात के दंगों पर राजेश जोषी, देवी प्रसाद मिश्र और विश्णु खरे की कविताएं अपना अलग-अलग स्वभाव रखती है। यहीं पर देवीषंकर अवस्थी का यह कथन सार्थक होता है कि कविता को समाजषास्त्र या राजनीति की ही दृश्टि से नहीं देखा जाना चाहिए-उसका अन्तर्ग्रथन भी अध्ययन की विशयवस्तु है। हिन्दी आलोचना पर ऐसा न करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता । समकालीन हिन्दी कविता की इसी विभिन्नता के चलते आलोचक अपना 'स्टांस' बदलते रहते है।
अक्सर विचार-विमर्ष के दौरान 'मुख्यधारा' पद द्वारा वामपंथ के साहित्य की ओर संकेत होता है। हिन्दी कविता के सन्दर्भ मेंं भी 'मुख्यधारा' पद का यह एक अभिप्रेत हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह इंगित करना जरूरी होगा कि समकालीन हिन्दी कविता को किसी 'वाद' के तहत हो रही कविता नही कहा जा सकता । यह बात दीगर की उद्देष्य की एकता के चलते समानताएँ दिखाई दे सकती है। सरोकार एक जैसे होने पर कविताओं की दिषा एक जैसी हो जाती है। अभी कुछ वर्श पहले 'सहमत' द्वारा प्रकाषित असद जैदी द्वारा सम्पादित 'दस बरस' का संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें अषोक वाजपेयी से लेकर कुंवर नारायण तक की कविताएँ थीं जो स्वयं को वामपंथी कहना पसंद नहीं करेंगे। कुल मिलाकर यह एक प्रजातांत्रिक सहयोग ही है जिसमें तमाम दिषाओं और विचारों के कवि सरोकारों की एकता के चलते एक स्थान पर खडे दिखाई देते हैं। समकालीन हिन्दी कविता से जुड़े इस तथ्य को साम्प्रदायिकता विरोधी हिन्दी कविता के प्रसंग में प्रमाणित किया जा सकता है।
फिर भी इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि आज की हिन्दी कविता अतिषय राजनीतिक है और यह उसकी पहचान का एक प्रमुख तत्व है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में हिन्दी कविता कभी भी इतनी राजनीतिक नहीं थी जितनी की आज है। ऐसे में किसी एक राजनीतिक विचार को (वामपंथ) को मुख्यधारा मानकर कलंकित करना एक तरह का हिन्दुस्तानी मैकार्थीवाद होगा जो कोई स्वस्थ प्रजातांत्रिक बात नही। हिन्दू पुनरुत्थान के दौर मे इस प्रकार की सेंसरषिप के भगवे प्रयास हो चुके ही। यह बताना जरूरी नहीं कि ये सभी प्रयास फासीवाद के ही रूप रहे हैं।
साम्प्रदायिकता के उभार का हिन्दी कविता पर गहरा असर पड़ा। साम्प्रदायिकता विरोधी कविता साम्प्रदायिक फासीवाद के उभार के दौर में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाषित हुई और कुछ पत्रिकाओं ने समय-समय पर इन कविताओं को विषेशरूप से स्थान दिया। चन्दौसी से प्रकाषित होनी वाली पत्रिका 'परिवेष' ने 1992 के बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद अपना साम्प्रदायिता विरोधी अंक ही प्रकाषित किया। इसके बाद से कई पत्रिकाओं ने साम्प्रदायिता विरोधी कविताओं को विषेशरूप से स्थान दिया। इन कविताओं से गुजरते हुए हम हिन्दी कविता में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित कर सकते है। दिसम्बर 1992 से पहले और उसके बाद लिखी गयी तमाम कविताएँ परिवर्तन के दो तथ्यों की ओर संकेत करती है। एक तो यह कि जो कवि पहले से कविताएँ लिख रहे थे उन्होंने साम्प्रदायिकता के प्रष्न को अपने लिए महत्वपूर्ण माना और उन्होंने इस विशय पर प्रमुखता से कविताएँ लिखीं। दूसरा यह कि नये उभरते कवियों ने इस विशय को तत्काल अपनी विशयवस्तु के रूप में चुना। ये कवि इस दौर की उपज थे या थोड़ा पहले से लिख रहे थे। इस क्षोभकारी घटना और इससे जुड़ी साम्प्रदायिक हिंसा ने दोनों पीढ़ियों के कवियों की संवेदना को गहराई से झकझोरा । हिन्दी की समकालीन कविता मे यही वह बिन्दु है जहाँ हम एक विषिश्ट प्रकार के मानववाद की वापसी देख सकते हैं। यह मानववाद, साम्प्रदायिकता का विरोध करने में व्यापक जमीन की प्राप्ति के लिए बना। राजनीति में यदि यह धर्मनिरपेक्ष षक्तियों के ढीले-ढाले गठजोड़ के रूप में दिखायी दिया तो साहित्य में हम इसे मानवीय भूमि पर समेकित होते देख सकते हैं। अषोक वाजपेयी जैसे साहित्य के स्वराज की बात करने वालों से लेकर अतिवाम समर्थकों तक ने इस मुद्दे पर लिखना जरूरी समझा।
(3)
भूमण्डलीकरण और बाजारवाद के विरोध मे हिन्दी मे बहुत सी कविताएँ लिखी गयीं मगर कविता पर उन दोनों आर्थिक परिवर्तनों का कैसा प्रभाव पड़ा यह देखना बाकी है। भूमण्डलीकरण और बाजारवाद ने जिस प्रकार के व्यवसायवाद को बढ़ावा दिया है उसका प्रभाव अब हिन्दी साहित्य पर स्पश्ट परिलक्षित होने लगा है। मूल्यों और नैतिकताओं के स्थान पर अब आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत सम्बन्ध अधिक महत्वपूर्ण हो गये है। सर्जनात्मकता में विष्वास कम और सफलता की सीढ़ियों पर विष्वास अधिक बढ़ा है। पुरस्कार लोभ, व्यक्तिगत राजनीति और जोड़-तोड़ ने हिन्दी कविता जगत मे भी दम मारा है। बाजारवाद के दौर में अवसरवाद तेजी से बढ़ा है। कविता धन तो नहीं मगर यष कमाने का एक आसान जरिया नज़र आने लगी है। इस सन्दर्भ में मैं अपने मित्र अश्टभुजा षुक्ल के एक महत्वपूर्ण लेख 'काव्यम् यशसे' की ओर इंगित करना चाहूंगा जो जयपुर से प्रकाषित होने वाली पत्रिका 'कृतिओर' में छपी थी।
भूमण्डलीकरण और बाजारवाद की एक विषेशता यह भी है कि वह जहाँ भी अवतरित होता है जनान्दोलनों को कमजोर करता है, उन्हें नश्ट करता है। इनके नीच प्रवाह में पतित लोग मूल्यों और विचारों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रचालित होते हैं। हिन्दी कविता में कैरियरिज्म की प्रछन्न प्रवृत्तिा बढ़ती लग रही है जो कि बेहत खतरनाक है। कविता के मूल्यांकन मेें इस ओर आलोचक की दृश्टि जानी ही चाहिए। उत्तार संरचनावादी कृति और कृतिकार को अलग-अलग करके देखने की बात करते हैं और इस सिलसिले में रोलाबार्थ के निबन्ध 'डेथ ऑफ आथर' में व्यक्त विचार सिध्दान्त सूत्र बने।
रोलांबार्थ अपने निबन्ध 'द डेथ ऑफ आथर' में पाठ के लिए लेखक की अनावष्यकता का जिक्र करते हैं और भाशा को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन एक ही समय मे एक ही प्रकार की भाशा में लिखी जा रही रचनाओं की वैचारिक अवस्थितियाँ कैसे निर्धारित होगी यदि रचनाकार के अस्तित्व से इंकार कर दिया जाय। हिन्दी जगत में अभी हम इतने इतिहास विहीन या स्मृतिविहीन नहीं है। समकालीन कविता में रचनाकार के जीवन और उसकी कविता के सम्बन्धों मे प्रामाणिकता की प्राप्ति होगी। इस अर्थ मे हमें रचनाकार को पुनर्जीवित करना पड़ेगा।
साहित्य के इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जब रचनाकार के जीवन ने उनकी कृतियों के अर्थ बदल दिये हैं। रचनाकार का जीवन किस प्रकार उसके साहित्य के मूल्यांकन के लिए एक प्रकार की कसौटी बनता है इसके उदाहरण्ा निराला, मुक्तिबोध जैसे कवि हैं। निराला की महाप्राणता उनके जीवन और कृतित्व दोनों के चलते है। मुक्तिबोध की विपन्नता में भी जाग्रत उनके स्व कें षब्द हमारी आत्मा के गुप्त स्वर्णाक्षर बन चुके है। क्या एजरा पाउण्ड और विन्डहम लीविस को पढ़ते समय उनके फासीवादी जुड़ावों को भुलाया जा सकेगा? पॉल डी मान के अपने सम्बन्ध उनकी आलोचना के छद्मों की पोल खोल देते हैं। क्या अटल विहारी वाजपेयी की कविताओं का मूल्यांकन करते समय यह भुलाया जा सकेगा कि उन्हीं के प्रधानमंत्रित्वकाल में गुजरात के भयानक दंगे हुए जिसका उन्होंने समय रहते षमन नहीं किया?
आज के इच्छाधारी साहित्य और साहित्यकारों के दौर में मेरी बातें कुछ लोगों को थोड़ा पुरानी और घिसी-पिटी लग सकती है। उन लोगों के लिए वीरेन डंगवाल की ये पक्तियाँ छोड़ रहा हूँ।
''मजे का बखत है तो इसमें हैरानी क्या है?
हमें भी कैलेन द्यो कुछ मज्जा परेसानी क्या?''
'कुछ कद्दू चमकाये मैंने'
रघुवंशमणि
जिस दौर में आज हम कविता की चर्चा कर रहे हैं वह सापेक्षित दृश्टि से तेज परिवर्तनों का समय है। जो परिवर्तन पहले सौ-पचास सालों में होते थे अब वे दो-चार सालों में सम्पन्न हो जाते हैं। आज हम जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रह रहे हैं, शयद उसकी कल्पना हम स्वयं 1970 के आसपास नहीं कर सकते थे। तकनीकी के तीव्र विकास ने जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये है। 1970 के आसपास गॉवों तक ट्रांजिस्टर/रेडियो की भी पहॅुंच नहीं थी। आज वहीं पर विभिन्न मीडियारूप अपने विभिन्न लुभावने रूप-रंगों के साथ पहुँचे हुए हैं। सूचना क्रान्ति ने लोगों को छपे शब्दों के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे साधन दिये हैं जिनकें द्वारा अभिव्यक्ति और संप्रेशण संभव हुए हैं। ऐसे में निष्चित रूप से कवित की हमारे समय में अवस्थिति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। यह मुद्दा हमें स्वाभाविक रूप से कविता की भूमिका से लेकर, कविता की आलोचना और मूल्यांकन के प्रष्नों तक ले जायेगा।
प्रत्येक काल में लोग अपने समय में होने वाले परिवर्तनों के प्रति इस प्रकार की बातें करते रहे हैं। प्रेमचन्द ने भी अपने समय में हो रहे सापेक्षिक रूप से तेज परिवर्तनों की बात की थी। हर युग के विचारषील लोगों को अपना समय पिछले कालों से अधिक तेज परिवर्तनों वाला लगा है। लेकिन यह एक तथ्य है कि विगत बीस-तीस वर्शों में ही परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं कि पिछले समय से गहरा अलगाव महसूस हो। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है इसके भौतिक प्रमाण मौजूद हैं। रेडियो, ट्रांजिस्टर से टी.वी., आकाषीय चैनल, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, टेलीफोन की भौतिक उपस्थिति इसके कुछ प्रमाण है। पारंपरिक मीडियारूपों में भी रूपगत परिवर्तन स्पश्टत: दृश्टिगोचर हुए है। इसी कारण हमारे इस दौर के परिवर्तनों को अभूतपूर्व कहा जा रहा है। यह बात दीगर कि आने वाले समय में परिवर्तन और भी तेज हों, और हमारे बाद की पीढ़ी को हमारा ही समय पिछड़ा हुआ लगे। यह भी संभव है कि ये परिवर्तन किसी ऐसी दिषा मेें फैले कि जीवन षैली पर इसका सीधा प्रभाव कम रहे और आने वाला जीवन इतनी उथल-पुथल से न भरा हो। कुछ लोग इस दौर को संरचनात्मक समायोजन के संक्रमण काल के रूप में भी देखते हैं जिसमें परिवर्तन तेज गति से होते हैं। इस संरचनात्मक समायोजन के बाद संभवत: इस परिवर्तन की गति थोड़ा मंद हो।
फिलहाल विभिन्न मीडिया रूपों मेें कविता क्ी उपस्थिति का सवाल काफी परेषान करने वाला हो सकता है। विषेशकर यदि हम उस पारंपरिक रूमानी सोच के तहत कविता पर विचार करना प्रारंभ करें जिनके तहत कवि, ' भावी का द्रश्टा' और 'विप्लव का स्रश्टा' होता था; या जो 'षाष्वत मूल्यों' की सृश्टि करता था, अथवा जिसके पास 'ईष्वरीय षक्ति' या 'प्रतिभा' होती थी जो पूर्व संस्कारों से प्राप्त होती थी। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को इस प्रकार के भ्रम न होंगे। तथापि 1970 के दशक में कविता की भूमिका की तुलना में यदि आज की कविता को रखें तो यह भूमिका घटी हुई ही लगेगी। कविता के पाठकों की घटती हुई संख्या निरंतर चिन्ता का विशय बनी रही है। इसी सापेक्ष कविता का प्रभावक्षेत्र भी सीमित हुआ है।
कविता को यदि 'मुफलिसों की अंजुमन' तक न भी पहुंचाया जा सके तो उसे कम से कम 'पढ़ी लिखी जनता' तक तो पहुंचाया ही जाना चाहिए। मगर सवाल यह है कि कविता का माध्यम क्या है? कविता स्वयं तो अपना माध्यम होती नहीं। कविता को यथाषक्ति पाठकों तक पहॅुंचाने का कार्य लघु पत्रिकाओं ने ही किया है। मगर हिन्दी के प्रकाशकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं क्योंकि वे अक्सर लाभ के अर्थषास्त्र के चलते कविताओं को पाठकों तक पहुँचाने के बजाय पुस्ताकालयों तक पहुंचाते हैं। डॉ. मैनेजर पाण्डेय ने ठीक ही कहा है कि हिन्दी के प्रकाशक वास्तव में हिन्दी के अंधकारक हैं। इधर हिन्दी कवियों के कविता संग्रहों के संस्करणों की प्रतियाँ भी काफी कम होती गयीं है। कुछ संग्रहों के प्रकाशन संस्करण 500 प्रतियों तक भी सीमित रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हिन्दी में कविताओं के पाठक कई कारणों के चलते कम हुए हैं।
मेरे एक मित्र अक्सर पूछते हैं कि यदि समकालीन हिन्दी कविता का मामला कुछ हजार लोगोें तक ही सीमित है तो फिर उसे लेकर ज्यादा उछल-कूद करने की क्या जरूरत? अगर कविता क्षेत्र में उठने वाले विवाद कुछ ही लोगों तक सीमित है तो फिर उसे ज्यादा महत्व क्यों दिया जाय? कविता को लेकर उठने वाले और उठाये जाने वाले इस प्रकार के प्रष्न अक्सर सिनिकल/नकारात्मक तरीके से सामने आते हैं और उन पर अंग्रेजी की एक कहावत के अनुसार टब के पानी के साथ-साथ बच्चे को भी फेंक देने का आरोप लगाया जायेगा क्योंकि कविता के पाठक कितनें भी कम क्यों न हुए हों, वह चर्चा का विशय बनी रहती है। समाज के एक संकुल में ही क्यों न सही वह गंभीरतापूर्वक समझी जाती है। लेकिन इस तर्क को कविता के पक्ष में आत्ममुग्ध तरीके से या 'संतोशधन' के रूप में नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए।
कविता की इस भौतिक स्थिति के प्रति चिन्ता ऐसा नहीं है कि हिन्दी जगत में व्यक्त नहीं हुई । आलोचकों में तो यह चर्चा रही ही, इसके प्रति कवियों में भी एक सजगता दिखाई देती है। अश्टभुजा षुक्ल और संजय चतुर्वेदी जैसे कवियों ने अपना रास्ता बदलकर नयी षैली अपनायी जो जनसामान्य के लिए ग्राह्य हो। जनगीतों के मार्ग तो प्रषस्त ही रहे। नयी कविता की कठिन और दुर्भेद्य षैली की तुलना मे समकालीन हिन्दी कविता सरलता की ओर बढ़ी है। अज्ञेयवादियों की षैली की तुलना में आज की कविता की षैली काफी सरल है। मगर कविता से कम सम्पर्क रखने वाले लोगों में कविता की कठिनाई का मिथक लगातार बना हुआ है। इसका एक बड़ा कारण यही है कि कविता को पढ़ी-लिखी हिन्दी जनता तक व्यापक रूप से पहुंचाने का कोई प्रभावी और व्यापक माध्यम नहीं है। कविता को जनता तक पहुंचा सकने वाले मंचों का अभाव है। इन प्रष्नों के खड़े होने पर हमेषा एक नवजागरण्ा की माँग की जाती है और हिन्दी जनता को कोसा जाता है। लेखक संघों और साहित्यिक संस्थाओं की गंभीर भागीदारी हो सकती है। जनसंस्कृति मंच के कुछ कवियों ने 'युध्द के विरुध्द कविता' के तहत कुछ समयपूर्व ऐसा प्रयास किया था जो सफल भी था। कई अवसरों पर कविता को लेकर जब भी जनता में जाना पड़ा है तो देखा गया है कि उसका प्रभाव अब भी काफी है। कविता को जनता के बीच ले जाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत है।
(2)
कविता के लिए जैसी भी भौतिक परिस्थितियां हैं उन्हीं के तहत समकालीन हिन्दी कविता को देखना होगा। कविता का यह भौतिक यथार्थ कविता की भूमिका के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। हिन्दी कविता कम लोग पढ़ते हैं इस तथ्य से ही कविता की सीमा को निर्धारित करना फिर भी खतरनाक होगा। कविता के लक्ष्य पाठकों की चर्चा में भी यह तथ्य नहीं भुलाया जाना चाहिए कि कविता के पेषेवर आलोचकों और नियमित पाठकों के अतिरिक्त एक यादृच्छिक पाठक वर्ग भी रहता है जो हमेषा महत्वपूर्ण होता है। फिर मुक्तिबोध के जनता के साहित्य के बारे में व्यक्त यह विचार नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जनता के बारे में लिखा गया साहित्य भी जनता का ही साहित्य है।
इन सारे द्वन्द्वों के बीच मुख्यधारा की कविता की बात बिडम्बनापूर्ण लगती है क्योंकि समकालीन हिन्दी कविता स्वयं मुख्यधारा से अलग हैं। मुख्यधारा में तो फिल्मी गीत, ग़जलें और बाजारू संगीत आयेगा जिसका धन्धा अभी भी लाभप्रद है। हिन्दी में कविता लिखकर यष:प्रार्थी तो हुआ जा सकता है पर धनपषु नहीं। समकालीन हिन्दी कविता (जैसा कि बार-बार कहा जाता रहा है) प्रतिरोध और विकल्पों की कविता है और विकल्पों की यह तलाष जारी रहनी चाहिए क्योंकि इन विकल्पों के ठोस, सार्थक और परिवर्तनकारी रूप अभी समाज/संस्कृति में दिखलाई नहीं पड़ते। समकालीन हिन्दी कविता विभिन्न संस्तरों पर लिखी जा रही है और विभिन्नताएं ऐसी हैं कि किसी भी आलोचक को परेषानी में डाल दे। ये कविताएँ अपने वर्चस्व विरोध और सत्ताा प्रतिरोध मे ही अपनी इयत्ताा तलाषती है। पूरी कविता के लिए किया गया सामान्यीकरण 'समकालीन' स्वयं में तमाम तत्वों का एक समुच्च है जिसे पारिभाशित करने में सैकड़ों पन्ने काले किये जा चुके है। यहाँ यदि कई पीढ़ियाँ एक साथ सृजनरत हैं तो एक ही पीढ़ी के कई कवि कई-कई तरह से लिख रहे हैं। इसलिए मुख्यधारा का कोई भी सवाल अपने जवाब मे बेहद सामान्यीकृत और भोथड़ा होगा। उम्रदराज होते कवियों जैसे उदय प्रकाश, स्वप्निल श्रीवास्तव, ज्ञानेन्द्रपति, राजेश जोषी और विनोद कुमार षुक्ल मे ही समानता की तलाश कितनी कठिन होगी।
समकालीन हिन्दी कविता का यही वह यथार्थ है जो आलोचकों के लिए एक चुनौती बनता है। कवि की अपनी अवस्थिति कविता मे अन्तर करने योग्य तत्व पैदा कर देती है। गुजरात के दंगों पर राजेश जोषी, देवी प्रसाद मिश्र और विश्णु खरे की कविताएं अपना अलग-अलग स्वभाव रखती है। यहीं पर देवीषंकर अवस्थी का यह कथन सार्थक होता है कि कविता को समाजषास्त्र या राजनीति की ही दृश्टि से नहीं देखा जाना चाहिए-उसका अन्तर्ग्रथन भी अध्ययन की विशयवस्तु है। हिन्दी आलोचना पर ऐसा न करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता । समकालीन हिन्दी कविता की इसी विभिन्नता के चलते आलोचक अपना 'स्टांस' बदलते रहते है।
अक्सर विचार-विमर्ष के दौरान 'मुख्यधारा' पद द्वारा वामपंथ के साहित्य की ओर संकेत होता है। हिन्दी कविता के सन्दर्भ मेंं भी 'मुख्यधारा' पद का यह एक अभिप्रेत हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह इंगित करना जरूरी होगा कि समकालीन हिन्दी कविता को किसी 'वाद' के तहत हो रही कविता नही कहा जा सकता । यह बात दीगर की उद्देष्य की एकता के चलते समानताएँ दिखाई दे सकती है। सरोकार एक जैसे होने पर कविताओं की दिषा एक जैसी हो जाती है। अभी कुछ वर्श पहले 'सहमत' द्वारा प्रकाषित असद जैदी द्वारा सम्पादित 'दस बरस' का संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें अषोक वाजपेयी से लेकर कुंवर नारायण तक की कविताएँ थीं जो स्वयं को वामपंथी कहना पसंद नहीं करेंगे। कुल मिलाकर यह एक प्रजातांत्रिक सहयोग ही है जिसमें तमाम दिषाओं और विचारों के कवि सरोकारों की एकता के चलते एक स्थान पर खडे दिखाई देते हैं। समकालीन हिन्दी कविता से जुड़े इस तथ्य को साम्प्रदायिकता विरोधी हिन्दी कविता के प्रसंग में प्रमाणित किया जा सकता है।
फिर भी इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि आज की हिन्दी कविता अतिषय राजनीतिक है और यह उसकी पहचान का एक प्रमुख तत्व है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में हिन्दी कविता कभी भी इतनी राजनीतिक नहीं थी जितनी की आज है। ऐसे में किसी एक राजनीतिक विचार को (वामपंथ) को मुख्यधारा मानकर कलंकित करना एक तरह का हिन्दुस्तानी मैकार्थीवाद होगा जो कोई स्वस्थ प्रजातांत्रिक बात नही। हिन्दू पुनरुत्थान के दौर मे इस प्रकार की सेंसरषिप के भगवे प्रयास हो चुके ही। यह बताना जरूरी नहीं कि ये सभी प्रयास फासीवाद के ही रूप रहे हैं।
साम्प्रदायिकता के उभार का हिन्दी कविता पर गहरा असर पड़ा। साम्प्रदायिकता विरोधी कविता साम्प्रदायिक फासीवाद के उभार के दौर में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाषित हुई और कुछ पत्रिकाओं ने समय-समय पर इन कविताओं को विषेशरूप से स्थान दिया। चन्दौसी से प्रकाषित होनी वाली पत्रिका 'परिवेष' ने 1992 के बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद अपना साम्प्रदायिता विरोधी अंक ही प्रकाषित किया। इसके बाद से कई पत्रिकाओं ने साम्प्रदायिता विरोधी कविताओं को विषेशरूप से स्थान दिया। इन कविताओं से गुजरते हुए हम हिन्दी कविता में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित कर सकते है। दिसम्बर 1992 से पहले और उसके बाद लिखी गयी तमाम कविताएँ परिवर्तन के दो तथ्यों की ओर संकेत करती है। एक तो यह कि जो कवि पहले से कविताएँ लिख रहे थे उन्होंने साम्प्रदायिकता के प्रष्न को अपने लिए महत्वपूर्ण माना और उन्होंने इस विशय पर प्रमुखता से कविताएँ लिखीं। दूसरा यह कि नये उभरते कवियों ने इस विशय को तत्काल अपनी विशयवस्तु के रूप में चुना। ये कवि इस दौर की उपज थे या थोड़ा पहले से लिख रहे थे। इस क्षोभकारी घटना और इससे जुड़ी साम्प्रदायिक हिंसा ने दोनों पीढ़ियों के कवियों की संवेदना को गहराई से झकझोरा । हिन्दी की समकालीन कविता मे यही वह बिन्दु है जहाँ हम एक विषिश्ट प्रकार के मानववाद की वापसी देख सकते हैं। यह मानववाद, साम्प्रदायिकता का विरोध करने में व्यापक जमीन की प्राप्ति के लिए बना। राजनीति में यदि यह धर्मनिरपेक्ष षक्तियों के ढीले-ढाले गठजोड़ के रूप में दिखायी दिया तो साहित्य में हम इसे मानवीय भूमि पर समेकित होते देख सकते हैं। अषोक वाजपेयी जैसे साहित्य के स्वराज की बात करने वालों से लेकर अतिवाम समर्थकों तक ने इस मुद्दे पर लिखना जरूरी समझा।
(3)
भूमण्डलीकरण और बाजारवाद के विरोध मे हिन्दी मे बहुत सी कविताएँ लिखी गयीं मगर कविता पर उन दोनों आर्थिक परिवर्तनों का कैसा प्रभाव पड़ा यह देखना बाकी है। भूमण्डलीकरण और बाजारवाद ने जिस प्रकार के व्यवसायवाद को बढ़ावा दिया है उसका प्रभाव अब हिन्दी साहित्य पर स्पश्ट परिलक्षित होने लगा है। मूल्यों और नैतिकताओं के स्थान पर अब आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत सम्बन्ध अधिक महत्वपूर्ण हो गये है। सर्जनात्मकता में विष्वास कम और सफलता की सीढ़ियों पर विष्वास अधिक बढ़ा है। पुरस्कार लोभ, व्यक्तिगत राजनीति और जोड़-तोड़ ने हिन्दी कविता जगत मे भी दम मारा है। बाजारवाद के दौर में अवसरवाद तेजी से बढ़ा है। कविता धन तो नहीं मगर यष कमाने का एक आसान जरिया नज़र आने लगी है। इस सन्दर्भ में मैं अपने मित्र अश्टभुजा षुक्ल के एक महत्वपूर्ण लेख 'काव्यम् यशसे' की ओर इंगित करना चाहूंगा जो जयपुर से प्रकाषित होने वाली पत्रिका 'कृतिओर' में छपी थी।
भूमण्डलीकरण और बाजारवाद की एक विषेशता यह भी है कि वह जहाँ भी अवतरित होता है जनान्दोलनों को कमजोर करता है, उन्हें नश्ट करता है। इनके नीच प्रवाह में पतित लोग मूल्यों और विचारों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रचालित होते हैं। हिन्दी कविता में कैरियरिज्म की प्रछन्न प्रवृत्तिा बढ़ती लग रही है जो कि बेहत खतरनाक है। कविता के मूल्यांकन मेें इस ओर आलोचक की दृश्टि जानी ही चाहिए। उत्तार संरचनावादी कृति और कृतिकार को अलग-अलग करके देखने की बात करते हैं और इस सिलसिले में रोलाबार्थ के निबन्ध 'डेथ ऑफ आथर' में व्यक्त विचार सिध्दान्त सूत्र बने।
रोलांबार्थ अपने निबन्ध 'द डेथ ऑफ आथर' में पाठ के लिए लेखक की अनावष्यकता का जिक्र करते हैं और भाशा को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन एक ही समय मे एक ही प्रकार की भाशा में लिखी जा रही रचनाओं की वैचारिक अवस्थितियाँ कैसे निर्धारित होगी यदि रचनाकार के अस्तित्व से इंकार कर दिया जाय। हिन्दी जगत में अभी हम इतने इतिहास विहीन या स्मृतिविहीन नहीं है। समकालीन कविता में रचनाकार के जीवन और उसकी कविता के सम्बन्धों मे प्रामाणिकता की प्राप्ति होगी। इस अर्थ मे हमें रचनाकार को पुनर्जीवित करना पड़ेगा।
साहित्य के इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जब रचनाकार के जीवन ने उनकी कृतियों के अर्थ बदल दिये हैं। रचनाकार का जीवन किस प्रकार उसके साहित्य के मूल्यांकन के लिए एक प्रकार की कसौटी बनता है इसके उदाहरण्ा निराला, मुक्तिबोध जैसे कवि हैं। निराला की महाप्राणता उनके जीवन और कृतित्व दोनों के चलते है। मुक्तिबोध की विपन्नता में भी जाग्रत उनके स्व कें षब्द हमारी आत्मा के गुप्त स्वर्णाक्षर बन चुके है। क्या एजरा पाउण्ड और विन्डहम लीविस को पढ़ते समय उनके फासीवादी जुड़ावों को भुलाया जा सकेगा? पॉल डी मान के अपने सम्बन्ध उनकी आलोचना के छद्मों की पोल खोल देते हैं। क्या अटल विहारी वाजपेयी की कविताओं का मूल्यांकन करते समय यह भुलाया जा सकेगा कि उन्हीं के प्रधानमंत्रित्वकाल में गुजरात के भयानक दंगे हुए जिसका उन्होंने समय रहते षमन नहीं किया?
आज के इच्छाधारी साहित्य और साहित्यकारों के दौर में मेरी बातें कुछ लोगों को थोड़ा पुरानी और घिसी-पिटी लग सकती है। उन लोगों के लिए वीरेन डंगवाल की ये पक्तियाँ छोड़ रहा हूँ।
''मजे का बखत है तो इसमें हैरानी क्या है?
हमें भी कैलेन द्यो कुछ मज्जा परेसानी क्या?''
'कुछ कद्दू चमकाये मैंने'
Friday, October 24, 2008
एक पीड़ादायक परिवर्तन
सूचना
एक पीड़ादायक परिवर्तन
ब्लाग मित्रो,
आप लोग मेरे ब्लाग वांगमय को लम्बे समय से पढ़ते रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है इस ब्लाग को देश-विदेश में पढा जाता रहा है। मुझे अपने लेखन पर समय-समय पर टिप्पणियाँ भी प्राप्त होती रही हैं। इस सब के लिए मैं आप सभी का आभारी हॅूं। मैंने यथासंभव यह प्रयास किया है कि यह ब्लाग गंभीर विषयों पर केन्द्रित रहे और इस पर होने वाली चर्चाएँ ऐसी हों कि उनसे कुछ सकारात्मक प्राप्त हो सके। इस बात में मैं कितना सफल रहा बता नहीं सकता। इसका मूल्यांकन आप लोग ही कर सकते हैं।
पिछले दिनों मेरे ब्लाग पर किसी अनाम व्यक्ति ने कुछ व्यक्तिगत आक्षेपकारी और आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कीं। इन टिप्पणियों से मुझे और मेरे मित्रों को क्लेश पहुँचा। इन्टरनेट सभी को यह सुविधा देता है कि बिना अपना परिचय बताये कोई भी टिप्पणी की जा सकती है। इसके कुछ सकारात्मक पक्ष अवश्य हैं। मगर इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि कोई भी आपके ब्लाग पर उल्टी सीधी टिप्प्णियाँ कर सकता है, गाली-गलौज और गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह की बातों से आप अपरिचित नहीं होंगे। उन सज्जन ने वांगमय पर इतनी आपत्तिजनक बातें लिख दी थी कि ब्लाग की गंभीरता नष्ट हुई और यहाँ तक कि मुझे एक पोस्ट ही निकाल देनी पड़ी। इस प्रकार की कुंठित और घटिया मानसिकता के लोग अन्य ब्लागों पर भी यह काम कर रहे हैं और उनके विरुध्द लोग शिकायतें भी दर्ज कर रहे हैं। यह घटियापन वास्तव में हमारे समाज में आ रहे सांस्कृतिक पतन की ओर भी संकेत है। अब लोगों में न तो दूसरों के सम्मान का ख्याल इै और न अपनी ही इज्जत का। खुले आम नेट पर गाली-गलौज हो रहा है और इस गाली-गलौज को ही लोग अपनी वाकपटुता और चतुराई समझ रहे हैं। दूसरों को अपमानित करने में ही एक प्रकार का गर्व अनुभव किया जा रहा है।
वांगमय की प्रकृति एक गंभीर ब्लाग की रही है। आप इस बात से सहमत होंगे कि इस ब्लाग पर गाली गलौज और कुठाग्रस्त मानसिकता के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आखिर विचार-विमर्श के इस मंच को किसी कुंठित मानसिकता के मलमूत्र विसर्जन का स्थान नहीं बनने दिया जा सकता। हम वैसे भी विषाणुओं से अपना बचाव करते ही हैं।
इसलिए दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आप जो भी टिप्पणियाँ प्रेषित करेंगे उन्हे संपादित होने के बाद ही इस ब्लाग पर प्रकाशित किया जा सकेगा। इससे निश्चितरूप से आप सभी को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो कि सामान्यत: वांछित नहीं। लेकिन आप मेरी विवशता समझ रहे होंगे। आशा है सहयोग बनाए रखेंगे।
रघुवंशमणि
एक पीड़ादायक परिवर्तन
ब्लाग मित्रो,
आप लोग मेरे ब्लाग वांगमय को लम्बे समय से पढ़ते रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है इस ब्लाग को देश-विदेश में पढा जाता रहा है। मुझे अपने लेखन पर समय-समय पर टिप्पणियाँ भी प्राप्त होती रही हैं। इस सब के लिए मैं आप सभी का आभारी हॅूं। मैंने यथासंभव यह प्रयास किया है कि यह ब्लाग गंभीर विषयों पर केन्द्रित रहे और इस पर होने वाली चर्चाएँ ऐसी हों कि उनसे कुछ सकारात्मक प्राप्त हो सके। इस बात में मैं कितना सफल रहा बता नहीं सकता। इसका मूल्यांकन आप लोग ही कर सकते हैं।
पिछले दिनों मेरे ब्लाग पर किसी अनाम व्यक्ति ने कुछ व्यक्तिगत आक्षेपकारी और आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कीं। इन टिप्पणियों से मुझे और मेरे मित्रों को क्लेश पहुँचा। इन्टरनेट सभी को यह सुविधा देता है कि बिना अपना परिचय बताये कोई भी टिप्पणी की जा सकती है। इसके कुछ सकारात्मक पक्ष अवश्य हैं। मगर इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि कोई भी आपके ब्लाग पर उल्टी सीधी टिप्प्णियाँ कर सकता है, गाली-गलौज और गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह की बातों से आप अपरिचित नहीं होंगे। उन सज्जन ने वांगमय पर इतनी आपत्तिजनक बातें लिख दी थी कि ब्लाग की गंभीरता नष्ट हुई और यहाँ तक कि मुझे एक पोस्ट ही निकाल देनी पड़ी। इस प्रकार की कुंठित और घटिया मानसिकता के लोग अन्य ब्लागों पर भी यह काम कर रहे हैं और उनके विरुध्द लोग शिकायतें भी दर्ज कर रहे हैं। यह घटियापन वास्तव में हमारे समाज में आ रहे सांस्कृतिक पतन की ओर भी संकेत है। अब लोगों में न तो दूसरों के सम्मान का ख्याल इै और न अपनी ही इज्जत का। खुले आम नेट पर गाली-गलौज हो रहा है और इस गाली-गलौज को ही लोग अपनी वाकपटुता और चतुराई समझ रहे हैं। दूसरों को अपमानित करने में ही एक प्रकार का गर्व अनुभव किया जा रहा है।
वांगमय की प्रकृति एक गंभीर ब्लाग की रही है। आप इस बात से सहमत होंगे कि इस ब्लाग पर गाली गलौज और कुठाग्रस्त मानसिकता के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आखिर विचार-विमर्श के इस मंच को किसी कुंठित मानसिकता के मलमूत्र विसर्जन का स्थान नहीं बनने दिया जा सकता। हम वैसे भी विषाणुओं से अपना बचाव करते ही हैं।
इसलिए दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आप जो भी टिप्पणियाँ प्रेषित करेंगे उन्हे संपादित होने के बाद ही इस ब्लाग पर प्रकाशित किया जा सकेगा। इससे निश्चितरूप से आप सभी को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो कि सामान्यत: वांछित नहीं। लेकिन आप मेरी विवशता समझ रहे होंगे। आशा है सहयोग बनाए रखेंगे।
रघुवंशमणि
Monday, October 20, 2008
बिहारी होने का मतलब
डायरी
बिहारी होने का मतलब
महाराष्ट्र में राज ठाकरे के वक्तव्यों और उसके बाद की हिंसक घटनाओं से बड़ी गहरी चिन्ताएँ पैदा होती हैं। यह बड़ी ही अजीब सी बात है कि अपने ही देश में एक प्रदेश का निवासी दूसरे प्रदेश में नौकरी की तलाश में न जा सके। हाल में जो घटनाएँ घटित हुई हैं वे भारत के नागरिकों के अधिकारों को ही निरस्त करने वाली हैं। देश में बहुत सी नौकरियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयन होते हैं और लोग आवेदन करते हैं। अब यदि इस तरह की हिंसात्मक पाबंदियाँ लगायी जायेंगी तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम होगा। मान लें कि इसी प्रकार हर प्रदेश के लोग हिंसा के द्वारा दूसरे प्रदेश के लोगों को अपने यहाँ आने से रोक दें तो क्या होगा? लेकिन दिक्कत यह है कि हम सोचने के बजाय अब मारपीट पर अधिक विश्वास करने लगे हैं। समझदारी के लिए सबसे कम जगह बची है।
अब लगता है कि बिहारी होना एक रूपक होता जा रहा है। एक ऐसा रूपक जिसके सामाजिक निर्माण के पीछे हिंसा और वर्चस्व का बोलबाला है। हर वह आदमी बिहारी होने की नियत झेले जो अपने बेहतर भविष्य की कामना करता है, और अपने प्रदेश के बाहर जाना चाहता है। यह दुखद ही है कि हम ऐसे समय में रह रहे है जिसमें हर मुद्दे को बड़ी छुद्र दृष्टि से देखा जा रहा है। जाति, धर्म और क्षेत्रीयता ने ऐसी गहरी विभाजक रेखाएँ खीच दी हैं कि किसी व्यापक सोच की सम्भावना ही खत्म होती जा रही है। हर समस्या का इलाज हिंसा को ही माना जा रहा है और अपनी बात को बलपूर्वक सही सिध्द करने का प्रयास किया जा रहा है। यह स्थिति निश्चित रूप से ऐसी दिशा में ले जायेगी जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। मगर शायद इस बात को समझने मे ठाकरे जैसे लोग और उनके समर्थक सक्षम नहीं।
अक्सर हम अपने तात्कालिक स्वार्थों को ही सामने रख पाते हैं और व्यापक हितों को नजरन्दाज करते हैं। सही गलत के निर्णय के बजाय हम बस अपने तक ही सीमित रह जा रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि जो लोग छोटे दायरों से शुरू होते हैं वे अनतत: स्वयम् पर ही जाकर समाप्त होते हैं। राधाकृष्णन जी ने परोक्षरुप से ऐसी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया था जो सर्वसत्तावाद और तानाशाही की ओर ले जाती है। इसके बरक्स समझदारी की संस्कृति ही एक मात्र रास्ता है। मगर यह रास्ता लम्बा है और इसमें कोई शार्टकट नहीं है।
हममें से बहुत लोग अपने गाँव, शहर या राज्य को छोड़कर दूसरी जगहों पर नौकरियाँ करने जाते हैं। हिन्दुस्तान के ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो विदेशों में रह रहे हैं। ये सभी लोग किसी न किसी अर्थ में बिहारी ही हैं। वे महाराष्ट्र के लोग भी जो बाहर कहीं काम कर रहे हैं। यदि हम महाराष्ट्र में पीटे जा रहे बेरोजगारों की जगह पर स्वयं को रखकर देख सकें तो हम सब बिहारी ही होंगे।
बिहारी होने का मतलब
महाराष्ट्र में राज ठाकरे के वक्तव्यों और उसके बाद की हिंसक घटनाओं से बड़ी गहरी चिन्ताएँ पैदा होती हैं। यह बड़ी ही अजीब सी बात है कि अपने ही देश में एक प्रदेश का निवासी दूसरे प्रदेश में नौकरी की तलाश में न जा सके। हाल में जो घटनाएँ घटित हुई हैं वे भारत के नागरिकों के अधिकारों को ही निरस्त करने वाली हैं। देश में बहुत सी नौकरियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयन होते हैं और लोग आवेदन करते हैं। अब यदि इस तरह की हिंसात्मक पाबंदियाँ लगायी जायेंगी तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम होगा। मान लें कि इसी प्रकार हर प्रदेश के लोग हिंसा के द्वारा दूसरे प्रदेश के लोगों को अपने यहाँ आने से रोक दें तो क्या होगा? लेकिन दिक्कत यह है कि हम सोचने के बजाय अब मारपीट पर अधिक विश्वास करने लगे हैं। समझदारी के लिए सबसे कम जगह बची है।
अब लगता है कि बिहारी होना एक रूपक होता जा रहा है। एक ऐसा रूपक जिसके सामाजिक निर्माण के पीछे हिंसा और वर्चस्व का बोलबाला है। हर वह आदमी बिहारी होने की नियत झेले जो अपने बेहतर भविष्य की कामना करता है, और अपने प्रदेश के बाहर जाना चाहता है। यह दुखद ही है कि हम ऐसे समय में रह रहे है जिसमें हर मुद्दे को बड़ी छुद्र दृष्टि से देखा जा रहा है। जाति, धर्म और क्षेत्रीयता ने ऐसी गहरी विभाजक रेखाएँ खीच दी हैं कि किसी व्यापक सोच की सम्भावना ही खत्म होती जा रही है। हर समस्या का इलाज हिंसा को ही माना जा रहा है और अपनी बात को बलपूर्वक सही सिध्द करने का प्रयास किया जा रहा है। यह स्थिति निश्चित रूप से ऐसी दिशा में ले जायेगी जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। मगर शायद इस बात को समझने मे ठाकरे जैसे लोग और उनके समर्थक सक्षम नहीं।
अक्सर हम अपने तात्कालिक स्वार्थों को ही सामने रख पाते हैं और व्यापक हितों को नजरन्दाज करते हैं। सही गलत के निर्णय के बजाय हम बस अपने तक ही सीमित रह जा रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि जो लोग छोटे दायरों से शुरू होते हैं वे अनतत: स्वयम् पर ही जाकर समाप्त होते हैं। राधाकृष्णन जी ने परोक्षरुप से ऐसी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया था जो सर्वसत्तावाद और तानाशाही की ओर ले जाती है। इसके बरक्स समझदारी की संस्कृति ही एक मात्र रास्ता है। मगर यह रास्ता लम्बा है और इसमें कोई शार्टकट नहीं है।
हममें से बहुत लोग अपने गाँव, शहर या राज्य को छोड़कर दूसरी जगहों पर नौकरियाँ करने जाते हैं। हिन्दुस्तान के ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो विदेशों में रह रहे हैं। ये सभी लोग किसी न किसी अर्थ में बिहारी ही हैं। वे महाराष्ट्र के लोग भी जो बाहर कहीं काम कर रहे हैं। यदि हम महाराष्ट्र में पीटे जा रहे बेरोजगारों की जगह पर स्वयं को रखकर देख सकें तो हम सब बिहारी ही होंगे।
Monday, October 13, 2008
झाँसी की गौरव गाथा
झाँसी की गौरव गाथा
हमारे देश के इतिहास में 1857 का स्वाधीनता संघर्ष स्वर्णाक्षरों में लिखित कालखण्ड है और इस समय की शौर्य गााथा की सबसे उज्ज्वल नक्षत्र महारानी लक्ष्मीबाई हैं। झाँसी की छोटी सी रियासत की भूमिका उस संघर्ष काल के एक दौर में केन्द्रीय हो गयी थी। हम में से अधिकतर लोग झाँसी के बारे में कम ही जानते हैं, शायद वहीं तक जहाँ तक झाँसी का इतिहास लक्ष्मीबाई से जुड़ता है। मगर झाँसी की कहानी लम्बी है और इस कहानी को झाँसी के ही निवासी और वरिष्ठ लेखक/कवि ओमशंकर खरे असर ने एक पुस्तक महारानी लक्ष्मीबाई एवं उनकी झाँसी का रूप दिया है।
यह पुस्तक वास्तव में असर साहब के लिखे गये कुछ लेखों का संकलन है जो उन्होंने जागरण अखबार के लिए एक श्रृंखला के अन्तर्गत लिखे थे। खरे साहब अपनी इस इतिहास की पुस्तक का प्रारम्भ बंगश और मराठों के बीच चल रहे संघर्ष से करते हैं जिसके चलते झाँसी एक शहर के रूप में सामने आया। पेशवा बाजीराव ने पहले-पहल इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को देखते हुए यहाँ एक छावनी स्थापित की थी क्योंकि यहाँ से दतिया और ओरक्षा राज्य करीब पड़ते थे जिनपर नियंत्रण जरूरी था। बाद में मराठा सेनानायक मल्हारकृष्ण की हत्या के बाद नारोशंकर झाँसी के सूबेदार बने। उन्होने राज्य की सीमा को बढ़ाया और झाँसी के किले को मजबूत किया। यही नहीं उन्होने झाँसी शहर को बसाने में भी दिलचस्पी दिखायी। पेशवा द्वारा उन्हें वापस बुलाने पर माधवगोविन्द आतिया , बाबूराव कन्हाई और विश्वासराव लक्ष्मण इस के सूबेदार नियुक्त हुए। पानीपत की लड़ाई में पराजय के बाद मराठे कमजोर पड़ गये। 1762 में शुजाउद्दौला ने झाँसी के किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1763 में ही मराठों ने फिर झाँसी पर कब्जा कर लिया। 1766 तक विश्वास राव लक्ष्मण यहाँ शासक रहे। 1770 में रघुनाथ हरी नेवलकर को झाँसी का शासन संभालने का अवसर मिला।
रघुनाथ हरी नेवलकर से ही वह वंश चलता है जिसकी राजबधू महारानी लक्ष्मीबाई बनी। वे एक प्रतापी शासक सिध्द हुए और उन्होने झाँसी को अवध और सिन्धिया की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों से बचाया। उनके समय में झाँसी ने कई हमलों और षडयन्त्रों का सामना सफलतापूर्वक किया। उन्होने अपने सुशासन द्वारा जनता में अपना प्रभाव बनाते हुए झाँसी में अपने राजवंश की नींव डाली। पच्चीस वर्षो तक शासन करने के उपरांत वे काशी चले गये। उनके छोटे भाई शिवराव भाÅ ने सन 1794 में झाँसँी के सूबेदार का पद संभाला। उनके समय में मराठों की पेशवाई कमजोर हो रही थी और अंग्रेजों का दबदबा भारत में बढ़ता जा रहा था। परिणाम स्वरूप शिवराव भाÅ को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। उनकी मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र रामचन्द्र भाÅ अपने चाचा के संरक्षण में महाराजा बने मगर अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गयी। इस दौरान अंग्रेजों का सम्पर्क झाँसी से बढ़ा और यह दौर षडयंत्रों का भी था। बढ़ते दबावों के चलते 1817 की संधि के अनुसार झाँसी में अंग्रेजी फोज का रखा जाना स्वीकार किया गया। रामचन्द राव के निघन के बाद अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को शासक बनाया जो कुख्यात और कुष्ठ रोग का शिकार था। वह शीघ्र ही कालकवलित हो गया। उत्तराधिकार के विवादों के बीच गंगाधर राव झाँसी के महाराजा बने जिनकी पत्नी महारानी लक्ष्मीबाई थीं।
गंगाधर राव के समय अंग्रेजों ने झाँसी के किले में अपनी सेना स्थापित क्ी। लेकिन इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुध्द छुटपुट विद्रोह शुरू हो गये थे। गंगाधर राव के समय में झाँसी का विकास हुआ क्योंकि वे एक कुशल और प्रभावशाली शसक थे। मगर वे विधुर हो गये थे उनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया था। सन्तान प्राप्ति के लिए उनहोने दूसरा विवाह किया था और रानी लक्ष्मीबाई उनकी पत्नी बनकर महल में आयी थीं। असर साहब यह बताते हैं कि लक्ष्मी बाई या मनू का जीवन कितने दुखों से भरा था। इस तथ्य को अब कम ही जाना जाता है। कम ही लोग जानते हैं क्योंकि यह दुख-कथा अब महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक शौर्य गााथा के नीचे दब सी गयी है। चार साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई की माता का निधन हो गया था। विवाहोपरान्त लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ था जो तीन माह बाद चल बसा। फिर महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु का कहर उन पर वैधव्य के रूप में टूटा।
लक्ष्मीबाई बचपन से ही प्रतिभाशाली और साहसी थीं। बिठूर में निवास के दौरान उन्होंने राजशाही के कायदे कानून सीखे। व्यायाम, घुड़सवारी वगैरह वहीं से सीखी। झाँसी आने पर शासन व्यवस्था में गंगाधर राव का सक्रिय सहयोग दिया। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद गंगाधर राव बीमार पड़ गये और उन्हें झाँसी के विलुप्त होने का भय सताने लगा। झाँसी की भीषण त्रासदी का चरण उनकी मृत्यु थी जिसने अंग्रेजों की सत्ता लोलुपता की कुदृष्टि को अवसर दिया। संग्रहणी के शिकार गंगाधर राव ने अपने अन्तिम दिनों में आनन्द राव को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया जिसकी उम्र पाँच वर्ष की थी। दत्तक विधान के बाद उसका नाम दामोदर राव गंगाधर रखा गया। यह 19 नवम्बर 1853 की बात है। उसी के दो दिन बाद महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया।
गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने लैप्स की नीति के तहत झाँसी को हड़पने की चेष्टाएँ आरम्भ कर दीं। महारानी लक्ष्मीबाई ने इसका हर प्रकार से विरोध किया। असर साहब ने अपनी पुस्तक में बतलाया है कि किस प्रकार स्लीमन ने दत्तक पुत्र के अधिकारों के प्रश्न पर दोहरा रवैया अपनाया था। इसी मुद्दे पर दो अंग्रेज प्रशासको एलिस और मैलकम में गहरे मतभेद थे । अत: सारा कुछ अन्तत: डलहौजी की सोच पर टिक गया । गोपनीय ढंग से झाँसी को जबलपुर के कमिश्नर के आधीन कर दिया गया गया और किसी को खबर तक नहीं हुई। अंग्रेजों ने कई मामले में दत्तक पुत्र के अधिकारों को स्वीकार किया था। मगर उनहोंने झाँसी के मामले में उसे नया राज्य मानकर ऐसा करने से इनकार किया। जबकि तथ्य यह है कि पेशवाई के समय से ही झाँसी एक राज्य के रूप में वर्तमान था। झाँसी को नया राज्य बताने को असर साहब अंग्रेजों की घटिया कूटनीति का उदाहरण मानते हैं।
ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर असर साहब बतलाते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई ने इस निर्णय के विरुध्द दो प्रार्थनापत्र कम्पनी सरकार के पास भेजे। ये दो पत्र इस बात के सबूत हैं कि महारानी में गजब की तर्क क्षमता थी। मगर अंग्रेजों ने इन्हे स्वीकार नहीं किया क्योंकि लार्ड डलहौजी की मंशा देशी राज्यों को हड़पकर अंग्रेजी राज्य में मिलाने की थी। परिणामस्वरूप रानी को किला छोड़कर रानी महल में रहना पड़ा। यह उनके लिए बेहद संकटग्रस्त समय था क्योंकि अंग्रेज सेना सभी खजानों को मोहरबंद कर हस्तगत कर रही थी और अभी रानी पति के शोक से उबर भी नहीं पायी थीं कि यह बड़ा राजनीतिक संकट सामने आन पड़ा था। इन भयानक दबावों के बीच महारानी ने हैमिल्टन से बात की जिसका जिक्र असर साहब ने विस्तारपूर्वक किया है। रानी ने अंग्रेजों की पेंशन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे स्वीकार करने का अर्थ था झाँसी के राज्य की समाप्ति को स्वीकार कर लेना। इसी दौर में जॉन लैंग के वर्णनों में महारानी के व्यक्तित्व, उनकी आनबान, और उनकी लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है। पुस्तक का यह अंश विशेष आकर्षित करता है।
2जून 1857 को झाँसी में सैनिकों ने विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया। मगर रानी ने सही अवसर की प्रतीक्षा की। तेज क्रान्तिकारी गतिविधियों के बीच अपनी कुशल कार्यनीति और नेतृत्व क्षमता के चलते 12 जून को महारानी ने झाँसी का शासन संभाल लिया। महारानी ने 11 माह तक झाँसी पर शासन किया और इस दौर में उनके क्रिया कलापों ने उन्हें जनता में अतिलोकप्रिय बनाया युध्द के अन्तिम दौर में अंग्रेजों ने झाँसी को बरबाद करने का पूरा प्रयास किया। आगजनी से लेकर निर्दोष जनता की हत्या तक का काम किया गया। इस प्रकार 1744 से 1858 तक चलने वाला झाँसी का सम्ध्द राज्य अंग्रेजों की सत्ता लोलुपता का शिकार हो गया। अपनी मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को विश्वासपात्र सरदार रामचन्द्र राव देशमुख को सौंपा था कि वह उसकी देखरेख करे। झाँसी के राजवंश का यह चिराग लम्बे समय तक बेतवा के धने जंगलों में कुछ विश्वासपात्र लोगों के साथ भटकता रहा। पर बाद में विश्वासघात और पैसे की कमी के चलते उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। दामोदर राव की मृत्यु 1906 में हुई।
झाँसी की कहानी का वर्णन ओमशंकर खरे असर ने आद्योपांत एक झाँसी के ऐसे नागरिक के रूप में किया है जिसे अपनी विरासत से गहरा लगाव है। इसका एक कारण उनके परिवार का स्वयं इतिहास के एक अंश से जुड़ा होना रहा है। झाँसी के इतिहास के कुछ पक्ष विवादों के घेरे में रहे हैं और उन पर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। ओमशंकर खरे असर के लेखन की विशेषता यह रही है कि विवादित मुद्दों के सभी पक्षों को हाजिर कर अपना तर्क और पक्ष प्रस्तुत करते हैं। झाँसी और महारानी लक्ष्मीबाई से जुउे विवादों में वे निर्णय बड़े तार्किक ढंग से लेते हैं। इस सिलसिले में उदाहरण के लिए उन्होंने महारानी के जन्म वर्ष के बारे में उन्होने लम्बी छानबीन की है। इसी प्रकार विवाह के समय महारानी की उम्र को लेकर उन्होने गहराई से विचार-विमर्श किया है। उन्होने यह पाया है कि विवाह के समय वे सात वर्ष की नहीं अपितु 15 वर्ष की थीं।
ओमशंकर जी झाँसी के निवासी होने के नाते इतिहास में घटित होने वाली घटनाओं के स्थानों का बखूबी वर्णन करते हैं। वे केवल इतिहास के लेखक न होकर एक साहित्यकार भी हैं। अत: उनकी भाषा में इतिहास लेखक का सूखापन नहीं है। उनकी भाषा सर्जनात्मक है। तथापि वे अपने लेखन में ऐतिहासिक तथ्यों को ही महत्व देते हैं। वे उससे परे की चीजों, जैसे लोक में प्रचलित बातों, को रेखांकित भर ही करते हैं। संक्षेप में यह कि झाँसी के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में रुचि रखने वालों के लिए यह एक जरूरी पुस्तक है।
.................. ................................ ......................
समीक्षित पुस्तक: महारानी लक्ष्मीबाई एवं उनकी झाँसी
लेखक: ओम शंकर असर
संपादक: ए. के. पाण्डेय
प्रकाशन: राजकीय संग्रहालय, झाँसी
हमारे देश के इतिहास में 1857 का स्वाधीनता संघर्ष स्वर्णाक्षरों में लिखित कालखण्ड है और इस समय की शौर्य गााथा की सबसे उज्ज्वल नक्षत्र महारानी लक्ष्मीबाई हैं। झाँसी की छोटी सी रियासत की भूमिका उस संघर्ष काल के एक दौर में केन्द्रीय हो गयी थी। हम में से अधिकतर लोग झाँसी के बारे में कम ही जानते हैं, शायद वहीं तक जहाँ तक झाँसी का इतिहास लक्ष्मीबाई से जुड़ता है। मगर झाँसी की कहानी लम्बी है और इस कहानी को झाँसी के ही निवासी और वरिष्ठ लेखक/कवि ओमशंकर खरे असर ने एक पुस्तक महारानी लक्ष्मीबाई एवं उनकी झाँसी का रूप दिया है।
यह पुस्तक वास्तव में असर साहब के लिखे गये कुछ लेखों का संकलन है जो उन्होंने जागरण अखबार के लिए एक श्रृंखला के अन्तर्गत लिखे थे। खरे साहब अपनी इस इतिहास की पुस्तक का प्रारम्भ बंगश और मराठों के बीच चल रहे संघर्ष से करते हैं जिसके चलते झाँसी एक शहर के रूप में सामने आया। पेशवा बाजीराव ने पहले-पहल इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को देखते हुए यहाँ एक छावनी स्थापित की थी क्योंकि यहाँ से दतिया और ओरक्षा राज्य करीब पड़ते थे जिनपर नियंत्रण जरूरी था। बाद में मराठा सेनानायक मल्हारकृष्ण की हत्या के बाद नारोशंकर झाँसी के सूबेदार बने। उन्होने राज्य की सीमा को बढ़ाया और झाँसी के किले को मजबूत किया। यही नहीं उन्होने झाँसी शहर को बसाने में भी दिलचस्पी दिखायी। पेशवा द्वारा उन्हें वापस बुलाने पर माधवगोविन्द आतिया , बाबूराव कन्हाई और विश्वासराव लक्ष्मण इस के सूबेदार नियुक्त हुए। पानीपत की लड़ाई में पराजय के बाद मराठे कमजोर पड़ गये। 1762 में शुजाउद्दौला ने झाँसी के किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1763 में ही मराठों ने फिर झाँसी पर कब्जा कर लिया। 1766 तक विश्वास राव लक्ष्मण यहाँ शासक रहे। 1770 में रघुनाथ हरी नेवलकर को झाँसी का शासन संभालने का अवसर मिला।
रघुनाथ हरी नेवलकर से ही वह वंश चलता है जिसकी राजबधू महारानी लक्ष्मीबाई बनी। वे एक प्रतापी शासक सिध्द हुए और उन्होने झाँसी को अवध और सिन्धिया की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों से बचाया। उनके समय में झाँसी ने कई हमलों और षडयन्त्रों का सामना सफलतापूर्वक किया। उन्होने अपने सुशासन द्वारा जनता में अपना प्रभाव बनाते हुए झाँसी में अपने राजवंश की नींव डाली। पच्चीस वर्षो तक शासन करने के उपरांत वे काशी चले गये। उनके छोटे भाई शिवराव भाÅ ने सन 1794 में झाँसँी के सूबेदार का पद संभाला। उनके समय में मराठों की पेशवाई कमजोर हो रही थी और अंग्रेजों का दबदबा भारत में बढ़ता जा रहा था। परिणाम स्वरूप शिवराव भाÅ को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। उनकी मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र रामचन्द्र भाÅ अपने चाचा के संरक्षण में महाराजा बने मगर अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गयी। इस दौरान अंग्रेजों का सम्पर्क झाँसी से बढ़ा और यह दौर षडयंत्रों का भी था। बढ़ते दबावों के चलते 1817 की संधि के अनुसार झाँसी में अंग्रेजी फोज का रखा जाना स्वीकार किया गया। रामचन्द राव के निघन के बाद अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को शासक बनाया जो कुख्यात और कुष्ठ रोग का शिकार था। वह शीघ्र ही कालकवलित हो गया। उत्तराधिकार के विवादों के बीच गंगाधर राव झाँसी के महाराजा बने जिनकी पत्नी महारानी लक्ष्मीबाई थीं।
गंगाधर राव के समय अंग्रेजों ने झाँसी के किले में अपनी सेना स्थापित क्ी। लेकिन इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुध्द छुटपुट विद्रोह शुरू हो गये थे। गंगाधर राव के समय में झाँसी का विकास हुआ क्योंकि वे एक कुशल और प्रभावशाली शसक थे। मगर वे विधुर हो गये थे उनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया था। सन्तान प्राप्ति के लिए उनहोने दूसरा विवाह किया था और रानी लक्ष्मीबाई उनकी पत्नी बनकर महल में आयी थीं। असर साहब यह बताते हैं कि लक्ष्मी बाई या मनू का जीवन कितने दुखों से भरा था। इस तथ्य को अब कम ही जाना जाता है। कम ही लोग जानते हैं क्योंकि यह दुख-कथा अब महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक शौर्य गााथा के नीचे दब सी गयी है। चार साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई की माता का निधन हो गया था। विवाहोपरान्त लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ था जो तीन माह बाद चल बसा। फिर महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु का कहर उन पर वैधव्य के रूप में टूटा।
लक्ष्मीबाई बचपन से ही प्रतिभाशाली और साहसी थीं। बिठूर में निवास के दौरान उन्होंने राजशाही के कायदे कानून सीखे। व्यायाम, घुड़सवारी वगैरह वहीं से सीखी। झाँसी आने पर शासन व्यवस्था में गंगाधर राव का सक्रिय सहयोग दिया। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद गंगाधर राव बीमार पड़ गये और उन्हें झाँसी के विलुप्त होने का भय सताने लगा। झाँसी की भीषण त्रासदी का चरण उनकी मृत्यु थी जिसने अंग्रेजों की सत्ता लोलुपता की कुदृष्टि को अवसर दिया। संग्रहणी के शिकार गंगाधर राव ने अपने अन्तिम दिनों में आनन्द राव को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया जिसकी उम्र पाँच वर्ष की थी। दत्तक विधान के बाद उसका नाम दामोदर राव गंगाधर रखा गया। यह 19 नवम्बर 1853 की बात है। उसी के दो दिन बाद महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया।
गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने लैप्स की नीति के तहत झाँसी को हड़पने की चेष्टाएँ आरम्भ कर दीं। महारानी लक्ष्मीबाई ने इसका हर प्रकार से विरोध किया। असर साहब ने अपनी पुस्तक में बतलाया है कि किस प्रकार स्लीमन ने दत्तक पुत्र के अधिकारों के प्रश्न पर दोहरा रवैया अपनाया था। इसी मुद्दे पर दो अंग्रेज प्रशासको एलिस और मैलकम में गहरे मतभेद थे । अत: सारा कुछ अन्तत: डलहौजी की सोच पर टिक गया । गोपनीय ढंग से झाँसी को जबलपुर के कमिश्नर के आधीन कर दिया गया गया और किसी को खबर तक नहीं हुई। अंग्रेजों ने कई मामले में दत्तक पुत्र के अधिकारों को स्वीकार किया था। मगर उनहोंने झाँसी के मामले में उसे नया राज्य मानकर ऐसा करने से इनकार किया। जबकि तथ्य यह है कि पेशवाई के समय से ही झाँसी एक राज्य के रूप में वर्तमान था। झाँसी को नया राज्य बताने को असर साहब अंग्रेजों की घटिया कूटनीति का उदाहरण मानते हैं।
ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर असर साहब बतलाते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई ने इस निर्णय के विरुध्द दो प्रार्थनापत्र कम्पनी सरकार के पास भेजे। ये दो पत्र इस बात के सबूत हैं कि महारानी में गजब की तर्क क्षमता थी। मगर अंग्रेजों ने इन्हे स्वीकार नहीं किया क्योंकि लार्ड डलहौजी की मंशा देशी राज्यों को हड़पकर अंग्रेजी राज्य में मिलाने की थी। परिणामस्वरूप रानी को किला छोड़कर रानी महल में रहना पड़ा। यह उनके लिए बेहद संकटग्रस्त समय था क्योंकि अंग्रेज सेना सभी खजानों को मोहरबंद कर हस्तगत कर रही थी और अभी रानी पति के शोक से उबर भी नहीं पायी थीं कि यह बड़ा राजनीतिक संकट सामने आन पड़ा था। इन भयानक दबावों के बीच महारानी ने हैमिल्टन से बात की जिसका जिक्र असर साहब ने विस्तारपूर्वक किया है। रानी ने अंग्रेजों की पेंशन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे स्वीकार करने का अर्थ था झाँसी के राज्य की समाप्ति को स्वीकार कर लेना। इसी दौर में जॉन लैंग के वर्णनों में महारानी के व्यक्तित्व, उनकी आनबान, और उनकी लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है। पुस्तक का यह अंश विशेष आकर्षित करता है।
2जून 1857 को झाँसी में सैनिकों ने विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया। मगर रानी ने सही अवसर की प्रतीक्षा की। तेज क्रान्तिकारी गतिविधियों के बीच अपनी कुशल कार्यनीति और नेतृत्व क्षमता के चलते 12 जून को महारानी ने झाँसी का शासन संभाल लिया। महारानी ने 11 माह तक झाँसी पर शासन किया और इस दौर में उनके क्रिया कलापों ने उन्हें जनता में अतिलोकप्रिय बनाया युध्द के अन्तिम दौर में अंग्रेजों ने झाँसी को बरबाद करने का पूरा प्रयास किया। आगजनी से लेकर निर्दोष जनता की हत्या तक का काम किया गया। इस प्रकार 1744 से 1858 तक चलने वाला झाँसी का सम्ध्द राज्य अंग्रेजों की सत्ता लोलुपता का शिकार हो गया। अपनी मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को विश्वासपात्र सरदार रामचन्द्र राव देशमुख को सौंपा था कि वह उसकी देखरेख करे। झाँसी के राजवंश का यह चिराग लम्बे समय तक बेतवा के धने जंगलों में कुछ विश्वासपात्र लोगों के साथ भटकता रहा। पर बाद में विश्वासघात और पैसे की कमी के चलते उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। दामोदर राव की मृत्यु 1906 में हुई।
झाँसी की कहानी का वर्णन ओमशंकर खरे असर ने आद्योपांत एक झाँसी के ऐसे नागरिक के रूप में किया है जिसे अपनी विरासत से गहरा लगाव है। इसका एक कारण उनके परिवार का स्वयं इतिहास के एक अंश से जुड़ा होना रहा है। झाँसी के इतिहास के कुछ पक्ष विवादों के घेरे में रहे हैं और उन पर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। ओमशंकर खरे असर के लेखन की विशेषता यह रही है कि विवादित मुद्दों के सभी पक्षों को हाजिर कर अपना तर्क और पक्ष प्रस्तुत करते हैं। झाँसी और महारानी लक्ष्मीबाई से जुउे विवादों में वे निर्णय बड़े तार्किक ढंग से लेते हैं। इस सिलसिले में उदाहरण के लिए उन्होंने महारानी के जन्म वर्ष के बारे में उन्होने लम्बी छानबीन की है। इसी प्रकार विवाह के समय महारानी की उम्र को लेकर उन्होने गहराई से विचार-विमर्श किया है। उन्होने यह पाया है कि विवाह के समय वे सात वर्ष की नहीं अपितु 15 वर्ष की थीं।
ओमशंकर जी झाँसी के निवासी होने के नाते इतिहास में घटित होने वाली घटनाओं के स्थानों का बखूबी वर्णन करते हैं। वे केवल इतिहास के लेखक न होकर एक साहित्यकार भी हैं। अत: उनकी भाषा में इतिहास लेखक का सूखापन नहीं है। उनकी भाषा सर्जनात्मक है। तथापि वे अपने लेखन में ऐतिहासिक तथ्यों को ही महत्व देते हैं। वे उससे परे की चीजों, जैसे लोक में प्रचलित बातों, को रेखांकित भर ही करते हैं। संक्षेप में यह कि झाँसी के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में रुचि रखने वालों के लिए यह एक जरूरी पुस्तक है।
.................. ................................ ......................
समीक्षित पुस्तक: महारानी लक्ष्मीबाई एवं उनकी झाँसी
लेखक: ओम शंकर असर
संपादक: ए. के. पाण्डेय
प्रकाशन: राजकीय संग्रहालय, झाँसी
Thursday, October 09, 2008
ईश्वर, सत्ता और कविता (4)
ईश्वर, सत्ता और कविता (4)
बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में ईश्वर के प्रति कविता में भाव बदलते गये हैं। भारतीय जनता पार्टी की धर्म को राजनीतिक हथकण्डे के रूप में अपनाने की नीति का सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ा । आस्तिक लोगों के ड्राइंग रूमों में आशीर्वाद देने की मुद्रा में अनामिका मोड़े खड़े राम के स्थान पर समुद्र को धमकाते धनुङ्ढ हाथ में ताने हुए राम के चित्र दिखाई देने लगे। संघी भाइयों के यहां तो ये चित्र अनिवार्यत: मिलने लगे जिसकी कलाकारी इस बात मे थी कि राम का क्रोध उनकी शक्तिशाली मांसपेसियों में झलकने लगा। भारत के सांप्रदायिक परिप्रेक्ष्य में यह बहुत स्पष्ट था कि 'जलधि जड़' मुसलामान ही थे। अभिवादन के लिए प्रयुक्त होने वाला राम का नाम आक्रामक और हिंसक 'जै श्रीराम' के भयानक उद्धोष मेंं बदल गया। ईश्वर के इस घटिया और स्थूल राजनीतिक प्रयोग ने किसी भी प्रकार के दार्शनिक उदात्ता के लिए स्पेस नहीं छोड़ा।
उत्पात के प्रारंभिक दौर में आयी मानबहादुर सिंह की कविता 'समकालीन ईश्वर की लाचारी' एक दूसरी अवस्थित से लिखी गयी कविता है । इस कविता का रचनाकाल वह समय है जब सांप्रदायिकता की गरज उतनी तेज नहीं थी इस कारण यह कविता अधिक महत्व की हो जाती है । यह कम पढ़ी गयी और लगभग अचर्चित कविता ईश्वर के दुरुप्योग और हिंसा से भरे माहौल में ईश्वर की लाचारी को दर्शाती है। इस मायने में ईश्वर के साथ 'समकालीन' पद का प्रयोग वाकई अर्थपूर्ण है। बाद में लिखी गयी वीरेन डंगवाल की कविता 'दुश्चक्र में स्रष्टा' से इस कविता को मिला कर देखा जा सकता है। यह कविता ईश्वर के पक्ष से प्रस्तुत एक अंधाधुंंध मोनोलाग है या कहें कि विवश ईश्वर का प्रलाप। यहां ईश्वर के मनुष्यता के विरोध में हुए प्रयोंगों को भर्त्सनात्मक ढंग से प्रदर्शित किया गया है।
वीरेन डंगवाल की कविता में 'दुश्चक्र में स्रष्टा' अपनी विडम्बनात्मक अभिव्यक्तियों के चलते महत्वपूर्ण है और इसी कारण उसने हिंदी के पाठकों और आलोचकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। कविता मे उपस्थित यह व्यंग्य और विडम्बना का स्वर कविता के अंत तक पहुंचते-पहुचते आक्रोश में बदल जाता है। 'दुश्चक्र में स्रष्टा' कविता का प्रारंभ भगवान के कारीगरी के कमाल के जिक्र के साथ होता है। समकालीन घटनाक्रम के सापेक्ष यह जिक्र व्यंग्य और विडम्बना के स्वर के साथ है।
'अरे, कुत्ते की उस पतली गुलाबी जीभ का ही क्या कहना!
कैसी रसीली और चिकनी टपकदार, सृष्टि के हर
स्वाद की मर्मज्ञ
और दुम की तो बात ही अलग
गोया एक अदृश्य पंखे की मूठ
तुम्हारे मुखड़े पर झलती हुई'
ईश्वर के शानदार कृत्यों का यह विडम्बनापूर्ण वर्णन इस शिकायत के साथ समय के यथार्थ तक पहुंचता है कि भगवान ने अपना कामयाब कारखाना बंद कर दिया है और अब जो कुछ भी इस तथाकथित ईश्वरीय सत्ता के नाम पर है वह बुरा ही बुरा है। क्या अच्छे और आश्चर्यजनक कार्य सम्पन्न करने वाला ईश्वर कहीं विलुप्त हो गया है? आखिर समकालीन तबाहियों के बीच 'रहमानुर्रहीम' या 'करूणानिधान'ईश्वर के अस्तित्व के कोई चिन्ह क्यों नहीं दिखाई पड़ते?
'बाढ़ें तो आयी खैर भरपूर, काफी भूकंप, तूफान
खून से लबालब हत्याकांड अलबत्ता हुए खूब
खूब अकाल, युध्द एक से एक तकनीकी चमत्कार
रह गयी सिर्फ एक सी भूख, लगभग एक सी फौजी
वर्दियां जैसे
मनुष्य मात्र की एकता प्रमाणित करने के लिए
एक जैसी हुंकार, हाहाकार!
प्रार्थना गृह जरूर उठाये गये एक से एक आलीशान!
मगर भीतर चिने हुए रक्त के गारे से
वे खोखले आत्माहीन शिखर-गुम्बद-मीनार
उंगली से छूते ही जिन्हें रिस आता है खून!
आखिर यह किनके हाथों सौंप दिया है ईश्वर
तुमने अपना इतना बड़ा करोबार?'
वीरेन डंगवाल की यह कविता ईश्वर के अस्तित्व और उसके कार्यों को लेकर प्रचलित मान्यताओं और परंपरागत विचारों से प्रारंभ होकर उन्हीं को प्रश्नांकित करती है।इयवर की अनुपस्थिति इस बात में है कि अब उसका इस विश्व पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।पर सवाल यह हुआ कि यदि इस पर उसका नियंत्रण नहीं तो फिर नियंत्रण है किसका। क्या ईश्वर की कोई वास्तविक सत्ता है भी या यह महज एक परंपरागत असत्य है? क्या ईश्वर नयी क्रूर सत्ताओं सा डर कर भाग गया है? शायद उसका इन क्रूर सत्ताओं से कोई परोक्ष-अपरोक्ष समझौता हो गया हो? कुल मिलाकर कवि के लिए ईश्वर असहनीय हो गया है। यही कानण है कि कविता आक्रोश के ऐसे बिन्दु पर समाप्त होती है जहाँ ईश्वर संबंधी सारी पारंपरिक अवधारणाएँ नष्ट हो जाती हैं।
'अपना कारखना बंद करके
किस घोसले में जा छिपे हो भगवान?
कौन सा है आखिर, वह सातवाँ आसमान?
हे, अरे, अबे, ओ करूणानिधान!!'
युवा कवि पंकज चतुर्वेदी की कविता 'ईसा, बुध्द, हज़रत मुहम्मद के लिए' ईश्वर और पैगम्बरों के नाम पर होने वाली हिंसा और मारकाट का खुलासा करती हुई उसके राजनीतिक प्रयोगों को रेखांकित करती है। भारत ने बुध्द पूर्णिमा के दिन पोकरण में परमाणु विस्फोट किया था तो संकेत का संदेश था 'बुध्द मुस्काराये'। यह विडम्बनापूर्ण संदेश इस ओर ले जाता है कि मनुष्य को नष्ट करने के ङ्ढडयंत्र में ईश्वर का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ ईश्वर की सत्ताा नगण्य है और महत्वपूर्ण है अमरीका, भारत ओर पाकिस्तान की शासन सत्तााएं जो बुध्द, ईसा और हजरत मोहम्मद का इस्तेमाल कर रहे है। यह यूं ही नहीं है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता और इस्लामिक बम के साथ-साथ हटिंगटन की पुस्तक भी आ पहुंची है। धर्म और नस्ल को वैधता देने मे ईश्वर कहीं न कहीं उपस्थित होता है।
ऋतुराज के कविता संग्रह 'लीलामुखारविन्द' में ईश्वर की उपस्थिति अनेक ठोस रूपों में दिखलाई पड़ती है। यह उसका कोई भक्तियुगीन साकार रूप नहीं है, मगर है कुछ वैसा ही। वह कहीं न होते हुए भी सर्वत्र उपस्थित है। सभी प्रकार के पापाचारों में वह शरीक है। यही वह लीला है जो सत्ता और शक्ति के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाकलापों में अन्तर्निहित है। ऋतुराज सत्ता के विभिन्न प्रकार के चेहरों के खेल में उसकी उपस्थिति पाते है- यही है 'लीला मुखारविन्द'। कविता 'ईश्वर चरितम्' में ईश्वर न होते हुए भी परेशानी का कारण है, क्योंकि वह तमाम सत्ता प्रतिष्ठानों और शक्ति केन्द्रों के लिए उपकरण बन गया है। प्रात: काल में बजने वाले भजनों से लेकर रात्रि तक, हर समय उसकी उपस्थिति है।
'हत्यारा हत्या करता है ईश्वर के नाम पर
हत्यारे के पक्ष में ईश्वर गवाही देता है
क्योंकि हर अपराध में उसका हाथ होता है।'
यह सब कुछ होते हुए भी ईश्वर नाम का यह 'मुख्य अभियुक्त अदृश्य' रहता है। इस प्रकार वह निराकार और साकार दोनों है। वास्तव मे यह सत्ता प्रतिष्ठानों का वह वर्चस्वी भ्रष्ट रूप है, जो ईश्वर का इस्तेमाल करता है। यहां ईश्वर तलवार भी है और ढाल भी। और कहीं-कहीं तो वह अदृश्य सत्ताानायक है जो स्वयं ही ईश्वर बन बैठता है। यह विडम्बना ही है। अपने समय के सांप्रदायिक और वर्चस्वी शक्तियाें को देखें तो वे ईश्वर सदृश ही हैं। यह ईश्वरत्व तो धरती पर ही साकार है और उसके ठोस रूप खूंखार और डरावने हैं।
''उनके हाथों में खून सनी छडे थी'
चाकू तेजाब की बोतलें भी
अनगिनत हाथ थे जैसे तुम्हारे ही हाथ हों वे''
'श्री ईश्वरचरितम्' कविता में ईश्वर इतना अधिक है कि कवि की नींद हराम है। वह ईश्वर को कोसता है। उसकी उपस्थिति अमानवीय है। ईश्वर के नाम पर सुबह से ही धूम-धड़ाका है। यह ढोंग तो है ही। अपने कुकर्मों को वैधता प्रदान करने का शक्तिपाठ है। ईश्वर ही वह प्रत्यय है जिसके द्वारा हत्याओं को वैधता दी जा सकती है। ईश्वर अदृश्य मुख्य अभियुक्त है। कविता की विडम्बना इस बात में है कि मुख्य अभियुक्त का दो अर्थ है। एक तो ईश्वर जो दिखाई नहीं देता और चारों तरफ है और दूसरी अर्थ है वह सत्ताा जो हर जगह शक्ति के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करता है। अपने दौर में राम के नाम पर हुए उत्पातों से जुड़ी दक्षिणपंथी शक्ति सत्ताा के सापेक्ष कविता का अर्थ बहुत साफ होता है। ईश्वर, धर्म और सत्ताा के इस क्रूर और अमानवीय गठजोड़ को यह कविता अपनी चिंता का विङ्ढय बनाती है।
सत्तााएं सदैव प्रत्ययों की मदद से शासन करती हैं और उन्हें अपनी वैधता सिध्द करने के लिए इस प्रकार के उपादानों की सदा ही आवश्यकता रहती है। यह किसी धर्म अथवा नस्ल की श्रेष्ठता से लेकर स्वतंत्रता तक का मुद्दा हो सकता है। बुश जैसे सत्तााधीश यदि इराक की जनता को मुक्त कराने के नाम पर आक्रमण को वैधता प्रदान करते हैं तो हिन्दू राष्ट्र और हिन्दुत्व की श्रेष्ठता का मुखौटा सत्तााछद्म पर पर्दे का काम करती है। इसी प्रकार 'देयर इज नो गाड बट अल्लाह' भी अपना काम करता है। ईश्वर सत्तााओं को किस प्रकार से वैधता प्रदान करता है इसका हमारे समय में इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि राम के नाम पर साम्प्रदायिकता के नंगे नृत्य को भी वैधता दी जाय। गुजरात के दंगों को उदार हिन्दुओं की स्वाभाविक प्रक्रिया कह कर बच चला जाय। हिन्दुओं की उदारता भी तो इसी बात द्वारा सिध्द की जाती है कि यहाँ असंख्य देवी-देवता है। अस्ल में इन देवी-देवताओं के पीछे सत्ताा एक ही है जिसके हजारों हाथ कहीं अदृश्य से प्रकट होकर जीवन घुस आते हैं और विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं।
मानववादी कविता से अलग इस नये तौर की कविता दृष्टि की महत्ताा इसी में है कि वह मनुष्य और ईश्वर की सत्ता को एक नहीं देखती। यह ईश्वर की अद्वितीय और सर्वशक्तिमान सत्ताा के प्रति भी मुग्ध नहीं। यह तो और पीछे की बात है। वह दरअस्ल ईश्वर को वर्चस्वी सत्ताा के एक प्रतिनिधि के रूप में देखती है जिसके विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते रहे हैं-खासकर भरतीय राजनीति में।
हिन्दी कविता में ईश्वर के प्रत्यय का यह इस्तेमाल अर्तक्य के विरोध में आता है। हमारे समय में उसकी एक ऐतिहासिक उपस्थिति है जिसे सांप्रदायिकता और फासीवाद के विरुध्द खड़े होते हुए देखा जा सकता है। यही कारण्ा है कि इन कविताओं मेें ईश्वर की चर्चा महज एक दार्शनिक प्रत्यय के रूप में नहीं है। यहाँ वह धर्म के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिफलनों मेें रेखांकित किया गया है। जाहिर तौर पर यह महज एक आस्था का प्रश्न नहीं बनकर रह जाता। इसके विभिन्न आयाम दिखलाई देते हैं। समाज संस्कृति में ईश्वर के प्रत्यय द्वारा एक मनुष्यता विरोधी वर्चस्वी व्यवस्था अथवा सत्ता की स्थापना का यहाँ स्पष्ट विरोध देखा जा सकता है।
प्रकृति और सामान्य जीवन की कविता लिखने वाले नरेन्द्र पुण्डरीक ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार कर पाते क्योंकि वह इश्वरीय सत्ता, आततायी सत्ता की समर्थक है ऐसे में ईश्वर की प्रार्थना के लिए शब्द कहां से आयेंगे।
''कैसे चुपचाप रोज
मेरे सपनों का रौंदता हुआ
आकाश से गुजर जाता है
इन्द्र का हाथी,
बताओ तुम्हारी सरोकारहीन
प्रार्थनाओं के लिए
कहां से जुटाऊं शब्द ईश्वर''
सत्ता और शक्ति के केन्द्र्र ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं और राम लोगों के हृदय से बाहर कैद में रह जाते हैं- अयोध्या को लेकर चलती राजनीति की कैद में। 'कैसे छीने गये राम' कविता में ऐसे विवश और शक्तिहीन ईश्वर का क्या किया जाय। इस फालतू ईश्वर के बारे में यदि जानकारियां हों भी तो किस काम की।
''ईश्वर के पास न कोई हुनर है
न जानकारी
न वह रस्सी बर सकता है
न गांठ सकता है जूते
खटिया बुनना
बर्तन बनाना
मिट्टी तैयार करना
जैसे छोटे-छोटे काम भी
ईश्वर के बस में नहीं थे''
(ईश्वर के बारे में उसके पास पर्याप्त जानकारी थी।)
ऐसे ईश्वर का एक मेहनतकश के लिए क्या महत्व हो सकता है? सत्ता के लिए जो शोषण और उत्पीड़न का शस्त्र है वह आखिर एक मजलूम के लिए कितना अर्थपूर्ण होगाा। जाहिर सी बात है कि वह नकारात्मक ही होगा।
'ईश्वर अन्न के दाने के
भीतर वैठी पाई है
ईश्वर लकड़ी के भीतर
बैठी घुन है'
(जो इस धरती के खिलाफ है)
वह जीवन में संघर्षरत व्यक्ति के लिए भय है जिसका प्रयोग ब्राह्मणवादी पुरोहिती व्यवस्था सदियों से करती रही है। वह सत्ता के तरफ से फैलाया गया 'राज रोग' है। नरेन्द्र पुण्डरीक द्वारा प्रयुक्त शब्द 'राज रोग' के निहितार्थ गहरे और बहुआयामी हैं। अन्तत: ईश्वर वह सब कुछ है जो मनुष्यता के विरुध्द है अर्थात 'जो इस धरती के खिलाफ है।'
नरेन्द्र पुण्डरीक की ईश्वर संबंधी यह कम चर्चित कविता श्रृंखला विचारधारा के मामले में एक गंभीर हस्तक्षेप करती है। वह प्रगतिशीलता के नास्तिक दर्शन के रास्ते को वैसे ही रेखाकित करती है जैसे नागार्जुन की कविता। मगर यह बिल्कुल बदले हुए संदर्भों में ऐसा करती है। सीतामढ़ी के सांप्रदायिक दंगे का जिक्र करती उनकी कविता में ईश्वर निश्चित तौर पर हमारे समय के संदर्भ में हैं। सीतामढ़ी के सामान्य लोगों के सामान्य स्वप्न थे और उनकी इच्छाओं और संघर्षों में ईश्वर कहीं नहीं था।
'फिर भी वे मारे गये
ईश्वर के नाम पर
उनके जलाये गये घर
ईश्वर के नाम पर
ईश्वर जो कभी था ही नहीं
इस दुनिया में
केवल उसके होने को लेकर
क्यों मारे गये लोग''
यहां कविता में उपस्थित सीतामढ़ी भारत का कोई भी शहर हो सकता है और साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने वाले लोग कहीं भी ईश्वर के नाम पर दंगा करा सकते थे। ईश्वर ही उनके लिये वह माध्यम है जिसका इस्तेमाल वे मनुष्य के विरुध्द करते है, सामान्य जीवन का विध्वंस करते हुए।
'कुछ शब्द थे
जो ईश्वर की शक्ल से
बहुत कुछ मिलते जुलते थे
वे उतने ही घृणित
अपवित्र
और धारदार थे
जितना कि ईश्वर
इस वक्त इन शब्दाें से
सीतामढ़ी क्या
तरबूज की तरह
पूरी दुनिया काटी जा सकती है।'
हिन्दी जगत अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में निहायत ही परंपराग्रस्त रहा है। केवल कुछ लेखकों, संस्कृतिकर्मियों के होने से यह सिध्द नहीं होता कि सब कुछ क्रान्तिकारी है। परंपरा अभिविन्यस्त होने में सुरक्षा और मान्यता दोनों मिलती रही है। यही कारण है कि धर्म और ईश्वर की पुनरुत्थानी स्वीकृति यहां की संसदीय राजनीति में प्रतिफलित हुई। ऐसे में ईश्वर की सत्ताा को परंपरा के प्रवाह की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके प्रति शंका, प्रश्न अथवा विद्रोह को परोक्षत: एक पूरी सत्ताा के प्रति होने वाले विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। हिन्दी कविता में इधर उभरते ईश्वर को सिर्फ आज की तात्कालिक सांप्रदायिकता विरोधी राजनीति से अलग एक विशिष्ट ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मेें देखने पर उसका स्पष्ट अलगाव दिखाई पड़ता है। यह बात भी सच है कि इस प्रतिरोध की अपनी एक परंपरा है, ठीक वैसे ही जैसे कूपमंडूकता और जाहिल परंपरावाद की परंपरा है ही। इसी विवेक से जुड़ी प्राश्निकता की यह ईश निन्दक परंपरा रेखांकित करने योग्य है, भले ही यह धारा अल्पसंख्यक और गौण ही क्यों न हो।
ईश्वर और सत्ताा का प्रश्न हिन्दी कविता में विशिष्ब्ट तौर पर सांप्रदायिकता के सापेक्ष ही सामने आया, मगर वास्तव मेें यह सिर्फ सांप्रदायिकता के उभार भर से जुड़ा एक प्रश्न नहीं। यह उस पूरे अतार्किक के विरुध्द आवाज उठाने की बात है जो तरह-तरह से भारतीय समाज में रचा-बसा है। संस्कृति की अनेकों दैनन्दिन की गतिविधियों में यह अतार्किक विद्यमान रहता है और तमाम महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्नों को पृष्ठभूमि में ढकेलता है।
यदि ईश्वर का प्रत्यय हिन्दी के इन कवियों के लिए सिर्फ एक दार्शनिक प्रत्यय नहीं, तो वह राजनीतिज्ञों के लिए जिस प्रकार एक नीतिगत प्रश्न है वैसा भी नहीं। संसदीय राजनीति में धर्म और ईश्वर के कुटिल प्रयोग होते रहे हैं। सांप्रदायिक दक्षिणपंथी दल उसका सीधा इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितो के लिए करते रहे है। यहाँ तक कि टकराव और दंगों के रास्तों को भी नहीं छोड़ा गया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रकरण और गुजरात के दंगों के उदाहरण स्थूल और स्पष्टत: रेखांकित करने योग्य हैं, जिसका विरोध इस दौर की हिन्दी कविता ने जोरदार ढंग से किया। मगर धर्म निरपेक्ष राजनीति ने ईश्वर और धर्म की स्पष्ट आलोचना से बचने का ही प्रयास किया। यहॉ वोट प्राप्त करने के लिए यह एक मजबूरी थी। इस प्रकार के प्रयोग सभी राजनीतिक दलों नें किये हैं बस थोड़ा अलग अलग ढंग से।इस पगकार के 'हितसाधन' या 'स्वार्थसिध्दि' से समकालीन कवियों को कोई वास्ता नहीं रहा है हाँलांकि ऐसे कवियों की कविताएँ निहायत राजनीतिक रही है। यह तथ्य सीधी संसदीय राजनीति और नागरिक जीवन से जुड़ी राजनीति के फर्क को तो साफ रेखांकित करता ही है। कविता के सरोकार के व्यापकतर घेरे बनते हैं। यही कारण है कि कविता भक्तियुगीन सर्वशक्तिमान ईश्वर से मनुष्ब्श् में व्याप्त ईश्वर तक पहुँचकर रूक नहीं जाती। वह ईश्वर के एक छोटे से औजार के रूप् में परिवर्तित हो जाने के तथ्य कोउजागर करती है। इस अर्थ में समकालीन हिन्दी कविता हमारे हिन्दी समाज में छाये एक आध्यात्मिक रहस्यवाद का विखंडन करती है।
''लोग कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर ईश्वर
क्या वह बना सकता है एक ऐसा बड़ा ढोका
जिसे वह दाँत पीसकर स्वयं ही न उठा सके''
बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में ईश्वर के प्रति कविता में भाव बदलते गये हैं। भारतीय जनता पार्टी की धर्म को राजनीतिक हथकण्डे के रूप में अपनाने की नीति का सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ा । आस्तिक लोगों के ड्राइंग रूमों में आशीर्वाद देने की मुद्रा में अनामिका मोड़े खड़े राम के स्थान पर समुद्र को धमकाते धनुङ्ढ हाथ में ताने हुए राम के चित्र दिखाई देने लगे। संघी भाइयों के यहां तो ये चित्र अनिवार्यत: मिलने लगे जिसकी कलाकारी इस बात मे थी कि राम का क्रोध उनकी शक्तिशाली मांसपेसियों में झलकने लगा। भारत के सांप्रदायिक परिप्रेक्ष्य में यह बहुत स्पष्ट था कि 'जलधि जड़' मुसलामान ही थे। अभिवादन के लिए प्रयुक्त होने वाला राम का नाम आक्रामक और हिंसक 'जै श्रीराम' के भयानक उद्धोष मेंं बदल गया। ईश्वर के इस घटिया और स्थूल राजनीतिक प्रयोग ने किसी भी प्रकार के दार्शनिक उदात्ता के लिए स्पेस नहीं छोड़ा।
उत्पात के प्रारंभिक दौर में आयी मानबहादुर सिंह की कविता 'समकालीन ईश्वर की लाचारी' एक दूसरी अवस्थित से लिखी गयी कविता है । इस कविता का रचनाकाल वह समय है जब सांप्रदायिकता की गरज उतनी तेज नहीं थी इस कारण यह कविता अधिक महत्व की हो जाती है । यह कम पढ़ी गयी और लगभग अचर्चित कविता ईश्वर के दुरुप्योग और हिंसा से भरे माहौल में ईश्वर की लाचारी को दर्शाती है। इस मायने में ईश्वर के साथ 'समकालीन' पद का प्रयोग वाकई अर्थपूर्ण है। बाद में लिखी गयी वीरेन डंगवाल की कविता 'दुश्चक्र में स्रष्टा' से इस कविता को मिला कर देखा जा सकता है। यह कविता ईश्वर के पक्ष से प्रस्तुत एक अंधाधुंंध मोनोलाग है या कहें कि विवश ईश्वर का प्रलाप। यहां ईश्वर के मनुष्यता के विरोध में हुए प्रयोंगों को भर्त्सनात्मक ढंग से प्रदर्शित किया गया है।
वीरेन डंगवाल की कविता में 'दुश्चक्र में स्रष्टा' अपनी विडम्बनात्मक अभिव्यक्तियों के चलते महत्वपूर्ण है और इसी कारण उसने हिंदी के पाठकों और आलोचकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। कविता मे उपस्थित यह व्यंग्य और विडम्बना का स्वर कविता के अंत तक पहुंचते-पहुचते आक्रोश में बदल जाता है। 'दुश्चक्र में स्रष्टा' कविता का प्रारंभ भगवान के कारीगरी के कमाल के जिक्र के साथ होता है। समकालीन घटनाक्रम के सापेक्ष यह जिक्र व्यंग्य और विडम्बना के स्वर के साथ है।
'अरे, कुत्ते की उस पतली गुलाबी जीभ का ही क्या कहना!
कैसी रसीली और चिकनी टपकदार, सृष्टि के हर
स्वाद की मर्मज्ञ
और दुम की तो बात ही अलग
गोया एक अदृश्य पंखे की मूठ
तुम्हारे मुखड़े पर झलती हुई'
ईश्वर के शानदार कृत्यों का यह विडम्बनापूर्ण वर्णन इस शिकायत के साथ समय के यथार्थ तक पहुंचता है कि भगवान ने अपना कामयाब कारखाना बंद कर दिया है और अब जो कुछ भी इस तथाकथित ईश्वरीय सत्ता के नाम पर है वह बुरा ही बुरा है। क्या अच्छे और आश्चर्यजनक कार्य सम्पन्न करने वाला ईश्वर कहीं विलुप्त हो गया है? आखिर समकालीन तबाहियों के बीच 'रहमानुर्रहीम' या 'करूणानिधान'ईश्वर के अस्तित्व के कोई चिन्ह क्यों नहीं दिखाई पड़ते?
'बाढ़ें तो आयी खैर भरपूर, काफी भूकंप, तूफान
खून से लबालब हत्याकांड अलबत्ता हुए खूब
खूब अकाल, युध्द एक से एक तकनीकी चमत्कार
रह गयी सिर्फ एक सी भूख, लगभग एक सी फौजी
वर्दियां जैसे
मनुष्य मात्र की एकता प्रमाणित करने के लिए
एक जैसी हुंकार, हाहाकार!
प्रार्थना गृह जरूर उठाये गये एक से एक आलीशान!
मगर भीतर चिने हुए रक्त के गारे से
वे खोखले आत्माहीन शिखर-गुम्बद-मीनार
उंगली से छूते ही जिन्हें रिस आता है खून!
आखिर यह किनके हाथों सौंप दिया है ईश्वर
तुमने अपना इतना बड़ा करोबार?'
वीरेन डंगवाल की यह कविता ईश्वर के अस्तित्व और उसके कार्यों को लेकर प्रचलित मान्यताओं और परंपरागत विचारों से प्रारंभ होकर उन्हीं को प्रश्नांकित करती है।इयवर की अनुपस्थिति इस बात में है कि अब उसका इस विश्व पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।पर सवाल यह हुआ कि यदि इस पर उसका नियंत्रण नहीं तो फिर नियंत्रण है किसका। क्या ईश्वर की कोई वास्तविक सत्ता है भी या यह महज एक परंपरागत असत्य है? क्या ईश्वर नयी क्रूर सत्ताओं सा डर कर भाग गया है? शायद उसका इन क्रूर सत्ताओं से कोई परोक्ष-अपरोक्ष समझौता हो गया हो? कुल मिलाकर कवि के लिए ईश्वर असहनीय हो गया है। यही कानण है कि कविता आक्रोश के ऐसे बिन्दु पर समाप्त होती है जहाँ ईश्वर संबंधी सारी पारंपरिक अवधारणाएँ नष्ट हो जाती हैं।
'अपना कारखना बंद करके
किस घोसले में जा छिपे हो भगवान?
कौन सा है आखिर, वह सातवाँ आसमान?
हे, अरे, अबे, ओ करूणानिधान!!'
युवा कवि पंकज चतुर्वेदी की कविता 'ईसा, बुध्द, हज़रत मुहम्मद के लिए' ईश्वर और पैगम्बरों के नाम पर होने वाली हिंसा और मारकाट का खुलासा करती हुई उसके राजनीतिक प्रयोगों को रेखांकित करती है। भारत ने बुध्द पूर्णिमा के दिन पोकरण में परमाणु विस्फोट किया था तो संकेत का संदेश था 'बुध्द मुस्काराये'। यह विडम्बनापूर्ण संदेश इस ओर ले जाता है कि मनुष्य को नष्ट करने के ङ्ढडयंत्र में ईश्वर का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ ईश्वर की सत्ताा नगण्य है और महत्वपूर्ण है अमरीका, भारत ओर पाकिस्तान की शासन सत्तााएं जो बुध्द, ईसा और हजरत मोहम्मद का इस्तेमाल कर रहे है। यह यूं ही नहीं है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता और इस्लामिक बम के साथ-साथ हटिंगटन की पुस्तक भी आ पहुंची है। धर्म और नस्ल को वैधता देने मे ईश्वर कहीं न कहीं उपस्थित होता है।
ऋतुराज के कविता संग्रह 'लीलामुखारविन्द' में ईश्वर की उपस्थिति अनेक ठोस रूपों में दिखलाई पड़ती है। यह उसका कोई भक्तियुगीन साकार रूप नहीं है, मगर है कुछ वैसा ही। वह कहीं न होते हुए भी सर्वत्र उपस्थित है। सभी प्रकार के पापाचारों में वह शरीक है। यही वह लीला है जो सत्ता और शक्ति के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाकलापों में अन्तर्निहित है। ऋतुराज सत्ता के विभिन्न प्रकार के चेहरों के खेल में उसकी उपस्थिति पाते है- यही है 'लीला मुखारविन्द'। कविता 'ईश्वर चरितम्' में ईश्वर न होते हुए भी परेशानी का कारण है, क्योंकि वह तमाम सत्ता प्रतिष्ठानों और शक्ति केन्द्रों के लिए उपकरण बन गया है। प्रात: काल में बजने वाले भजनों से लेकर रात्रि तक, हर समय उसकी उपस्थिति है।
'हत्यारा हत्या करता है ईश्वर के नाम पर
हत्यारे के पक्ष में ईश्वर गवाही देता है
क्योंकि हर अपराध में उसका हाथ होता है।'
यह सब कुछ होते हुए भी ईश्वर नाम का यह 'मुख्य अभियुक्त अदृश्य' रहता है। इस प्रकार वह निराकार और साकार दोनों है। वास्तव मे यह सत्ता प्रतिष्ठानों का वह वर्चस्वी भ्रष्ट रूप है, जो ईश्वर का इस्तेमाल करता है। यहां ईश्वर तलवार भी है और ढाल भी। और कहीं-कहीं तो वह अदृश्य सत्ताानायक है जो स्वयं ही ईश्वर बन बैठता है। यह विडम्बना ही है। अपने समय के सांप्रदायिक और वर्चस्वी शक्तियाें को देखें तो वे ईश्वर सदृश ही हैं। यह ईश्वरत्व तो धरती पर ही साकार है और उसके ठोस रूप खूंखार और डरावने हैं।
''उनके हाथों में खून सनी छडे थी'
चाकू तेजाब की बोतलें भी
अनगिनत हाथ थे जैसे तुम्हारे ही हाथ हों वे''
'श्री ईश्वरचरितम्' कविता में ईश्वर इतना अधिक है कि कवि की नींद हराम है। वह ईश्वर को कोसता है। उसकी उपस्थिति अमानवीय है। ईश्वर के नाम पर सुबह से ही धूम-धड़ाका है। यह ढोंग तो है ही। अपने कुकर्मों को वैधता प्रदान करने का शक्तिपाठ है। ईश्वर ही वह प्रत्यय है जिसके द्वारा हत्याओं को वैधता दी जा सकती है। ईश्वर अदृश्य मुख्य अभियुक्त है। कविता की विडम्बना इस बात में है कि मुख्य अभियुक्त का दो अर्थ है। एक तो ईश्वर जो दिखाई नहीं देता और चारों तरफ है और दूसरी अर्थ है वह सत्ताा जो हर जगह शक्ति के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करता है। अपने दौर में राम के नाम पर हुए उत्पातों से जुड़ी दक्षिणपंथी शक्ति सत्ताा के सापेक्ष कविता का अर्थ बहुत साफ होता है। ईश्वर, धर्म और सत्ताा के इस क्रूर और अमानवीय गठजोड़ को यह कविता अपनी चिंता का विङ्ढय बनाती है।
सत्तााएं सदैव प्रत्ययों की मदद से शासन करती हैं और उन्हें अपनी वैधता सिध्द करने के लिए इस प्रकार के उपादानों की सदा ही आवश्यकता रहती है। यह किसी धर्म अथवा नस्ल की श्रेष्ठता से लेकर स्वतंत्रता तक का मुद्दा हो सकता है। बुश जैसे सत्तााधीश यदि इराक की जनता को मुक्त कराने के नाम पर आक्रमण को वैधता प्रदान करते हैं तो हिन्दू राष्ट्र और हिन्दुत्व की श्रेष्ठता का मुखौटा सत्तााछद्म पर पर्दे का काम करती है। इसी प्रकार 'देयर इज नो गाड बट अल्लाह' भी अपना काम करता है। ईश्वर सत्तााओं को किस प्रकार से वैधता प्रदान करता है इसका हमारे समय में इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि राम के नाम पर साम्प्रदायिकता के नंगे नृत्य को भी वैधता दी जाय। गुजरात के दंगों को उदार हिन्दुओं की स्वाभाविक प्रक्रिया कह कर बच चला जाय। हिन्दुओं की उदारता भी तो इसी बात द्वारा सिध्द की जाती है कि यहाँ असंख्य देवी-देवता है। अस्ल में इन देवी-देवताओं के पीछे सत्ताा एक ही है जिसके हजारों हाथ कहीं अदृश्य से प्रकट होकर जीवन घुस आते हैं और विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं।
मानववादी कविता से अलग इस नये तौर की कविता दृष्टि की महत्ताा इसी में है कि वह मनुष्य और ईश्वर की सत्ता को एक नहीं देखती। यह ईश्वर की अद्वितीय और सर्वशक्तिमान सत्ताा के प्रति भी मुग्ध नहीं। यह तो और पीछे की बात है। वह दरअस्ल ईश्वर को वर्चस्वी सत्ताा के एक प्रतिनिधि के रूप में देखती है जिसके विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते रहे हैं-खासकर भरतीय राजनीति में।
हिन्दी कविता में ईश्वर के प्रत्यय का यह इस्तेमाल अर्तक्य के विरोध में आता है। हमारे समय में उसकी एक ऐतिहासिक उपस्थिति है जिसे सांप्रदायिकता और फासीवाद के विरुध्द खड़े होते हुए देखा जा सकता है। यही कारण्ा है कि इन कविताओं मेें ईश्वर की चर्चा महज एक दार्शनिक प्रत्यय के रूप में नहीं है। यहाँ वह धर्म के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिफलनों मेें रेखांकित किया गया है। जाहिर तौर पर यह महज एक आस्था का प्रश्न नहीं बनकर रह जाता। इसके विभिन्न आयाम दिखलाई देते हैं। समाज संस्कृति में ईश्वर के प्रत्यय द्वारा एक मनुष्यता विरोधी वर्चस्वी व्यवस्था अथवा सत्ता की स्थापना का यहाँ स्पष्ट विरोध देखा जा सकता है।
प्रकृति और सामान्य जीवन की कविता लिखने वाले नरेन्द्र पुण्डरीक ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार कर पाते क्योंकि वह इश्वरीय सत्ता, आततायी सत्ता की समर्थक है ऐसे में ईश्वर की प्रार्थना के लिए शब्द कहां से आयेंगे।
''कैसे चुपचाप रोज
मेरे सपनों का रौंदता हुआ
आकाश से गुजर जाता है
इन्द्र का हाथी,
बताओ तुम्हारी सरोकारहीन
प्रार्थनाओं के लिए
कहां से जुटाऊं शब्द ईश्वर''
सत्ता और शक्ति के केन्द्र्र ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं और राम लोगों के हृदय से बाहर कैद में रह जाते हैं- अयोध्या को लेकर चलती राजनीति की कैद में। 'कैसे छीने गये राम' कविता में ऐसे विवश और शक्तिहीन ईश्वर का क्या किया जाय। इस फालतू ईश्वर के बारे में यदि जानकारियां हों भी तो किस काम की।
''ईश्वर के पास न कोई हुनर है
न जानकारी
न वह रस्सी बर सकता है
न गांठ सकता है जूते
खटिया बुनना
बर्तन बनाना
मिट्टी तैयार करना
जैसे छोटे-छोटे काम भी
ईश्वर के बस में नहीं थे''
(ईश्वर के बारे में उसके पास पर्याप्त जानकारी थी।)
ऐसे ईश्वर का एक मेहनतकश के लिए क्या महत्व हो सकता है? सत्ता के लिए जो शोषण और उत्पीड़न का शस्त्र है वह आखिर एक मजलूम के लिए कितना अर्थपूर्ण होगाा। जाहिर सी बात है कि वह नकारात्मक ही होगा।
'ईश्वर अन्न के दाने के
भीतर वैठी पाई है
ईश्वर लकड़ी के भीतर
बैठी घुन है'
(जो इस धरती के खिलाफ है)
वह जीवन में संघर्षरत व्यक्ति के लिए भय है जिसका प्रयोग ब्राह्मणवादी पुरोहिती व्यवस्था सदियों से करती रही है। वह सत्ता के तरफ से फैलाया गया 'राज रोग' है। नरेन्द्र पुण्डरीक द्वारा प्रयुक्त शब्द 'राज रोग' के निहितार्थ गहरे और बहुआयामी हैं। अन्तत: ईश्वर वह सब कुछ है जो मनुष्यता के विरुध्द है अर्थात 'जो इस धरती के खिलाफ है।'
नरेन्द्र पुण्डरीक की ईश्वर संबंधी यह कम चर्चित कविता श्रृंखला विचारधारा के मामले में एक गंभीर हस्तक्षेप करती है। वह प्रगतिशीलता के नास्तिक दर्शन के रास्ते को वैसे ही रेखाकित करती है जैसे नागार्जुन की कविता। मगर यह बिल्कुल बदले हुए संदर्भों में ऐसा करती है। सीतामढ़ी के सांप्रदायिक दंगे का जिक्र करती उनकी कविता में ईश्वर निश्चित तौर पर हमारे समय के संदर्भ में हैं। सीतामढ़ी के सामान्य लोगों के सामान्य स्वप्न थे और उनकी इच्छाओं और संघर्षों में ईश्वर कहीं नहीं था।
'फिर भी वे मारे गये
ईश्वर के नाम पर
उनके जलाये गये घर
ईश्वर के नाम पर
ईश्वर जो कभी था ही नहीं
इस दुनिया में
केवल उसके होने को लेकर
क्यों मारे गये लोग''
यहां कविता में उपस्थित सीतामढ़ी भारत का कोई भी शहर हो सकता है और साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने वाले लोग कहीं भी ईश्वर के नाम पर दंगा करा सकते थे। ईश्वर ही उनके लिये वह माध्यम है जिसका इस्तेमाल वे मनुष्य के विरुध्द करते है, सामान्य जीवन का विध्वंस करते हुए।
'कुछ शब्द थे
जो ईश्वर की शक्ल से
बहुत कुछ मिलते जुलते थे
वे उतने ही घृणित
अपवित्र
और धारदार थे
जितना कि ईश्वर
इस वक्त इन शब्दाें से
सीतामढ़ी क्या
तरबूज की तरह
पूरी दुनिया काटी जा सकती है।'
हिन्दी जगत अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में निहायत ही परंपराग्रस्त रहा है। केवल कुछ लेखकों, संस्कृतिकर्मियों के होने से यह सिध्द नहीं होता कि सब कुछ क्रान्तिकारी है। परंपरा अभिविन्यस्त होने में सुरक्षा और मान्यता दोनों मिलती रही है। यही कारण है कि धर्म और ईश्वर की पुनरुत्थानी स्वीकृति यहां की संसदीय राजनीति में प्रतिफलित हुई। ऐसे में ईश्वर की सत्ताा को परंपरा के प्रवाह की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके प्रति शंका, प्रश्न अथवा विद्रोह को परोक्षत: एक पूरी सत्ताा के प्रति होने वाले विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। हिन्दी कविता में इधर उभरते ईश्वर को सिर्फ आज की तात्कालिक सांप्रदायिकता विरोधी राजनीति से अलग एक विशिष्ट ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मेें देखने पर उसका स्पष्ट अलगाव दिखाई पड़ता है। यह बात भी सच है कि इस प्रतिरोध की अपनी एक परंपरा है, ठीक वैसे ही जैसे कूपमंडूकता और जाहिल परंपरावाद की परंपरा है ही। इसी विवेक से जुड़ी प्राश्निकता की यह ईश निन्दक परंपरा रेखांकित करने योग्य है, भले ही यह धारा अल्पसंख्यक और गौण ही क्यों न हो।
ईश्वर और सत्ताा का प्रश्न हिन्दी कविता में विशिष्ब्ट तौर पर सांप्रदायिकता के सापेक्ष ही सामने आया, मगर वास्तव मेें यह सिर्फ सांप्रदायिकता के उभार भर से जुड़ा एक प्रश्न नहीं। यह उस पूरे अतार्किक के विरुध्द आवाज उठाने की बात है जो तरह-तरह से भारतीय समाज में रचा-बसा है। संस्कृति की अनेकों दैनन्दिन की गतिविधियों में यह अतार्किक विद्यमान रहता है और तमाम महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्नों को पृष्ठभूमि में ढकेलता है।
यदि ईश्वर का प्रत्यय हिन्दी के इन कवियों के लिए सिर्फ एक दार्शनिक प्रत्यय नहीं, तो वह राजनीतिज्ञों के लिए जिस प्रकार एक नीतिगत प्रश्न है वैसा भी नहीं। संसदीय राजनीति में धर्म और ईश्वर के कुटिल प्रयोग होते रहे हैं। सांप्रदायिक दक्षिणपंथी दल उसका सीधा इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितो के लिए करते रहे है। यहाँ तक कि टकराव और दंगों के रास्तों को भी नहीं छोड़ा गया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रकरण और गुजरात के दंगों के उदाहरण स्थूल और स्पष्टत: रेखांकित करने योग्य हैं, जिसका विरोध इस दौर की हिन्दी कविता ने जोरदार ढंग से किया। मगर धर्म निरपेक्ष राजनीति ने ईश्वर और धर्म की स्पष्ट आलोचना से बचने का ही प्रयास किया। यहॉ वोट प्राप्त करने के लिए यह एक मजबूरी थी। इस प्रकार के प्रयोग सभी राजनीतिक दलों नें किये हैं बस थोड़ा अलग अलग ढंग से।इस पगकार के 'हितसाधन' या 'स्वार्थसिध्दि' से समकालीन कवियों को कोई वास्ता नहीं रहा है हाँलांकि ऐसे कवियों की कविताएँ निहायत राजनीतिक रही है। यह तथ्य सीधी संसदीय राजनीति और नागरिक जीवन से जुड़ी राजनीति के फर्क को तो साफ रेखांकित करता ही है। कविता के सरोकार के व्यापकतर घेरे बनते हैं। यही कारण है कि कविता भक्तियुगीन सर्वशक्तिमान ईश्वर से मनुष्ब्श् में व्याप्त ईश्वर तक पहुँचकर रूक नहीं जाती। वह ईश्वर के एक छोटे से औजार के रूप् में परिवर्तित हो जाने के तथ्य कोउजागर करती है। इस अर्थ में समकालीन हिन्दी कविता हमारे हिन्दी समाज में छाये एक आध्यात्मिक रहस्यवाद का विखंडन करती है।
''लोग कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर ईश्वर
क्या वह बना सकता है एक ऐसा बड़ा ढोका
जिसे वह दाँत पीसकर स्वयं ही न उठा सके''
Wednesday, October 08, 2008
ईश्वर, सत्ता और कविता 3
ईश्वर, सत्ता और कविता 3
चिन्तन की एक खास अवस्था में ईश्वर के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगने शुरू होते हैं और नास्तिक दर्शन का प्रारंभ होता है। भारत में भगत सिंह के प्रसिध्द लेख '' मैं नास्तिक क्यों हूँ'' से अधिकांश पाठक परिचित होंगे। यह नास्तिकता एक तरह की प्रश्नाकुलता का परिणाम होती है। ऐसी प्रश्नाकुलता जिसके पीछे कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ कार्य करती है। एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है तार्किकता की तलाश जो एक वैज्ञानिक दृष्टि का परिणाम होती है। ईश्वर प्रत्यय को लेकर होने वाली तमाम बहसाें के पीछे इसी तार्किकता की तलाश है जो किसी तथ्य को विवके सम्मत और स्वीकृति योग्य बनाता है। आध्यात्म ने सदैव इस प्रकार की तार्किक और परीक्षणधर्मी प्रवृत्ति का विरोध किया है ओर उसे सीमाबध्द बतलाने की चेष्टा की है।
इस प्रकार की प्रश्नाकुलता के चलते ही आर्य समाज एक दौर मेें ईश्वर से जुड़े ढोंगों का विरोध करता था। मगर यह विरोध अन्तत: नये किस्म के आध्यात्म में जाकर निपट गया। फिर भी यह ध्यातव्य है कि नवजागरण के प्रारंभ की यह प्रश्नाकुलता अपना महत्व रखती है जिसके तार्किक तत्व हिन्दी कविता मे तरह-तरह से उभरते है। 'देवी चबूतरा' जैसी कविता आध्यात्म के दैवीय प्रतिफलन पर चोट करती है। देवी चबूतरा पूजा का एक स्थानीय केन्द्र है लेकिन देवी जी अपने चबूतरे पर पेशाब और संभोग करने वाले कुत्ताों को भगाने तक की सामर्थ्य नहीं रखतीं।पंकज चतुर्वेदी आर्यसमाजी कवि नहीं मगर आर्यसमाजी खण्डन-मण्डन का ही यह विस्तार एक आधुनिक प्रगतिशीलता की ओर ले जाता है और ऐसे तत्व हिन्दी की बहुत सी कविताओं में विद्यमान है।
यही प्रश्नाकुलता अपने आधुनिक शिल्प में विडंबनापूर्ण हो जाती है जब शंकाएँ अविश्वास में बदलती हैं और ढोंग का विरोघ करती हैं। संजय चतुर्वेदी की कविता 'पानी में नबूवत' धर्म और ईश्वर की विसंगतिपूर्ण स्थिति को अपने संरचना के एब्सर्ड में प्रस्तुत करती है। यह संजय चतुर्वेदी के प्रारंभिक दौर की कविताओं मेें से एक है जब वे विसंगतियों के बरक्स कविता में उलट-पुलट कर रहे थे। यह कविता इण्डिया टुडे वर्ङ्ढ 1993 की वार्ङ्ढिकी में प्राकाशित हुई थी। बाद में उन्होंने यह शैली त्याग दी ओर आसानी से संप्रेङ्ढित हो सकने वाली कविताएं लिखी। 'पानी मे नबूवत' ईश्वर और धर्म सम्बन्धी सामान्यत: प्रचलित बातों को उलट-पुलट कर उनमें बैठे अतार्किक तत्वों को सामने लाती है। अर्थात विरुपों का विरुपण। कविता अपने अतारतम्य में ईश्वर की उपस्थिति उसकी तथाकथित तारतम्यता का मजाक उड़ाती है और सब कुछ एक झकझकी सा लगता है।
'सृष्टिकर्ता का दूरदर्शन बूंदों से उतरता है घास पर
सताई हुई धरती पर इलहाम बरसता है।''
खुदा को पाने का रास्ता मसखरी है, ईश्वर ने अवतार नहीं लिया मगर उस पर श्रीमद्भगवत् कृपा रही होगी। 'पालक और सृष्टिपालक का समुचित सेवन/दीन और दुनिया दोनों को फिट रखता है'। फिर खुदा के होते हुए धरती पर सभी नेक लोग पीड़ित है और दुष्ट लोग सुखी तो जरूर वह खुदा अखबार नहीं पढ़ता होगा। कवि छोटा मोटा नबी होता है तो उसकी कविता में नबूवत गर्म तवे पर रखी वर्फ से निकलती भाप की तरह होती है। प्रकृति ईश्वर का काव्य है- वगैरह, वगैरह। कविता के लगभग अराजक माहौल में धार्मिक विचारों की अराजकता बेपर्दा होती है और ईश्वर को लेकर फैलायी गयी वैचारिक बाजीगीरी भूलुंठित होती है। संजय चतुर्वेदी की यह जटिल और कम पढ़ी गयी कविता धर्म और ईश्वर से जुड़ी अवधारणाओं को विखण्डित करने वाली है।
चिन्तन की एक खास अवस्था में ईश्वर के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगने शुरू होते हैं और नास्तिक दर्शन का प्रारंभ होता है। भारत में भगत सिंह के प्रसिध्द लेख '' मैं नास्तिक क्यों हूँ'' से अधिकांश पाठक परिचित होंगे। यह नास्तिकता एक तरह की प्रश्नाकुलता का परिणाम होती है। ऐसी प्रश्नाकुलता जिसके पीछे कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ कार्य करती है। एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है तार्किकता की तलाश जो एक वैज्ञानिक दृष्टि का परिणाम होती है। ईश्वर प्रत्यय को लेकर होने वाली तमाम बहसाें के पीछे इसी तार्किकता की तलाश है जो किसी तथ्य को विवके सम्मत और स्वीकृति योग्य बनाता है। आध्यात्म ने सदैव इस प्रकार की तार्किक और परीक्षणधर्मी प्रवृत्ति का विरोध किया है ओर उसे सीमाबध्द बतलाने की चेष्टा की है।
इस प्रकार की प्रश्नाकुलता के चलते ही आर्य समाज एक दौर मेें ईश्वर से जुड़े ढोंगों का विरोध करता था। मगर यह विरोध अन्तत: नये किस्म के आध्यात्म में जाकर निपट गया। फिर भी यह ध्यातव्य है कि नवजागरण के प्रारंभ की यह प्रश्नाकुलता अपना महत्व रखती है जिसके तार्किक तत्व हिन्दी कविता मे तरह-तरह से उभरते है। 'देवी चबूतरा' जैसी कविता आध्यात्म के दैवीय प्रतिफलन पर चोट करती है। देवी चबूतरा पूजा का एक स्थानीय केन्द्र है लेकिन देवी जी अपने चबूतरे पर पेशाब और संभोग करने वाले कुत्ताों को भगाने तक की सामर्थ्य नहीं रखतीं।पंकज चतुर्वेदी आर्यसमाजी कवि नहीं मगर आर्यसमाजी खण्डन-मण्डन का ही यह विस्तार एक आधुनिक प्रगतिशीलता की ओर ले जाता है और ऐसे तत्व हिन्दी की बहुत सी कविताओं में विद्यमान है।
यही प्रश्नाकुलता अपने आधुनिक शिल्प में विडंबनापूर्ण हो जाती है जब शंकाएँ अविश्वास में बदलती हैं और ढोंग का विरोघ करती हैं। संजय चतुर्वेदी की कविता 'पानी में नबूवत' धर्म और ईश्वर की विसंगतिपूर्ण स्थिति को अपने संरचना के एब्सर्ड में प्रस्तुत करती है। यह संजय चतुर्वेदी के प्रारंभिक दौर की कविताओं मेें से एक है जब वे विसंगतियों के बरक्स कविता में उलट-पुलट कर रहे थे। यह कविता इण्डिया टुडे वर्ङ्ढ 1993 की वार्ङ्ढिकी में प्राकाशित हुई थी। बाद में उन्होंने यह शैली त्याग दी ओर आसानी से संप्रेङ्ढित हो सकने वाली कविताएं लिखी। 'पानी मे नबूवत' ईश्वर और धर्म सम्बन्धी सामान्यत: प्रचलित बातों को उलट-पुलट कर उनमें बैठे अतार्किक तत्वों को सामने लाती है। अर्थात विरुपों का विरुपण। कविता अपने अतारतम्य में ईश्वर की उपस्थिति उसकी तथाकथित तारतम्यता का मजाक उड़ाती है और सब कुछ एक झकझकी सा लगता है।
'सृष्टिकर्ता का दूरदर्शन बूंदों से उतरता है घास पर
सताई हुई धरती पर इलहाम बरसता है।''
खुदा को पाने का रास्ता मसखरी है, ईश्वर ने अवतार नहीं लिया मगर उस पर श्रीमद्भगवत् कृपा रही होगी। 'पालक और सृष्टिपालक का समुचित सेवन/दीन और दुनिया दोनों को फिट रखता है'। फिर खुदा के होते हुए धरती पर सभी नेक लोग पीड़ित है और दुष्ट लोग सुखी तो जरूर वह खुदा अखबार नहीं पढ़ता होगा। कवि छोटा मोटा नबी होता है तो उसकी कविता में नबूवत गर्म तवे पर रखी वर्फ से निकलती भाप की तरह होती है। प्रकृति ईश्वर का काव्य है- वगैरह, वगैरह। कविता के लगभग अराजक माहौल में धार्मिक विचारों की अराजकता बेपर्दा होती है और ईश्वर को लेकर फैलायी गयी वैचारिक बाजीगीरी भूलुंठित होती है। संजय चतुर्वेदी की यह जटिल और कम पढ़ी गयी कविता धर्म और ईश्वर से जुड़ी अवधारणाओं को विखण्डित करने वाली है।
Tuesday, October 07, 2008
ईश्वर, सत्ता और कविता 2
ईश्वर, सत्ता और कविता 2
ईश्वर और धर्म को लेकर प्रचलित मानववादी दृष्टि का हिन्दी कविता में अभाव नहीं। गांधीवाद के दौर मेें इस व्यापक दृष्टि की राजनीति भी बड़ी व्यापक थी जिसका सैध्दान्तिक प्रतिफलन 'सर्वधर्म समभाव' में देखा गया। धर्म निरपेक्षता का यह व्यापक तौर पर स्वीकृत रूप था और यह रूप उस समय के साहित्य मेंे पर्याप्त दृष्टिगोचर है। सांप्रदायिकता के विरुध्द लड़ने का यह भी एक शस्त्र रहा। अपने व्यापक परिप्रेक्ष्य के चलते यह एक सकारात्मक विजन भी बना रहा जिसके तहत मनुष्य को ईश्वर में और ईश्वर को मनुष्य में देख पाने की अवधारणा विकसित हुई। यह विजन इतना पुराना है कि इसकी परिपाटी भक्ति युग के सूफी और निर्गुण कवियों तक जायेगी। यदि थोड़ी जबर्दस्ती की जाय तो वेद से भी प्रारंभ किया जा सकता है - अर्थात कविता के प्रारंभ से ही प्रारंभ।
लेकिन इन मानववादी कवियाें की तुलना वैदिक अथवा भक्ति युग के कवियो से करना गलता होगा। ईश्वर की सम्पूर्ण सत्ताा और उसके आगे निरा समर्पित रहने वाला भक्तिभाव इन कवियो में नहीं। न ही यह ईश्वर उनकी कविता का केन्द्रीय विङ्ढय बनता है जैसा कि भक्ति युग के साहित्य में है। नवजागरण पर चल रही सारी खींचा-तानी के बाद भी यह स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि ईश्वर प्रत्यय सम्बन्धी दार्शनिक सोच के मामले में भक्ति कवि, सन्त अगस्ताइन जैसे यूरोपियन मध्ययुगीनों से बहुत आगे नहीं। मगर ये मानवतावादी कवि तो आधुनिकता में पाँव डाले हुए हैं। भक्तियुग की अन्तिम परछायीं हिन्दी साहित्य में निराला की कविता में दिखलायी पड़ती है और वहीं से उससे मुक्त होने का मार्ग भी दृष्टिगोचर होता है। वैसे निराला स्वयं भक्ति के कवि तो कतई नहीं। भक्ति है भी तो छायावाद और आधुनिकता के फार्मे में। अत: इस पूरे विश्लेङ्ढण में निराला से पहले के समय में जाने की जरूरत नहीं महसूस होती।
इस मानववादी दृष्टि की विशेङ्ढता यह है कि इस दार्शनिक अवस्थिति में ईश्वर की सत्ता मनुष्य की सत्ता से जुड़ जाती है। हरिजन, दलित, मजदूर, किसानों में ईश्वर की प्राप्ति इसी अर्थ मे है और रवीन्द्रनाथ टैगोर ऐसी कविताएं लिखने वाले एकमात्र कवि नहीं। ऐसी कविताएं हिन्दी में कम नहीं जिनमें मनुष्य को ईश्वर का रूप बतलाया गया हो और उसकी अवहेलना करके होने वाली ईश्वर भक्ति को पाखण्ड और ढोंग बताया गया हो। ईश्वर की इस मानवीय सत्ता के दर्शन की आवश्यकता हमारे समय में साम्प्रदायिकता के बरक्स बार-बार दिखाई दी और धर्मनिरपेक्षता के समर्थकों द्वारा बार-बार पीछे जाकर इन कवियों में अपनी परंपरा तलाशने की बेचैनी इसी का प्रतिफलन है। यह देखने की बात है कि टैगोर एक तरफ ईश्वर को सामान्य जनता में तलाशते हैं तो दूसरी तरफ साम्प्रदायिकता के अंधकार को भाई-भाई के बीच हो रहे अज्ञानतापूर्ण अनुचित संघर्ङ्ढ के रूप में देखते है। ये दोनाें विचार दार्शनिक संस्तर पर नाभिनाल बध्द हैं।
राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से प्रादुर्भूत साम्प्रदायिक वैमनस्य के दौर मे इस दृष्0श्निV की ओर पुनर्वापसी स्वाभाविक थी। अनिल सिंह अपनी बहुचर्चित कविता 'अयोध्या' में उसे इस प्रकार रखते हैं।
'' मनुष्; रहते हैं इस शहर में
जिनमें रहता है भगवान
और चूंकी भगवान मनुष्; में रहता है
इसलिए वह अल्लाह भी हो सकता है''
फिर मनुष्; और उसका सामान्य नागरिक जीवन ईश्वर से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि-
''इतना ही यथार्थ है यह शहर जितना यह कि
आदमी का कलेजा काटकर उसकी जगह
शिवलिंग रख देने से वह मर जायेगा''
ईश्वर और मनुष्य की सत्ताा का एकाकार होना मानववादी कविता की एक प्रमुख विशेङ्ढता है। यह भी कहा जा सकता है कि इस कविता में मनुष्य ही ईश्वर हो जाता है। आगे चलें तो यह तथ्य सामने आता है कि मनुष्य के तिरस्कार पर ईश्वर और उसकी भक्ति ही निरर्थक हो जाती है। ऐसे में उसके प्रति भक्ति या श्रध्दा का कोई महत्व नहीं। बाह्याडम्बरों पर हुए आक्रमण इसी के चलते हैें। देखें तो ईश्वर और धर्म के प्रति यही सोच भारत मेें धर्मनिरपेक्षता का मूल बनती है और जिसके कुछ तत्व भक्ति युग में प्राप्त होते हैं। मनुष्य के कारण ही तो ईश्यर का अस्तित्व है वगर्ना धर्म का सारा ताना-बाना बेकार है। आध्यात्म के अखण्ड भाव में पूरे विश्व का समा जाना जरूरी है और मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे।
इस मानववाद की अभिव्यक्ति हमारे समय की साम्प्रदायिकता विरोधी हिन्दी कविता में तरह-तरह से हुई। नवल शुक्ल स्वयं को ईश्वर से अधिक पाते है क्योंकि ईश्वर युगों में पृथ्वी की सुधि लेते हैं जबकि कवि (मनुष्य) ''किसी भी जगह जनम लेकर'' पूरे ब्रह्माण्ड के बारे में सोचता है और ''अपनी क्षमता से अधिक रहने की कोशिश करता'' है। साम्प्रदायिकता के इस विकट दौर से पहले आने वाले कवि सर्वेश्वर के लिए-
'' इस दुनिया में
आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है
न ईश्वर
न ज्ञान
न चुनाव
न संविधान
इसके नाम पर कागज पर लिखी कोई भी इबारत
फाड़ी जा सकती है
और जमीन के भीतर गाड़ी जा सकती है''
केदारनाथ सिंह की कविताओं में ईश्वर का जिक्र एक मुहावरे के रूप में आता है। ऐसा सिर्फ केदारनाथ सिंह की कविता में नहीं अपितु बहुत से अन्य कवियों की भी कविताओं में है। वहां यह 'ईश्वर' एक भाव बोधक शब्द भी है, जो कविता से बाहर जीवन में घनघोर प्रचलन रखता है। इस अर्थ में यह शब्द 'ईश्वर' के दार्शनिक अथवा धार्मिक अर्थ सन्दर्भों से बिल्कुल अलग अस्तित्वमान है। 'हे राम' या 'राम नाम सत्य है' या 'खुदा कसम' जैसे वाक्यांशाें की तरह यह भाङ्ढा में विद्यमान है। यह एक जटिल प्रश्न है कि यह सत्ताा भाङ्ढा के इस प्रकार के स्वतंत्र लगने वाले प्रयोगों मेें किस प्रकार लगातार क्रियाशील करती है? इस लगातार बरकरार भाङ्ढायी तत्व में क्या कहीं दार्शनिक प्रत्ययों को भी वैधता तो नहीं प्राप्त होती? कैन्टरबरी के एनसेल्म ने ईश्वर के अस्तित्वमान होने का प्रमाण देते हुए कहा था कि 'ईश्वर' शब्द का होना ही उसके अस्तित्वमान होने का सबूत है। यह सत्ताा शब्दों के माध्यम से बनी रहती है। मेरे एक उर्दू पढ़ाने वाले मित्र ने बताया था कि किस प्रकार प्रारंभिक कक्षाओं में भाङ्ढा ज्ञान कराते समय ही बच्चों को शब्दों के माध्यम से ईश्वर और धर्म की घुट्टी पिला दी जाती है। लेकिन ईश्वर को गंभीरतापूर्वक न लेने वालों के बीच भी ईश्वर शब्द बना रहता है और प्रयोग से बाहर नहीं होता। यही वजह है कि ईश्वर संबन्धी कविताओं के गहरे अर्थों तक पहुंचने की जरूरत महसूस होती है।
मुहावरे की ही तरह ही ईश्वर के प्रति प्रार्थना के शिल्प में लिखी गयीं कविताएं किस प्रकार प्रार्थना की सीमा से बाहर निकलती है उसका उदाहरण है निराला की वे अन्तिम कविताएं जो सिर्फ प्रार्थनाएं न होकर स्वातंत्रोत्तर भारत की बदलती परिस्थितियाें में एक संवेदनशील कवि के मोहभंग की विशिष्ट कोटि की अभिव्यक्ति है। इस विङ्ढय पर कवि एवं आलोचक केदारनाथ सिंह ने एक बहुत प्रभावशाली लेख लिखा है। निराला अपनी इन कविताओं में ईश्वर के संदर्भ को अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर सूक्ष्म राजनीतिक अर्थ प्रदान करते हैैं।
'जय तुम्हारी देख भी ली
रूप की गुण की, सुरीली।
वृध्द हूँ मैं, ऋध्दि की क्या,
साधना की, सिध्दि की क्या?
खिल चुका है फूल मेरा,
पखड़ियाँ हो गयीं ढीली।
चढ़ी थी जो ऑंख मेरी,
बज रही थी जहाँ भेरी,
वहाँ सिकुड़न पड़ चुकी है,
बढ़ रही है रेख नीली।
आग सारी फुक चुकी है,
रागिनी वह रुक चुकी है,
याद करता हुआ जीवन,
जीर्ण जर्जर आज तीली।'
यही प्रार्थना का सबवर्जिव काव्य प्रारूप किस प्रकार ईश्वर के प्रति नकारात्मक रुख अख्तियार करता है यह यदि देखना हो तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 'ईश्वर' पर लिखित कविता देखने योग्य होगी। 'गर्म हवाएं' संग्रह में आयी यह कविता ऐसी अन्य कविताओं से घिरी है जो कवि के अपने व्यक्तिगत दु:खों, सामाजिक मोहभंग और व्यथित चुनावों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। संग्रह 'धीरे-धीरे' जैसी राजनीतिक कविता से प्रारंभ होता है जिसमें सर्वेश्वर एक 'क्रांतियात्रा' को 'शवयात्रा' में बदलते हुए देखते हैं। पत्नी की मृत्यु पर लिखी गयी एक अत्यन्त ही भावपूर्ण कविता के बाद आती है प्रार्थना कविताओं की ऋृंखला जिनमें कवि ईश्वर से शक्ति नहीं मांगता (प्रार्थना-1) 'दुर्गम पथ' मांगता है जिस पर उसके 'थके चरण' हों (प्रार्थना-2), अपनी सीमाओं का ध्यान और दुर्बलताओं का अभियान मांगता है (प्रार्थना-3)। पर अपनी कविता 'प्रार्थना-4' में वह ईश्वर का लगभग निङ्ढेध करता है।
'यही प्रार्थना है प्रभु तुमसे
जब हारा हूं तब न आइये।'
कवि अपने शौर्य की तो सराहना चाहता है, मगर वह ईश्वर के चरणों में नहीं गिरना चाहता। वह जानता है कि संसार में दु:ख की ऑंखें बहुत बड़ी है और उसके एक अश्रु की आयु के सामने कल्पचक्र अस्वीकार्य है। और इन प्रार्थनाओं के बाद आती है कविता 'ईश्वर'। सर्वेश्वर की यह कविता निश्चित रूप से दु:ख से भीगी हुई है। व्यक्तिगत दु:ख और मोहभंग से घिरी हुई यह कविता ईश्वर को एक ठोस रूप में प्रस्तुत करती है जो एक व्यापारी या बॉस की तरह 'बहुत लम्बी जेबों वाला कोट' पहनकर आता है और कवि की माँ, पिता, पत्नी और बच्चे को खिलौनों की तरह जेब में रखकर चला जाता है। कवि के लिए दुनियाँ छोड़ जाता है, जिसमें उसे बहलाने के लिए और बहुत से खिलौने हैं। आगे कवि लिखता है,
'मैंने सुना है
उसने कहीं खोल रखी है
खिलौनो की दूकान,
अभागे के पास
कितनी जरा सी पूँजी है
रोजगार चलाने के लिए।'
एक खिलौने के व्यापारी के रूप में ईश्वर का अवमूल्यन उसे हास्यास्पद बना देता है। ईश्वर की इतनी ठोस उपस्थिति सिर्फ उसके लम्बे कोट की वजह से बन पड़ी है, जो प्रभु की इमेज को इस कविता में सुनिश्चित करता है। यह सर्वेश्वर की प्रार्थना श्रृंखला की कविताओं में उपस्थित पारंपरिक प्रार्थनाभाव की बची-खुची संभावनाओं को भी ध्वस्त कर देता है और उनमें निहित दूसरे प्रतिरोधी भावों को आलोकित करता है। यह प्रश्न भी उठता है कि वह जो कुछ भी है- ईश्वर है भी या कोई और। सर्वेश्वर की ये कविताएं उस अस्पष्ट भूमि पर खड़ी है, जहाँ ईश्वर सत्ता का प्रतीक बनता दिखाई देता है। ईश्वर की सत्ता के प्रति प्रार्थना के ही शिल्प में व्यंगाात्मक सूक्ष्म कटाक्ष भरे प्रयोग किस प्रकार प्रभावपूर्ण हो सकते हैं इसका एक उदाहरण है शमशेर बहादुर सिेह की द्वारा भजन के शिल्प में प्रस्तुत यह कविता:
हरि मोरी आड़, हरि ही मोरी आड़॥
हरि मोरी झाँकी, हरि ही केंवाड़॥
हरि जमुना-मंथन मोरे, हरि ही
थाम्हे दुख के पहाड़॥
हरि संग ज्ञान-ध्यान मोहे मधुऋतु
हरि बिन सकल उजाड़॥
मज्जा-भेद बसे हरि अंतर
हरि संबल मोरे हाड़॥
जग बाड़व में जनम-जनम लौं
झोंक्यों कितने भाड़॥
तब आयो समसेरु मुकति को
परलौ मास असाढ़॥
हरि मोरी आड़, हरि ही मोरी आड़॥
सांप्रदायिक उन्माद के भीषण दौर से पूर्वं, अर्थात 1990 से पहले के समय की समकालीन हिन्दी कविता में ईश्वर की उपस्थिति की तुलना मेें बाद की कविताओं में उसकी उपस्थिति काबिले गौर है। स्वप्निल श्रीवास्तव की कविताओं मे ईश्वर की उपस्थिति एक वैचाारिक द्वंद्व का परिणाम है। 'ईश्वर एक लाठी है' कविता इस अर्थ में ध्यातव्य है। यहां कवि अपने पिता जैसे बूढे लोगाें के लिए ईश्वर के निहितार्थ को समझने की कोशिश करता है। इस कविता में यदि पिता के ईश्वर में विश्वास के प्रति सहानुभूति है तो उस विश्वास की व्यर्थता का भी एहसास है। ईश्वर पिता के लिए एक ऐसी लाठी है जिसे वे अक्सर तान देते है। उन्होंने इस लाठी को जिन्दगी भर मजबूत रखने की कोशिश की है, मगर उन्हें लाठी में घुन के चालने की आवाज सुनायी देती है। अपनी जीवन भर की आस्था के बाद भी वे यह नहीं जान सके हैं कि ईश्वर आखिर किस कोठ की लाठी है। स्वप्निल श्रीवास्तव की इस कविता के तमाम निहितार्थ निकलते हैं, विशेषरूप से इस कारण कि कवि के काव्यानुशासन में कविता के अर्थ एक दिशा में चलते हुए भी विभिन्न संस्तरों पर खुलते है। एक आस्तिक पिता के द्वंद को यह बखूबी रेखांकित करने वाली कविता है जिसके लिए ईश्वर एक ऐसा सहारा है जो कमजोर होता जा रहा है, मगर जिसे त्याग पाना उसके तर्क स्वभाव में कहीं दूर-दूर तक नहीं।
ईश्वर और धर्म को लेकर प्रचलित मानववादी दृष्टि का हिन्दी कविता में अभाव नहीं। गांधीवाद के दौर मेें इस व्यापक दृष्टि की राजनीति भी बड़ी व्यापक थी जिसका सैध्दान्तिक प्रतिफलन 'सर्वधर्म समभाव' में देखा गया। धर्म निरपेक्षता का यह व्यापक तौर पर स्वीकृत रूप था और यह रूप उस समय के साहित्य मेंे पर्याप्त दृष्टिगोचर है। सांप्रदायिकता के विरुध्द लड़ने का यह भी एक शस्त्र रहा। अपने व्यापक परिप्रेक्ष्य के चलते यह एक सकारात्मक विजन भी बना रहा जिसके तहत मनुष्य को ईश्वर में और ईश्वर को मनुष्य में देख पाने की अवधारणा विकसित हुई। यह विजन इतना पुराना है कि इसकी परिपाटी भक्ति युग के सूफी और निर्गुण कवियों तक जायेगी। यदि थोड़ी जबर्दस्ती की जाय तो वेद से भी प्रारंभ किया जा सकता है - अर्थात कविता के प्रारंभ से ही प्रारंभ।
लेकिन इन मानववादी कवियाें की तुलना वैदिक अथवा भक्ति युग के कवियो से करना गलता होगा। ईश्वर की सम्पूर्ण सत्ताा और उसके आगे निरा समर्पित रहने वाला भक्तिभाव इन कवियो में नहीं। न ही यह ईश्वर उनकी कविता का केन्द्रीय विङ्ढय बनता है जैसा कि भक्ति युग के साहित्य में है। नवजागरण पर चल रही सारी खींचा-तानी के बाद भी यह स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि ईश्वर प्रत्यय सम्बन्धी दार्शनिक सोच के मामले में भक्ति कवि, सन्त अगस्ताइन जैसे यूरोपियन मध्ययुगीनों से बहुत आगे नहीं। मगर ये मानवतावादी कवि तो आधुनिकता में पाँव डाले हुए हैं। भक्तियुग की अन्तिम परछायीं हिन्दी साहित्य में निराला की कविता में दिखलायी पड़ती है और वहीं से उससे मुक्त होने का मार्ग भी दृष्टिगोचर होता है। वैसे निराला स्वयं भक्ति के कवि तो कतई नहीं। भक्ति है भी तो छायावाद और आधुनिकता के फार्मे में। अत: इस पूरे विश्लेङ्ढण में निराला से पहले के समय में जाने की जरूरत नहीं महसूस होती।
इस मानववादी दृष्टि की विशेङ्ढता यह है कि इस दार्शनिक अवस्थिति में ईश्वर की सत्ता मनुष्य की सत्ता से जुड़ जाती है। हरिजन, दलित, मजदूर, किसानों में ईश्वर की प्राप्ति इसी अर्थ मे है और रवीन्द्रनाथ टैगोर ऐसी कविताएं लिखने वाले एकमात्र कवि नहीं। ऐसी कविताएं हिन्दी में कम नहीं जिनमें मनुष्य को ईश्वर का रूप बतलाया गया हो और उसकी अवहेलना करके होने वाली ईश्वर भक्ति को पाखण्ड और ढोंग बताया गया हो। ईश्वर की इस मानवीय सत्ता के दर्शन की आवश्यकता हमारे समय में साम्प्रदायिकता के बरक्स बार-बार दिखाई दी और धर्मनिरपेक्षता के समर्थकों द्वारा बार-बार पीछे जाकर इन कवियों में अपनी परंपरा तलाशने की बेचैनी इसी का प्रतिफलन है। यह देखने की बात है कि टैगोर एक तरफ ईश्वर को सामान्य जनता में तलाशते हैं तो दूसरी तरफ साम्प्रदायिकता के अंधकार को भाई-भाई के बीच हो रहे अज्ञानतापूर्ण अनुचित संघर्ङ्ढ के रूप में देखते है। ये दोनाें विचार दार्शनिक संस्तर पर नाभिनाल बध्द हैं।
राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से प्रादुर्भूत साम्प्रदायिक वैमनस्य के दौर मे इस दृष्0श्निV की ओर पुनर्वापसी स्वाभाविक थी। अनिल सिंह अपनी बहुचर्चित कविता 'अयोध्या' में उसे इस प्रकार रखते हैं।
'' मनुष्; रहते हैं इस शहर में
जिनमें रहता है भगवान
और चूंकी भगवान मनुष्; में रहता है
इसलिए वह अल्लाह भी हो सकता है''
फिर मनुष्; और उसका सामान्य नागरिक जीवन ईश्वर से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि-
''इतना ही यथार्थ है यह शहर जितना यह कि
आदमी का कलेजा काटकर उसकी जगह
शिवलिंग रख देने से वह मर जायेगा''
ईश्वर और मनुष्य की सत्ताा का एकाकार होना मानववादी कविता की एक प्रमुख विशेङ्ढता है। यह भी कहा जा सकता है कि इस कविता में मनुष्य ही ईश्वर हो जाता है। आगे चलें तो यह तथ्य सामने आता है कि मनुष्य के तिरस्कार पर ईश्वर और उसकी भक्ति ही निरर्थक हो जाती है। ऐसे में उसके प्रति भक्ति या श्रध्दा का कोई महत्व नहीं। बाह्याडम्बरों पर हुए आक्रमण इसी के चलते हैें। देखें तो ईश्वर और धर्म के प्रति यही सोच भारत मेें धर्मनिरपेक्षता का मूल बनती है और जिसके कुछ तत्व भक्ति युग में प्राप्त होते हैं। मनुष्य के कारण ही तो ईश्यर का अस्तित्व है वगर्ना धर्म का सारा ताना-बाना बेकार है। आध्यात्म के अखण्ड भाव में पूरे विश्व का समा जाना जरूरी है और मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे।
इस मानववाद की अभिव्यक्ति हमारे समय की साम्प्रदायिकता विरोधी हिन्दी कविता में तरह-तरह से हुई। नवल शुक्ल स्वयं को ईश्वर से अधिक पाते है क्योंकि ईश्वर युगों में पृथ्वी की सुधि लेते हैं जबकि कवि (मनुष्य) ''किसी भी जगह जनम लेकर'' पूरे ब्रह्माण्ड के बारे में सोचता है और ''अपनी क्षमता से अधिक रहने की कोशिश करता'' है। साम्प्रदायिकता के इस विकट दौर से पहले आने वाले कवि सर्वेश्वर के लिए-
'' इस दुनिया में
आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है
न ईश्वर
न ज्ञान
न चुनाव
न संविधान
इसके नाम पर कागज पर लिखी कोई भी इबारत
फाड़ी जा सकती है
और जमीन के भीतर गाड़ी जा सकती है''
केदारनाथ सिंह की कविताओं में ईश्वर का जिक्र एक मुहावरे के रूप में आता है। ऐसा सिर्फ केदारनाथ सिंह की कविता में नहीं अपितु बहुत से अन्य कवियों की भी कविताओं में है। वहां यह 'ईश्वर' एक भाव बोधक शब्द भी है, जो कविता से बाहर जीवन में घनघोर प्रचलन रखता है। इस अर्थ में यह शब्द 'ईश्वर' के दार्शनिक अथवा धार्मिक अर्थ सन्दर्भों से बिल्कुल अलग अस्तित्वमान है। 'हे राम' या 'राम नाम सत्य है' या 'खुदा कसम' जैसे वाक्यांशाें की तरह यह भाङ्ढा में विद्यमान है। यह एक जटिल प्रश्न है कि यह सत्ताा भाङ्ढा के इस प्रकार के स्वतंत्र लगने वाले प्रयोगों मेें किस प्रकार लगातार क्रियाशील करती है? इस लगातार बरकरार भाङ्ढायी तत्व में क्या कहीं दार्शनिक प्रत्ययों को भी वैधता तो नहीं प्राप्त होती? कैन्टरबरी के एनसेल्म ने ईश्वर के अस्तित्वमान होने का प्रमाण देते हुए कहा था कि 'ईश्वर' शब्द का होना ही उसके अस्तित्वमान होने का सबूत है। यह सत्ताा शब्दों के माध्यम से बनी रहती है। मेरे एक उर्दू पढ़ाने वाले मित्र ने बताया था कि किस प्रकार प्रारंभिक कक्षाओं में भाङ्ढा ज्ञान कराते समय ही बच्चों को शब्दों के माध्यम से ईश्वर और धर्म की घुट्टी पिला दी जाती है। लेकिन ईश्वर को गंभीरतापूर्वक न लेने वालों के बीच भी ईश्वर शब्द बना रहता है और प्रयोग से बाहर नहीं होता। यही वजह है कि ईश्वर संबन्धी कविताओं के गहरे अर्थों तक पहुंचने की जरूरत महसूस होती है।
मुहावरे की ही तरह ही ईश्वर के प्रति प्रार्थना के शिल्प में लिखी गयीं कविताएं किस प्रकार प्रार्थना की सीमा से बाहर निकलती है उसका उदाहरण है निराला की वे अन्तिम कविताएं जो सिर्फ प्रार्थनाएं न होकर स्वातंत्रोत्तर भारत की बदलती परिस्थितियाें में एक संवेदनशील कवि के मोहभंग की विशिष्ट कोटि की अभिव्यक्ति है। इस विङ्ढय पर कवि एवं आलोचक केदारनाथ सिंह ने एक बहुत प्रभावशाली लेख लिखा है। निराला अपनी इन कविताओं में ईश्वर के संदर्भ को अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर सूक्ष्म राजनीतिक अर्थ प्रदान करते हैैं।
'जय तुम्हारी देख भी ली
रूप की गुण की, सुरीली।
वृध्द हूँ मैं, ऋध्दि की क्या,
साधना की, सिध्दि की क्या?
खिल चुका है फूल मेरा,
पखड़ियाँ हो गयीं ढीली।
चढ़ी थी जो ऑंख मेरी,
बज रही थी जहाँ भेरी,
वहाँ सिकुड़न पड़ चुकी है,
बढ़ रही है रेख नीली।
आग सारी फुक चुकी है,
रागिनी वह रुक चुकी है,
याद करता हुआ जीवन,
जीर्ण जर्जर आज तीली।'
यही प्रार्थना का सबवर्जिव काव्य प्रारूप किस प्रकार ईश्वर के प्रति नकारात्मक रुख अख्तियार करता है यह यदि देखना हो तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 'ईश्वर' पर लिखित कविता देखने योग्य होगी। 'गर्म हवाएं' संग्रह में आयी यह कविता ऐसी अन्य कविताओं से घिरी है जो कवि के अपने व्यक्तिगत दु:खों, सामाजिक मोहभंग और व्यथित चुनावों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। संग्रह 'धीरे-धीरे' जैसी राजनीतिक कविता से प्रारंभ होता है जिसमें सर्वेश्वर एक 'क्रांतियात्रा' को 'शवयात्रा' में बदलते हुए देखते हैं। पत्नी की मृत्यु पर लिखी गयी एक अत्यन्त ही भावपूर्ण कविता के बाद आती है प्रार्थना कविताओं की ऋृंखला जिनमें कवि ईश्वर से शक्ति नहीं मांगता (प्रार्थना-1) 'दुर्गम पथ' मांगता है जिस पर उसके 'थके चरण' हों (प्रार्थना-2), अपनी सीमाओं का ध्यान और दुर्बलताओं का अभियान मांगता है (प्रार्थना-3)। पर अपनी कविता 'प्रार्थना-4' में वह ईश्वर का लगभग निङ्ढेध करता है।
'यही प्रार्थना है प्रभु तुमसे
जब हारा हूं तब न आइये।'
कवि अपने शौर्य की तो सराहना चाहता है, मगर वह ईश्वर के चरणों में नहीं गिरना चाहता। वह जानता है कि संसार में दु:ख की ऑंखें बहुत बड़ी है और उसके एक अश्रु की आयु के सामने कल्पचक्र अस्वीकार्य है। और इन प्रार्थनाओं के बाद आती है कविता 'ईश्वर'। सर्वेश्वर की यह कविता निश्चित रूप से दु:ख से भीगी हुई है। व्यक्तिगत दु:ख और मोहभंग से घिरी हुई यह कविता ईश्वर को एक ठोस रूप में प्रस्तुत करती है जो एक व्यापारी या बॉस की तरह 'बहुत लम्बी जेबों वाला कोट' पहनकर आता है और कवि की माँ, पिता, पत्नी और बच्चे को खिलौनों की तरह जेब में रखकर चला जाता है। कवि के लिए दुनियाँ छोड़ जाता है, जिसमें उसे बहलाने के लिए और बहुत से खिलौने हैं। आगे कवि लिखता है,
'मैंने सुना है
उसने कहीं खोल रखी है
खिलौनो की दूकान,
अभागे के पास
कितनी जरा सी पूँजी है
रोजगार चलाने के लिए।'
एक खिलौने के व्यापारी के रूप में ईश्वर का अवमूल्यन उसे हास्यास्पद बना देता है। ईश्वर की इतनी ठोस उपस्थिति सिर्फ उसके लम्बे कोट की वजह से बन पड़ी है, जो प्रभु की इमेज को इस कविता में सुनिश्चित करता है। यह सर्वेश्वर की प्रार्थना श्रृंखला की कविताओं में उपस्थित पारंपरिक प्रार्थनाभाव की बची-खुची संभावनाओं को भी ध्वस्त कर देता है और उनमें निहित दूसरे प्रतिरोधी भावों को आलोकित करता है। यह प्रश्न भी उठता है कि वह जो कुछ भी है- ईश्वर है भी या कोई और। सर्वेश्वर की ये कविताएं उस अस्पष्ट भूमि पर खड़ी है, जहाँ ईश्वर सत्ता का प्रतीक बनता दिखाई देता है। ईश्वर की सत्ता के प्रति प्रार्थना के ही शिल्प में व्यंगाात्मक सूक्ष्म कटाक्ष भरे प्रयोग किस प्रकार प्रभावपूर्ण हो सकते हैं इसका एक उदाहरण है शमशेर बहादुर सिेह की द्वारा भजन के शिल्प में प्रस्तुत यह कविता:
हरि मोरी आड़, हरि ही मोरी आड़॥
हरि मोरी झाँकी, हरि ही केंवाड़॥
हरि जमुना-मंथन मोरे, हरि ही
थाम्हे दुख के पहाड़॥
हरि संग ज्ञान-ध्यान मोहे मधुऋतु
हरि बिन सकल उजाड़॥
मज्जा-भेद बसे हरि अंतर
हरि संबल मोरे हाड़॥
जग बाड़व में जनम-जनम लौं
झोंक्यों कितने भाड़॥
तब आयो समसेरु मुकति को
परलौ मास असाढ़॥
हरि मोरी आड़, हरि ही मोरी आड़॥
सांप्रदायिक उन्माद के भीषण दौर से पूर्वं, अर्थात 1990 से पहले के समय की समकालीन हिन्दी कविता में ईश्वर की उपस्थिति की तुलना मेें बाद की कविताओं में उसकी उपस्थिति काबिले गौर है। स्वप्निल श्रीवास्तव की कविताओं मे ईश्वर की उपस्थिति एक वैचाारिक द्वंद्व का परिणाम है। 'ईश्वर एक लाठी है' कविता इस अर्थ में ध्यातव्य है। यहां कवि अपने पिता जैसे बूढे लोगाें के लिए ईश्वर के निहितार्थ को समझने की कोशिश करता है। इस कविता में यदि पिता के ईश्वर में विश्वास के प्रति सहानुभूति है तो उस विश्वास की व्यर्थता का भी एहसास है। ईश्वर पिता के लिए एक ऐसी लाठी है जिसे वे अक्सर तान देते है। उन्होंने इस लाठी को जिन्दगी भर मजबूत रखने की कोशिश की है, मगर उन्हें लाठी में घुन के चालने की आवाज सुनायी देती है। अपनी जीवन भर की आस्था के बाद भी वे यह नहीं जान सके हैं कि ईश्वर आखिर किस कोठ की लाठी है। स्वप्निल श्रीवास्तव की इस कविता के तमाम निहितार्थ निकलते हैं, विशेषरूप से इस कारण कि कवि के काव्यानुशासन में कविता के अर्थ एक दिशा में चलते हुए भी विभिन्न संस्तरों पर खुलते है। एक आस्तिक पिता के द्वंद को यह बखूबी रेखांकित करने वाली कविता है जिसके लिए ईश्वर एक ऐसा सहारा है जो कमजोर होता जा रहा है, मगर जिसे त्याग पाना उसके तर्क स्वभाव में कहीं दूर-दूर तक नहीं।
ईश्वर, सत्ता और कविता (1)
ईश्वर, सत्ता और कविता
(1)
आपातकाल के पश्चात्, प्र्रकाशित हुए अपने कविता संग्रह 'हजार हजार बाहों वाली' में जनकवि नागार्जुन की एक कविता थी 'कल्पना के पुत्र हे भगवान'। अपने शीर्ङ्ढक को सार्थक करती हुई यह कविता ईश्वर के अस्तित्व पर लिखी गयी उस कालखंड की एक महत्वपूर्ण कविता थी। कल्पनाजनित ईश्वर को संबोधित करती यह कविता कुछ इस प्रकार प्रारम्भ होती है-
''कल्पना के पुत्र हे भगवान
चाहिए मुझको नहीं वरदान
दे सको तो दो मुझे अभिशाप
प्रिय मुझे है जलन प्रिय संताप
चाहिए मुझको नहीं यह शान्ति
चाहिए संदेह उलझन भ्रांति''
आस्था के स्थान पर संदेह की माँग करती यह कविता बेहद चुनौतीपूर्ण है। संग्रह में दिये गये विवरण के अनुसार इस कविता का रचना समय 1946 है। उस समय के पारंपरिक समाज को देखते हुए यह तथ्य इस कविता के ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ा देता है। पारंपरिक तौर पर ईश्वर से होने वाली आस्था की माँग के बरक्स अनास्था की मॉग करने वाली यह कविता एक प्रकार का वैचारिक साहस थी। बरबस ध्यान खींच लेने वाली बाबा की यह कविता या तो आश्चर्य मिश्रित उत्साह के साथ पढ़ी गयी या फिर भयाक्रांत निन्दाभाव से। वह दौर हमारे आज के अभी-अभी गुजरे फासीवादी दौर के दु:स्वप्न से बिल्कुल अलग था, वगर्ना संघी भाई लाठी लेकर नागार्जुन को खोजते और बाबा अपनी खास मुद्रा में कोई अटपटा सा उत्तर देते। फासीवादियों को केवल गर्मी और उत्तेजना से मतलब होता है, जिसे वे विचार के लोहे में ढालकर हथियार के तौर पर जनता में ट्रांसफर कर अपना उल्लू सीधा करते है। उन्हें कविता अथवा किसी भी कला के अर्थ, भाव या अभिव्यक्ति की सूक्ष्मताओं से कुछ खास लेना देना नहीं होता। यदि ऐसा न होता तो वे बर्बर दंगाइयों में क्यों तब्दील होते और पिछले तीस वङ्र्ढों का भारतीय इतिहास आदमीयत के खून से सराबोर न होता।
इस कविता के सिलसिले में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे कविता के पेशेवर पाठकों तक ने उस सूक्ष्मता में नहीं देखा जिस सूक्ष्मता मेें यह कविता अपने पाठ की अपेक्षा रखती है। इसे नागार्जुन की 'प्रतिबध्द हॅू' या फिर 'प्रतिहिंसा स्थायीभाव है' वाली सीधी कविताओं की ही तरह देखा गया। नागार्जुन की यह कविता अपनी अभिधा में ईश्वर को सम्बोधित है जिसको वह स्वयं कल्पना का पुत्र बतलाती है। जिसके अस्तित्व पर ही शंका है या जिसके न होने पर पूरा विश्वास है, उसे संबोधित करने का औचित्य सिध्द करना थोड़ा विचित्र लगेगा। इस कविता के निहितार्थ को कविता की बाद की पंक्तियों में तलाशने पर ही कविता के वास्तविक मंतव्य से मिला जा सकेगा और वह भी कविता के व्यंग्यार्थ में। कविता में 'निन्दा' और 'पाप' करने का जी खोल अभिशाप माँगा गया है। जो सुनिश्चित तौर पर किसी नैतिक वरदान की अभिलाङ्ढा रखने वालों के लिए अच्छा खासा धक्का साबित होगा, पर कविता का वास्तविक केन्द्र वह स्थान है जहांॅ कवि पारंपरिक तौर पर ईश्वर के सामने कान पकड़कर नाक नहीं रगड़ना चाहता।
''बाप-दादों की तरह रगडू न मैं निज नाक
मंदिर की देहली पर पकड़ दोनों कान''
यह साफ है कि यहाँ ईश्वर की सर्वशक्तिमान सत्ता से इन्कार है। नागार्जुन की यह कविता सिर्फ कल्पना सृजित ईश्वर के दार्शनिक विरोध तक ही सीमित नहीं अपितु ईश्वर की अवधारणा से जुड़ी तमाम परंपरागत और अविवेकी बातों का भी प्रतिकार थी जिन्हें आस्था, धर्म और नैतिकता के नाम पर लादा या स्वीकार किया जाता रहा है। ये सभी बातें हमारे समय के मनुष्य को उसकी वास्तविक समस्याओं से दूर ले जाती हैं,
'सड़ गमी है ऑंत
दिखाए जा रहे है दांत''
नागार्जुन समाज में धर्म और ईश्वर के नाम पर पैदा किये जाने वाले भय का प्रतिकार करते है। इस धर्मभीरुता अथवा पारंपरिक कायरता के प्रतिवाद के संदर्भ मे वे धर्म के वर्चस्व को नहीं स्वीकार करते। वे धर्म के इस प्रतिगामी पक्ष की ओर संकेत करते है, जब वे लिखते है कि 'छोड़कर प्रासाद खोजूं खोह/कह रहा है पूर्वजों का मोह'।
इस प्रतिकार भाव को ध्यान में रखें तो यह कविता हिन्दी साहित्य में अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। नागार्जुन की कविता के सामान्य पाठक को भी यह बात अवश्य आकर्ङ्ढित करती है कि वहां व्यर्थ के आध्यात्म के लिए स्पेस लगभग नहीं है। अपने सारे प्रकार-प्रकार के सर्जनात्मक मुद्रा-मुखौटों के उपरांत भी नागार्जुन की कविता विवेक सम्मतता की ही विजय का धर्मनिरपेक्ष उद्धोङ्ढ है। यहां मैं धर्मनिरपेक्षता को महज ईश्वर विरोध तक सीमित करने का कोई उपक्रम नहीं कर रहा। धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित तौर पर एक अधिक व्यापक प्रत्यय है। इतनी व्यापक कि इतिहास के प्रवाह में वह धर्म से लेकर विज्ञान तक में विकसित होती दिखायी दे। यहाँ मैं उस अवस्थिति की चर्चा कर रहा हूं, जो इधर लिखी गयी हिन्दी कविता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और जहां से एक पूरे कालखंड में लिखी गयी ढेर सारी कविताओं का निर्वचन संभव है।
अपनी दूसरी कविता 'थकित-चकित-भ्रमित-भग्नमन' में वे ईश्वर को एक सहारे के रूप में भी स्वीकार करने से इन्कार करते हैं। यद्यपि वे जानते है कि बहुतों के लिए ईश्वर जैसे 'समर्थ' का सहारा स्फूर्ति देता है। फिर वृध्दावस्था के डूबते के लिए तो तिनके का सहारा ही बहुत होता है। वृध्दावस्था में बहुत से प्रगतिशील तार्किकजन ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं, क्योकि बुढ़ापे के कमजोर तन-मन को आस्था का कोई आश्रय चाहिए होता है। इसके अतिरिक्त फिर सुविधा के भी तो अपने तर्क होते ही होते हैं जो मनुष्य को ललचाते हैं।
'सुख-सुविधा और ऐश-आराम के साधन
डाल देते हैं दरार प्रखर नास्तिकता की भीत मेें
बड़ा ही मादक होता है, 'यथास्थिति' का शहद
बड़ी ही मीठी होती है 'गतानुगतिकता' की संजीवनी'
नागार्जुन की यह कविता अपने अंतिम पड़ाव में स्वयं से और अपने जैसे तमाम तार्किकों से यह प्रश्न करती है कि क्या जीवन के अंतिम दौर में उन्हें किसी धार्मिक मठ की शरण लेनी पड़ेगी? इस प्रश्न की भाङ्ढायी नकार और व्यंग में नागार्जुन अपनी स्पष्ट अवस्थिति और दृढ़ निश्चय की ओर ही संकेत करते है।
' तो क्या मुझे भी बुढ़ापे में 'पुष्टई' के लिए
वापस नहीं जाना है किसी मठ के अन्दर '
यह एक रोचक प्रश्न हो सकता है कि क्या नागार्जुन अपनी इस कविता में निराला की अन्तिम कविताओं की ओर संकेत कर रहे हैं जिनमें निराला ईश्वर के प्रति प्रार्थनाभाव की कविताएं लिखते हैं। संभवत: यह नागार्जुन का संकेत नहीं, लेकिन हिन्दी के कई आलोचकाें ने निराला के इस अन्तिम दौर के भागवतवाद पर टिप्पणियाँ की हैं। लेकिन निराला के अन्तिम दौर की प्रार्थनापरक कविताएं इस तरह सरलीकृत नहीं हैं और उनकी जटिलता में निराला के जीवन, उनके नैराश्य, पत्नी प्रेम, मृत्यु छाया और उनका अपना समय परोक्ष पढ़ा जा सकता है। यहां प्रार्थना महज आस्था की अभिव्यक्ति नहीं एक रचना प्रविधि भी है।
नागार्जुन की इस कविता के सापेक्ष हिन्दी की उस पहली दलित कविता का जिक्र जरूरी लगता है जिसमें ईश्वर को 'भगवनवा' कहा गया है, अथवा निराला के उस लघु उपन्यास का जिक्र जिसका नायक ईश्वर पर लाठी चला देता हैं। मगर ये दोनाें ही कृतियाँ नागार्जुन की इस कविता से थोड़ा अलग हैं। हिन्दी की प्रसिध्द ऐतिहासिक महत्व की पत्रिका 'सरस्वती' में प्रकाशित और यहां संदर्भित हीरा डोम की कविता अपने वक्तव्यों में पात्र अथवा कवि की विवशता और शिकायत को व्यक्त करती है जो अपनी जीवन स्थितियों से तंग है। यहां वर्ण व्यवस्था के प्रति आक्रोश पढ़ा जा सकता है । लेकिन देखें तो वास्तव में वही मुख्य बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्याेंंकि वर्ण व्यवस्था के प्रति यह आक्रोश ही उसे उद्वेलित कर ईश्वर की ओर ले जाता है और उसकी लानत-मलामत तक उतारता है। मगर वर्ण व्यवस्था की परिधि से बाहर खड़ा यह डोम ईश्वर की सत्ता से इन्कार नहीं करता। यहां ईश्वर के प्रति निङ्ढेध नहीं अपितु एक विडम्बना पूर्ण और विवश धिक्कार है। महाप्राण निराला की उपन्यासिका में यह प्रतिकिया दूसरे प्रकार की है। मगर दोनों जगह ईश्वर के प्रत्यय को सत्ता से प्रछन्नत: जोड़ा गया है- छल-छद्म और वर्ण व्यवस्था की सत्ताा। हीरा डोम की कविता में तो ईश्वर वर्ण व्यवस्था का पोङ्ढक लगता है। यहां चूकि संदर्भ कविता का है इसलिए निराला की उपन्यासिका का जिक्र छोड़ना पडेग़ा। इस लेख में हिन्दी कविता में ईश्वर के प्रत्यय का प्रयोग निराला के बाद के कवियों ने किस प्रकार किया है और उसके क्या व्यापक निहितार्थ हैं, यही मूल चर्चा का विङ्ढय है। इस प्रश्न के मौजू होने के ऐतिहासिक कारण हैं जो हिन्दी कविता के किसी भी सतर्क पाठक से छिपे नहीं है।
हमारे समय में धर्म का सांप्रदायिक और मनुष्य विरोधी स्वरूप काफी स्पष्ट हो गया है। बीसवीं शताब्दि के आखिरी दशकों से लेकर यदि नयी शताब्दी के प्रारंभिक वङ्र्ढो तक को ध्यान मे रखें तो धर्म को लेकर हुए उत्पातों में जितने निर्दोङ्ढ लोग मारे गये उतने किसी भी प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी मानवीय त्रासदी मेें नहीं मारे गये। यह सांप्रदायिकता विभिन्न प्रकार से उभरी और हिन्दू साम्प्रदायिकता का नग्न नृत्य इसका चरमोत्कर्ङ्ढ है। पंजाब के सिख आतंकवाद, कश्मीर के मुस्लिम आतंकवाद और हिन्दू सांप्रदायिकता की आग में अपनी जान खो देने वाले निर्दोङ्ढ लोगों की संख्या का आंकड़ा रख पाना कठिन है। सिर्फ एक गुजरात के दंगों में 6000 से अधिक लोगो के मारे जाने के आंकड़े है। यह संख्या कम अथवा अधिक हो सकती है और यह बहस का मुद्दा नहीं। मुद्दा यह है कि मनुष्य को सदाचार और मानवीयता का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाला धर्म आज राजनीतिज्ञों द्वारा किस प्रकार इस्तेमाल हो रहा है और धर्म तधा ईश्वर के ठेकेदार किस प्रकार इस अमानवीय कृत्य में लिप्त हैं और किस प्रकार इसे अपना मुद्दा बनाये हुए है। धर्म की राजनीति करने वाले लोग हत्याओं तर्क तलाशने में जुटे हुए है। स्वयं को सहिष्णु बताने वाले धर्मो के इस प्रकार सामने आने वाले हिंसक रूप किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए चिन्ता का विषय होंगें।
'किसी धर्मस्थल के
विवाद में
तीन हजार लोग बम से
दो हजार गोली से
और पाँच सौ
जलाकर मार डाले जाते हैं
चार सौ महिलाओं की
इज्ज़त लूटी जाती है
और तीन सौ शिशुओं को
बलि का बकरा बनाया जाता है
धर्म में
सहिष्णुता का
प्रतिशत ज्ञात कीजिए'
-अष्टभुजा शुक्ल
इस प्रकार की परिस्थितियाें में हिन्दी कविता में ईश्वर के प्रति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखलाई देती हैं। यह ईश्वर ही वह दार्शनिक प्रत्यय है जिसके इर्द-गिर्द धर्म का तानाबाना बुना हुआ है। यही वह दार्शनिक केंन्द्र है जिसके चारो ओर फैला प्रपंच धर्म के नाम पर होने वाली तमाम अमानवीय गतिविधियों को वैधता प्रदान करता है। एक प्रकार से यह सांप्रदायिकता को भी वैधता प्रदान करने वाला आधार है जिसकी जन्मभूमि के विवाद को राजनीतिक सीढ़ी बनाकर भाजपा के लिए केंद्र की सत्ता पर आसीन होना संभव हुआ। यह महज एक इत्तिाफाक नहीं कि ऐसे समय में ऋतुराज अपना संग्रह 'लीला मुखारविंद' उन नास्तिकों को समर्पित करते हैं जो ईश्वर अथवा धर्म में विश्वास नहीं करते मगर जो मनुष्यता के सुखद और बेहतर भविष्य के लिए संघष्र् ारत हैं, 'जो बिना निराश हुए अपने विवेक की दृढ़ता मेंं साहसपूर्वक संघष्र् ारत है। मानव जाति का सुखमय भविष्य ही जिनका परलोक है।' वैसे भी देखे तो इधर धर्म ओर नस्ल के नाम पर पूरी दुनिया में इतने दंगे और खून खराबे हुए हैं कि नीत्शे का यह वाक्य प्रासंगिक लगता है, ' ईश्वर मर चुका है और मैंने उसे दफन होते हुए देखा है.' ऋतुराज की तरह हर संवेदनशील और विवेकवान व्यक्ति इस साम्प्रदायिक उन्माद और उसके फासीवादी विस्तार के दौर में ईश्वर प्रत्यय और उससे जुड़े धर्म के हत्यारे प्रयोगों को प्रश्न के घेरे मेें रख सकता है। यदि इस दौर का सांप्रदायिक अमानवीय धर्म ही बचा है, तो इस धर्म के रास्ते पर न चलना ही वास्तविक धर्म होगा।
(1)
आपातकाल के पश्चात्, प्र्रकाशित हुए अपने कविता संग्रह 'हजार हजार बाहों वाली' में जनकवि नागार्जुन की एक कविता थी 'कल्पना के पुत्र हे भगवान'। अपने शीर्ङ्ढक को सार्थक करती हुई यह कविता ईश्वर के अस्तित्व पर लिखी गयी उस कालखंड की एक महत्वपूर्ण कविता थी। कल्पनाजनित ईश्वर को संबोधित करती यह कविता कुछ इस प्रकार प्रारम्भ होती है-
''कल्पना के पुत्र हे भगवान
चाहिए मुझको नहीं वरदान
दे सको तो दो मुझे अभिशाप
प्रिय मुझे है जलन प्रिय संताप
चाहिए मुझको नहीं यह शान्ति
चाहिए संदेह उलझन भ्रांति''
आस्था के स्थान पर संदेह की माँग करती यह कविता बेहद चुनौतीपूर्ण है। संग्रह में दिये गये विवरण के अनुसार इस कविता का रचना समय 1946 है। उस समय के पारंपरिक समाज को देखते हुए यह तथ्य इस कविता के ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ा देता है। पारंपरिक तौर पर ईश्वर से होने वाली आस्था की माँग के बरक्स अनास्था की मॉग करने वाली यह कविता एक प्रकार का वैचारिक साहस थी। बरबस ध्यान खींच लेने वाली बाबा की यह कविता या तो आश्चर्य मिश्रित उत्साह के साथ पढ़ी गयी या फिर भयाक्रांत निन्दाभाव से। वह दौर हमारे आज के अभी-अभी गुजरे फासीवादी दौर के दु:स्वप्न से बिल्कुल अलग था, वगर्ना संघी भाई लाठी लेकर नागार्जुन को खोजते और बाबा अपनी खास मुद्रा में कोई अटपटा सा उत्तर देते। फासीवादियों को केवल गर्मी और उत्तेजना से मतलब होता है, जिसे वे विचार के लोहे में ढालकर हथियार के तौर पर जनता में ट्रांसफर कर अपना उल्लू सीधा करते है। उन्हें कविता अथवा किसी भी कला के अर्थ, भाव या अभिव्यक्ति की सूक्ष्मताओं से कुछ खास लेना देना नहीं होता। यदि ऐसा न होता तो वे बर्बर दंगाइयों में क्यों तब्दील होते और पिछले तीस वङ्र्ढों का भारतीय इतिहास आदमीयत के खून से सराबोर न होता।
इस कविता के सिलसिले में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे कविता के पेशेवर पाठकों तक ने उस सूक्ष्मता में नहीं देखा जिस सूक्ष्मता मेें यह कविता अपने पाठ की अपेक्षा रखती है। इसे नागार्जुन की 'प्रतिबध्द हॅू' या फिर 'प्रतिहिंसा स्थायीभाव है' वाली सीधी कविताओं की ही तरह देखा गया। नागार्जुन की यह कविता अपनी अभिधा में ईश्वर को सम्बोधित है जिसको वह स्वयं कल्पना का पुत्र बतलाती है। जिसके अस्तित्व पर ही शंका है या जिसके न होने पर पूरा विश्वास है, उसे संबोधित करने का औचित्य सिध्द करना थोड़ा विचित्र लगेगा। इस कविता के निहितार्थ को कविता की बाद की पंक्तियों में तलाशने पर ही कविता के वास्तविक मंतव्य से मिला जा सकेगा और वह भी कविता के व्यंग्यार्थ में। कविता में 'निन्दा' और 'पाप' करने का जी खोल अभिशाप माँगा गया है। जो सुनिश्चित तौर पर किसी नैतिक वरदान की अभिलाङ्ढा रखने वालों के लिए अच्छा खासा धक्का साबित होगा, पर कविता का वास्तविक केन्द्र वह स्थान है जहांॅ कवि पारंपरिक तौर पर ईश्वर के सामने कान पकड़कर नाक नहीं रगड़ना चाहता।
''बाप-दादों की तरह रगडू न मैं निज नाक
मंदिर की देहली पर पकड़ दोनों कान''
यह साफ है कि यहाँ ईश्वर की सर्वशक्तिमान सत्ता से इन्कार है। नागार्जुन की यह कविता सिर्फ कल्पना सृजित ईश्वर के दार्शनिक विरोध तक ही सीमित नहीं अपितु ईश्वर की अवधारणा से जुड़ी तमाम परंपरागत और अविवेकी बातों का भी प्रतिकार थी जिन्हें आस्था, धर्म और नैतिकता के नाम पर लादा या स्वीकार किया जाता रहा है। ये सभी बातें हमारे समय के मनुष्य को उसकी वास्तविक समस्याओं से दूर ले जाती हैं,
'सड़ गमी है ऑंत
दिखाए जा रहे है दांत''
नागार्जुन समाज में धर्म और ईश्वर के नाम पर पैदा किये जाने वाले भय का प्रतिकार करते है। इस धर्मभीरुता अथवा पारंपरिक कायरता के प्रतिवाद के संदर्भ मे वे धर्म के वर्चस्व को नहीं स्वीकार करते। वे धर्म के इस प्रतिगामी पक्ष की ओर संकेत करते है, जब वे लिखते है कि 'छोड़कर प्रासाद खोजूं खोह/कह रहा है पूर्वजों का मोह'।
इस प्रतिकार भाव को ध्यान में रखें तो यह कविता हिन्दी साहित्य में अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। नागार्जुन की कविता के सामान्य पाठक को भी यह बात अवश्य आकर्ङ्ढित करती है कि वहां व्यर्थ के आध्यात्म के लिए स्पेस लगभग नहीं है। अपने सारे प्रकार-प्रकार के सर्जनात्मक मुद्रा-मुखौटों के उपरांत भी नागार्जुन की कविता विवेक सम्मतता की ही विजय का धर्मनिरपेक्ष उद्धोङ्ढ है। यहां मैं धर्मनिरपेक्षता को महज ईश्वर विरोध तक सीमित करने का कोई उपक्रम नहीं कर रहा। धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित तौर पर एक अधिक व्यापक प्रत्यय है। इतनी व्यापक कि इतिहास के प्रवाह में वह धर्म से लेकर विज्ञान तक में विकसित होती दिखायी दे। यहाँ मैं उस अवस्थिति की चर्चा कर रहा हूं, जो इधर लिखी गयी हिन्दी कविता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और जहां से एक पूरे कालखंड में लिखी गयी ढेर सारी कविताओं का निर्वचन संभव है।
अपनी दूसरी कविता 'थकित-चकित-भ्रमित-भग्नमन' में वे ईश्वर को एक सहारे के रूप में भी स्वीकार करने से इन्कार करते हैं। यद्यपि वे जानते है कि बहुतों के लिए ईश्वर जैसे 'समर्थ' का सहारा स्फूर्ति देता है। फिर वृध्दावस्था के डूबते के लिए तो तिनके का सहारा ही बहुत होता है। वृध्दावस्था में बहुत से प्रगतिशील तार्किकजन ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं, क्योकि बुढ़ापे के कमजोर तन-मन को आस्था का कोई आश्रय चाहिए होता है। इसके अतिरिक्त फिर सुविधा के भी तो अपने तर्क होते ही होते हैं जो मनुष्य को ललचाते हैं।
'सुख-सुविधा और ऐश-आराम के साधन
डाल देते हैं दरार प्रखर नास्तिकता की भीत मेें
बड़ा ही मादक होता है, 'यथास्थिति' का शहद
बड़ी ही मीठी होती है 'गतानुगतिकता' की संजीवनी'
नागार्जुन की यह कविता अपने अंतिम पड़ाव में स्वयं से और अपने जैसे तमाम तार्किकों से यह प्रश्न करती है कि क्या जीवन के अंतिम दौर में उन्हें किसी धार्मिक मठ की शरण लेनी पड़ेगी? इस प्रश्न की भाङ्ढायी नकार और व्यंग में नागार्जुन अपनी स्पष्ट अवस्थिति और दृढ़ निश्चय की ओर ही संकेत करते है।
' तो क्या मुझे भी बुढ़ापे में 'पुष्टई' के लिए
वापस नहीं जाना है किसी मठ के अन्दर '
यह एक रोचक प्रश्न हो सकता है कि क्या नागार्जुन अपनी इस कविता में निराला की अन्तिम कविताओं की ओर संकेत कर रहे हैं जिनमें निराला ईश्वर के प्रति प्रार्थनाभाव की कविताएं लिखते हैं। संभवत: यह नागार्जुन का संकेत नहीं, लेकिन हिन्दी के कई आलोचकाें ने निराला के इस अन्तिम दौर के भागवतवाद पर टिप्पणियाँ की हैं। लेकिन निराला के अन्तिम दौर की प्रार्थनापरक कविताएं इस तरह सरलीकृत नहीं हैं और उनकी जटिलता में निराला के जीवन, उनके नैराश्य, पत्नी प्रेम, मृत्यु छाया और उनका अपना समय परोक्ष पढ़ा जा सकता है। यहां प्रार्थना महज आस्था की अभिव्यक्ति नहीं एक रचना प्रविधि भी है।
नागार्जुन की इस कविता के सापेक्ष हिन्दी की उस पहली दलित कविता का जिक्र जरूरी लगता है जिसमें ईश्वर को 'भगवनवा' कहा गया है, अथवा निराला के उस लघु उपन्यास का जिक्र जिसका नायक ईश्वर पर लाठी चला देता हैं। मगर ये दोनाें ही कृतियाँ नागार्जुन की इस कविता से थोड़ा अलग हैं। हिन्दी की प्रसिध्द ऐतिहासिक महत्व की पत्रिका 'सरस्वती' में प्रकाशित और यहां संदर्भित हीरा डोम की कविता अपने वक्तव्यों में पात्र अथवा कवि की विवशता और शिकायत को व्यक्त करती है जो अपनी जीवन स्थितियों से तंग है। यहां वर्ण व्यवस्था के प्रति आक्रोश पढ़ा जा सकता है । लेकिन देखें तो वास्तव में वही मुख्य बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्याेंंकि वर्ण व्यवस्था के प्रति यह आक्रोश ही उसे उद्वेलित कर ईश्वर की ओर ले जाता है और उसकी लानत-मलामत तक उतारता है। मगर वर्ण व्यवस्था की परिधि से बाहर खड़ा यह डोम ईश्वर की सत्ता से इन्कार नहीं करता। यहां ईश्वर के प्रति निङ्ढेध नहीं अपितु एक विडम्बना पूर्ण और विवश धिक्कार है। महाप्राण निराला की उपन्यासिका में यह प्रतिकिया दूसरे प्रकार की है। मगर दोनों जगह ईश्वर के प्रत्यय को सत्ता से प्रछन्नत: जोड़ा गया है- छल-छद्म और वर्ण व्यवस्था की सत्ताा। हीरा डोम की कविता में तो ईश्वर वर्ण व्यवस्था का पोङ्ढक लगता है। यहां चूकि संदर्भ कविता का है इसलिए निराला की उपन्यासिका का जिक्र छोड़ना पडेग़ा। इस लेख में हिन्दी कविता में ईश्वर के प्रत्यय का प्रयोग निराला के बाद के कवियों ने किस प्रकार किया है और उसके क्या व्यापक निहितार्थ हैं, यही मूल चर्चा का विङ्ढय है। इस प्रश्न के मौजू होने के ऐतिहासिक कारण हैं जो हिन्दी कविता के किसी भी सतर्क पाठक से छिपे नहीं है।
हमारे समय में धर्म का सांप्रदायिक और मनुष्य विरोधी स्वरूप काफी स्पष्ट हो गया है। बीसवीं शताब्दि के आखिरी दशकों से लेकर यदि नयी शताब्दी के प्रारंभिक वङ्र्ढो तक को ध्यान मे रखें तो धर्म को लेकर हुए उत्पातों में जितने निर्दोङ्ढ लोग मारे गये उतने किसी भी प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी मानवीय त्रासदी मेें नहीं मारे गये। यह सांप्रदायिकता विभिन्न प्रकार से उभरी और हिन्दू साम्प्रदायिकता का नग्न नृत्य इसका चरमोत्कर्ङ्ढ है। पंजाब के सिख आतंकवाद, कश्मीर के मुस्लिम आतंकवाद और हिन्दू सांप्रदायिकता की आग में अपनी जान खो देने वाले निर्दोङ्ढ लोगों की संख्या का आंकड़ा रख पाना कठिन है। सिर्फ एक गुजरात के दंगों में 6000 से अधिक लोगो के मारे जाने के आंकड़े है। यह संख्या कम अथवा अधिक हो सकती है और यह बहस का मुद्दा नहीं। मुद्दा यह है कि मनुष्य को सदाचार और मानवीयता का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाला धर्म आज राजनीतिज्ञों द्वारा किस प्रकार इस्तेमाल हो रहा है और धर्म तधा ईश्वर के ठेकेदार किस प्रकार इस अमानवीय कृत्य में लिप्त हैं और किस प्रकार इसे अपना मुद्दा बनाये हुए है। धर्म की राजनीति करने वाले लोग हत्याओं तर्क तलाशने में जुटे हुए है। स्वयं को सहिष्णु बताने वाले धर्मो के इस प्रकार सामने आने वाले हिंसक रूप किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए चिन्ता का विषय होंगें।
'किसी धर्मस्थल के
विवाद में
तीन हजार लोग बम से
दो हजार गोली से
और पाँच सौ
जलाकर मार डाले जाते हैं
चार सौ महिलाओं की
इज्ज़त लूटी जाती है
और तीन सौ शिशुओं को
बलि का बकरा बनाया जाता है
धर्म में
सहिष्णुता का
प्रतिशत ज्ञात कीजिए'
-अष्टभुजा शुक्ल
इस प्रकार की परिस्थितियाें में हिन्दी कविता में ईश्वर के प्रति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखलाई देती हैं। यह ईश्वर ही वह दार्शनिक प्रत्यय है जिसके इर्द-गिर्द धर्म का तानाबाना बुना हुआ है। यही वह दार्शनिक केंन्द्र है जिसके चारो ओर फैला प्रपंच धर्म के नाम पर होने वाली तमाम अमानवीय गतिविधियों को वैधता प्रदान करता है। एक प्रकार से यह सांप्रदायिकता को भी वैधता प्रदान करने वाला आधार है जिसकी जन्मभूमि के विवाद को राजनीतिक सीढ़ी बनाकर भाजपा के लिए केंद्र की सत्ता पर आसीन होना संभव हुआ। यह महज एक इत्तिाफाक नहीं कि ऐसे समय में ऋतुराज अपना संग्रह 'लीला मुखारविंद' उन नास्तिकों को समर्पित करते हैं जो ईश्वर अथवा धर्म में विश्वास नहीं करते मगर जो मनुष्यता के सुखद और बेहतर भविष्य के लिए संघष्र् ारत हैं, 'जो बिना निराश हुए अपने विवेक की दृढ़ता मेंं साहसपूर्वक संघष्र् ारत है। मानव जाति का सुखमय भविष्य ही जिनका परलोक है।' वैसे भी देखे तो इधर धर्म ओर नस्ल के नाम पर पूरी दुनिया में इतने दंगे और खून खराबे हुए हैं कि नीत्शे का यह वाक्य प्रासंगिक लगता है, ' ईश्वर मर चुका है और मैंने उसे दफन होते हुए देखा है.' ऋतुराज की तरह हर संवेदनशील और विवेकवान व्यक्ति इस साम्प्रदायिक उन्माद और उसके फासीवादी विस्तार के दौर में ईश्वर प्रत्यय और उससे जुड़े धर्म के हत्यारे प्रयोगों को प्रश्न के घेरे मेें रख सकता है। यदि इस दौर का सांप्रदायिक अमानवीय धर्म ही बचा है, तो इस धर्म के रास्ते पर न चलना ही वास्तविक धर्म होगा।
Sunday, July 20, 2008
कविता
हम मॉंझी हुए फटी नाव के
प्रेमशंकर मिश्र
धूप के हुए न हुए छझांव के
हम मॉंझी हुए फटी नाव के।
चलना फिरना हंसना बोलना
किस्त किस्त क़रजो की वापसी
इनकी उनकी पीली नीली बातें
ऑंच चढ़े उड़ जाती भाप सी
ऐसे में कैसे कोई पंक्षी पर साधे
छिन पछुवा, छिन पछियांव के।
हम मॉंझी हुए फटी नाव के।
खेतों से कटना, बोझा बनना
दाने दाने की मजबूरी
रेह देह लहरों का आमंत्रण
बान बिंधी घायल कस्तूरी
बूंद बूंद रिस चुके बनमोहन
गंध के हुए न हुए भाव के।
हम मॉंझी हुए फटी नाव के।
गलती फसलें, चटके ताल हैं
अंधा सूखा, बहरी बाढ़
लूले को काम कुऑं खोदना
लंगड़े को लांधना पहाड़
धुएं धुएं धोखे के घनपॉंखी
शहर के हुए न हुए गॉंव के।
हम मॉंझी हुए फटी नाव के।
आओ रुकें क्षण दम लें
इतना ज्यादा है थोड़ा कम लें
पिंजरे की मैना से कुछ सीखें
खुशियॉं बॉंटें सारा गम लें
सििद्धहीन मंत्रों से क्या हासिल
अर्थ के हुए न हुए भाव के।
हम मॉंझी हुए फटी नाव के।
हम मॉंझी हुए फटी नाव के
प्रेमशंकर मिश्र
धूप के हुए न हुए छझांव के
हम मॉंझी हुए फटी नाव के।
चलना फिरना हंसना बोलना
किस्त किस्त क़रजो की वापसी
इनकी उनकी पीली नीली बातें
ऑंच चढ़े उड़ जाती भाप सी
ऐसे में कैसे कोई पंक्षी पर साधे
छिन पछुवा, छिन पछियांव के।
हम मॉंझी हुए फटी नाव के।
खेतों से कटना, बोझा बनना
दाने दाने की मजबूरी
रेह देह लहरों का आमंत्रण
बान बिंधी घायल कस्तूरी
बूंद बूंद रिस चुके बनमोहन
गंध के हुए न हुए भाव के।
हम मॉंझी हुए फटी नाव के।
गलती फसलें, चटके ताल हैं
अंधा सूखा, बहरी बाढ़
लूले को काम कुऑं खोदना
लंगड़े को लांधना पहाड़
धुएं धुएं धोखे के घनपॉंखी
शहर के हुए न हुए गॉंव के।
हम मॉंझी हुए फटी नाव के।
आओ रुकें क्षण दम लें
इतना ज्यादा है थोड़ा कम लें
पिंजरे की मैना से कुछ सीखें
खुशियॉं बॉंटें सारा गम लें
सििद्धहीन मंत्रों से क्या हासिल
अर्थ के हुए न हुए भाव के।
हम मॉंझी हुए फटी नाव के।
पं. प्रेमशंकर मिश्र का अवसान
पं. प्रेमशंकर मिश्र का अवसान
डॉ. रमाशंकर तिवारी त्रिभुवन ट्रस्ट
10, गंधमादन, लक्ष्मणपुरी फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश
शोक प्रस्ताव
कल 16.07.2008 की रात हिन्दी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि और संस्कृतिकमी पं. प्रेमशंकर मिश्र जी का 83 वषZ की अवस्था में फैज़ाबाद के जिला चिकित्सालय में एक सप्ताह की बीमारी के बाद निधन हो गया। पं. प्रेमशंकर मिश्र को कविता अपने पिता द्विजेष जी से परम्परा में प्राप्त हुई थी। प्रारिम्भक दौर की पारम्परिक कविताओं के बाद वे नयी कविता और नवगीत आन्दोलनों से जुड़े और पर्याप्त ख्याति अर्जित की। प्रसिद्ध नवगीतकार शंभुनाथ सिंह ने मिश्र जी की कविताओं को अपने नवगीत संकलन नवगीत अर्धशती में स्थान देकर आपके महत्व को दषZया था। जीवन के अन्तिम दिनों तक वे कविता और संस्कृति के प्रति समर्पित रहे। सामान्य जीवन के सुखों और दुखों को अभिव्यक्ति देने वाली प्रेमशंकर मिश्र जी की कविता में साहित्य की कई परम्पराएं एक साथ चलती दिखायी देती हैं। पं. मिश्र जी के निधन से कविता की इन धाराओं की गंभीर क्षति हुई है।
संस्कृतिक परिवेश के निर्माण के उद्देश के प्रति समर्पित पं. प्रेमशंकर मिश्र जी की संस्था सम्पर्क ने फैजाबाद में साहित्य और संस्कृति से जुड़ी कई पीढ़ियों के लिए आगे बढ़ने का आधार निर्मित किया। अपनी संवादधमी प्रकृति के चलते वे विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े लोगों से विचार-विमष करते रहे। मनोविनोद की उनकी जीवन्त प्रवृत्ति ने साहित्यजगत में ही नहीं वरन् सामान्य जीवन में भी उन्हें लोकप्रिय बनाया। फैज़ाबाद के साहित्य और संस्कृति जगत में उनका अविस्मरणीय योगदान सदा याद किया जायेगा।
वे डॉ. रमाशंकर तिवारी त्रिभुवन ट्रस्ट के प्रारिम्भक सदस्यों में से थे। उन्हें उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य संस्थान के साहित्य भूषण सम्मान मिलने के अवसर पर ट्रस्ट ने भी उन्हें सम्मानित किया था। कुछ समय पूर्व ट्रस्ट के तत्वावधान में पं. प्रेमशंकर मिश्र जी का एकल काव्यपाठ आयोजित किया गया था जिसे सहित्य प्रेमियों ने बहुत सराहा था। शोकाकुल मन से हमें यह कहना पड़ रहा है कि उनके अवसान से ट्रस्ट ने अपना अतिमहत्वपूर्ण और विशष्सनीय सहयोगी खो दिया है। यह हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है। पं. प्रेमशंकर मिश्र जी की स्मृतियॉं हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेंगी।
रघुवंश मणि
साहित्य सचिव
डॉ. रमाशंकर तिवारी त्रिभुवन ट्रस्ट
10, गंधमादन, लक्ष्मणपुरी फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश
शोक प्रस्ताव
कल 16.07.2008 की रात हिन्दी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि और संस्कृतिकमी पं. प्रेमशंकर मिश्र जी का 83 वषZ की अवस्था में फैज़ाबाद के जिला चिकित्सालय में एक सप्ताह की बीमारी के बाद निधन हो गया। पं. प्रेमशंकर मिश्र को कविता अपने पिता द्विजेष जी से परम्परा में प्राप्त हुई थी। प्रारिम्भक दौर की पारम्परिक कविताओं के बाद वे नयी कविता और नवगीत आन्दोलनों से जुड़े और पर्याप्त ख्याति अर्जित की। प्रसिद्ध नवगीतकार शंभुनाथ सिंह ने मिश्र जी की कविताओं को अपने नवगीत संकलन नवगीत अर्धशती में स्थान देकर आपके महत्व को दषZया था। जीवन के अन्तिम दिनों तक वे कविता और संस्कृति के प्रति समर्पित रहे। सामान्य जीवन के सुखों और दुखों को अभिव्यक्ति देने वाली प्रेमशंकर मिश्र जी की कविता में साहित्य की कई परम्पराएं एक साथ चलती दिखायी देती हैं। पं. मिश्र जी के निधन से कविता की इन धाराओं की गंभीर क्षति हुई है।
संस्कृतिक परिवेश के निर्माण के उद्देश के प्रति समर्पित पं. प्रेमशंकर मिश्र जी की संस्था सम्पर्क ने फैजाबाद में साहित्य और संस्कृति से जुड़ी कई पीढ़ियों के लिए आगे बढ़ने का आधार निर्मित किया। अपनी संवादधमी प्रकृति के चलते वे विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े लोगों से विचार-विमष करते रहे। मनोविनोद की उनकी जीवन्त प्रवृत्ति ने साहित्यजगत में ही नहीं वरन् सामान्य जीवन में भी उन्हें लोकप्रिय बनाया। फैज़ाबाद के साहित्य और संस्कृति जगत में उनका अविस्मरणीय योगदान सदा याद किया जायेगा।
वे डॉ. रमाशंकर तिवारी त्रिभुवन ट्रस्ट के प्रारिम्भक सदस्यों में से थे। उन्हें उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य संस्थान के साहित्य भूषण सम्मान मिलने के अवसर पर ट्रस्ट ने भी उन्हें सम्मानित किया था। कुछ समय पूर्व ट्रस्ट के तत्वावधान में पं. प्रेमशंकर मिश्र जी का एकल काव्यपाठ आयोजित किया गया था जिसे सहित्य प्रेमियों ने बहुत सराहा था। शोकाकुल मन से हमें यह कहना पड़ रहा है कि उनके अवसान से ट्रस्ट ने अपना अतिमहत्वपूर्ण और विशष्सनीय सहयोगी खो दिया है। यह हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है। पं. प्रेमशंकर मिश्र जी की स्मृतियॉं हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेंगी।
रघुवंश मणि
साहित्य सचिव
Sunday, April 06, 2008
लेखक और प्रकाशक
लेखक और प्रकाशक
हिन्दी जगत में लेखक और प्रकाशक के बीच बनते बिगड़ते सम्बन्धों पर अक्सर अनौपचारिक चर्चाएँ होती रही हैं। बातचीत के दौरान लेखकगण पारिश्रमिक कम मिलने या न मिलने की शिकायत करते रहे हैं। इसके विपरीत प्रकाशक पुस्तकों के न बिकने का रोना रोते रहते हैं। वे यह दलील देते रहे हैं कि पुस्तकें बिकतीं ही नहीं हैं अत: पारिश्रमिक वे दें भी तो कैसे? इधर रायल्टी के मुद्दे पर गगन गिल और महाश्वेतादेवी के वक्तव्यों को लेकर लेखकों और प्रकाशकों के बीच के सम्बन्ध पुन: बहस में आ गये हैं। इस प्रकरण को किसी एक हिन्दी प्रकाशक से जोड़कर देखने के बजाय हिन्दी जगत की सामान्य समस्या के रूप में देखा ताना चाहिए। मेरे विचार से प्रकाशकों की ओर से इस विषय पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार करने की जरूरत है।
साहित्य के समुचित विकास के लिए लेखकों और प्रकाशकों के बीच सकारात्मक सम्बन्ध होना जरूरी है। साहित्य जगत में प्रकाशन एक व्यवसाय है, मगर यह अन्य व्यवसायों से थोड़ा अलग होना चाहिए क्योंकि साहित्य स्वयं में आदर्शों की वकालत करता है। यदि आदर्श शब्द थोड़ा पुरातनपंथी लगे तो मूल्य की बात की जा सकती है। जीवन मूल्यों के संवाहक साहित्य के प्रकाशकों में लेखकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है।
यह विचित्र सी बात है कि हिन्दी की तुलना में अंग्रेजी के प्रकाशक बेहतर पारिश्रमिक देते हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि अंग्रेजी पुस्तकों का व्यापार अधिक लम्बा-चौड़ा है जिसके चलते वे अच्छा पारिश्रमिक दे लेते हैं। लेकिन यह कोई बहुत मतलब का तर्क नहीं क्योंकि हिन्दी पुस्तकों की खरीद कोई कम नहीं। पुस्तकालयों और सरकारी खरीद ही काफी होती है। अंग्रेजी प्रकाशकों के यहाँ पुस्तक प्रकाशन के समय जहाँ सारी बातें लिखित तौर पर होती हैं वहाँ हिन्दी में अधिकांशत: यह सारा कार्यकलाप मौखिक और आश्वासनधर्मी होता है। एक अंग्रेजी के लेखक ने बताया कि वह पहले हिन्दी में ही लिखता था लेकिन प्रकाशकों का रवैया ऐसा था कि उसने अंग्रेजी में लिखना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि वहाँ पैसा ही नहीं सम्मान भी अधिक है।
डॉ मैनेजर पाण्डेय ने एक बार कहा था कि हिन्दी के प्रकाशक वस्तुत: हिन्दी के अन्धकारक हैं। कारण यह कि वे बिक्री के लिए पाठकों पर बहुत निर्भर नहीं करते। इधर वितरण की एक ऐसी व्यवस्था विकसित हुई है जिसमें पाठक आनुसंगिक महत्व का रह गया है। पाठक के महत्व के घटने के साथ-साथ लेखक का महत्व भी घट गया है। इस दृष्टि से देखें तो यह एक भारी सांस्कृतिक समस्या है जिसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। प्रकाशक यह समझता है कि जब सब काम वही कर रहा है तो फिर लेखक को पैसे क्यों दिये जाँय।
हिन्दी के एक लेखक ने जब अपने प्रकाशक से रायल्टी का हिसाब माँगा तो उसने उत्तर में लिखा कि यदि लेखक अपनी प्रकाशित पुस्तकों की सभी प्रतियाँ खरीद ले तो वह रायल्टी दे देगा। यह बेहद अपमानजनक उत्तर था जो किसी भी तरह से उचित नहीं। रायल्टी के लफड़े से तंग आकर बहुत से हिन्दी लेखक अब 'लंप सम' मांगते हैं क्योंकि पुस्तकों की बिक्री का कुछ भी पता लगा पाना लेखक के लिए संभव नहीं होता।
सवाल यह है कि जिन लेखकों को प्रकाशकगण छापते हैं, उनके अधिकारों और सम्मान का ख्याल रखना क्या उनका भी धर्म नहीं है?
हिन्दी जगत में लेखक और प्रकाशक के बीच बनते बिगड़ते सम्बन्धों पर अक्सर अनौपचारिक चर्चाएँ होती रही हैं। बातचीत के दौरान लेखकगण पारिश्रमिक कम मिलने या न मिलने की शिकायत करते रहे हैं। इसके विपरीत प्रकाशक पुस्तकों के न बिकने का रोना रोते रहते हैं। वे यह दलील देते रहे हैं कि पुस्तकें बिकतीं ही नहीं हैं अत: पारिश्रमिक वे दें भी तो कैसे? इधर रायल्टी के मुद्दे पर गगन गिल और महाश्वेतादेवी के वक्तव्यों को लेकर लेखकों और प्रकाशकों के बीच के सम्बन्ध पुन: बहस में आ गये हैं। इस प्रकरण को किसी एक हिन्दी प्रकाशक से जोड़कर देखने के बजाय हिन्दी जगत की सामान्य समस्या के रूप में देखा ताना चाहिए। मेरे विचार से प्रकाशकों की ओर से इस विषय पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार करने की जरूरत है।
साहित्य के समुचित विकास के लिए लेखकों और प्रकाशकों के बीच सकारात्मक सम्बन्ध होना जरूरी है। साहित्य जगत में प्रकाशन एक व्यवसाय है, मगर यह अन्य व्यवसायों से थोड़ा अलग होना चाहिए क्योंकि साहित्य स्वयं में आदर्शों की वकालत करता है। यदि आदर्श शब्द थोड़ा पुरातनपंथी लगे तो मूल्य की बात की जा सकती है। जीवन मूल्यों के संवाहक साहित्य के प्रकाशकों में लेखकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है।
यह विचित्र सी बात है कि हिन्दी की तुलना में अंग्रेजी के प्रकाशक बेहतर पारिश्रमिक देते हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि अंग्रेजी पुस्तकों का व्यापार अधिक लम्बा-चौड़ा है जिसके चलते वे अच्छा पारिश्रमिक दे लेते हैं। लेकिन यह कोई बहुत मतलब का तर्क नहीं क्योंकि हिन्दी पुस्तकों की खरीद कोई कम नहीं। पुस्तकालयों और सरकारी खरीद ही काफी होती है। अंग्रेजी प्रकाशकों के यहाँ पुस्तक प्रकाशन के समय जहाँ सारी बातें लिखित तौर पर होती हैं वहाँ हिन्दी में अधिकांशत: यह सारा कार्यकलाप मौखिक और आश्वासनधर्मी होता है। एक अंग्रेजी के लेखक ने बताया कि वह पहले हिन्दी में ही लिखता था लेकिन प्रकाशकों का रवैया ऐसा था कि उसने अंग्रेजी में लिखना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि वहाँ पैसा ही नहीं सम्मान भी अधिक है।
डॉ मैनेजर पाण्डेय ने एक बार कहा था कि हिन्दी के प्रकाशक वस्तुत: हिन्दी के अन्धकारक हैं। कारण यह कि वे बिक्री के लिए पाठकों पर बहुत निर्भर नहीं करते। इधर वितरण की एक ऐसी व्यवस्था विकसित हुई है जिसमें पाठक आनुसंगिक महत्व का रह गया है। पाठक के महत्व के घटने के साथ-साथ लेखक का महत्व भी घट गया है। इस दृष्टि से देखें तो यह एक भारी सांस्कृतिक समस्या है जिसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। प्रकाशक यह समझता है कि जब सब काम वही कर रहा है तो फिर लेखक को पैसे क्यों दिये जाँय।
हिन्दी के एक लेखक ने जब अपने प्रकाशक से रायल्टी का हिसाब माँगा तो उसने उत्तर में लिखा कि यदि लेखक अपनी प्रकाशित पुस्तकों की सभी प्रतियाँ खरीद ले तो वह रायल्टी दे देगा। यह बेहद अपमानजनक उत्तर था जो किसी भी तरह से उचित नहीं। रायल्टी के लफड़े से तंग आकर बहुत से हिन्दी लेखक अब 'लंप सम' मांगते हैं क्योंकि पुस्तकों की बिक्री का कुछ भी पता लगा पाना लेखक के लिए संभव नहीं होता।
सवाल यह है कि जिन लेखकों को प्रकाशकगण छापते हैं, उनके अधिकारों और सम्मान का ख्याल रखना क्या उनका भी धर्म नहीं है?
Monday, January 14, 2008
एक स्त्रीवादी चुटकुला
एक स्त्रीवादी चुटकुला
एक दिन उल्लू बहुत उदास था। वह रात भर चुप्पी साधे रहा। लक्ष्मी जी ने उससे पूछा, ''प्रिय उल्लू तुम इतने उदास क्यों हो? अपनी उदासी का कारण मुझे बतलाओ।''
उलूक महोदय ने जवाब दिया, '' लक्ष्मी जी मैं आपको रोज ढोता रहता हूँ। आपकी इतनी सेवा करता हँ। मगर मेरा कोई महत्व नहीं हो पाया है। दीपावली के दिन सारी दुनिया में आपकी पूजा होती है, मगर मुझे कोई नहीं पूँछता। अब ये क्या बात हुई? उल्टे लोग मुझे उल्लू कहकर चिढ़ाते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है।''
लक्ष्मी जी ने अपने वाहन के दुख को समझा और किंचित विचार करते हुए बोलीं ,'' ठीक है प्रिय उलूक। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें आशिर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारी पूजा मुझसे पहले हुआ करेगी। तुम्हारी पूजा दीपावली से पहले करवा चौथ के दिन हुआ करेगी।
तभी से करवा चौथ मनाया जाने लगा।
एक दिन उल्लू बहुत उदास था। वह रात भर चुप्पी साधे रहा। लक्ष्मी जी ने उससे पूछा, ''प्रिय उल्लू तुम इतने उदास क्यों हो? अपनी उदासी का कारण मुझे बतलाओ।''
उलूक महोदय ने जवाब दिया, '' लक्ष्मी जी मैं आपको रोज ढोता रहता हूँ। आपकी इतनी सेवा करता हँ। मगर मेरा कोई महत्व नहीं हो पाया है। दीपावली के दिन सारी दुनिया में आपकी पूजा होती है, मगर मुझे कोई नहीं पूँछता। अब ये क्या बात हुई? उल्टे लोग मुझे उल्लू कहकर चिढ़ाते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है।''
लक्ष्मी जी ने अपने वाहन के दुख को समझा और किंचित विचार करते हुए बोलीं ,'' ठीक है प्रिय उलूक। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें आशिर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारी पूजा मुझसे पहले हुआ करेगी। तुम्हारी पूजा दीपावली से पहले करवा चौथ के दिन हुआ करेगी।
तभी से करवा चौथ मनाया जाने लगा।
साहित्य/संस्कृतिकर्म और राजनीति
साहित्य और संस्कृतिकर्म की अवस्थिति को यदि सूक्ष्मतापूर्वक देखें तो वह राजनीति की अपनी अवस्थिति से अलग केन्द्रित मिलेगी। राजनीतिक लोगों की प्राथमिकताएँ भिन्न प्रकार की होती हैं। अपनी व्यावहारिक अपरिहार्यताओं के चलते वे तमाम साहित्यिक/सांसकृतिक मूल्यों को अनदेखा कर देते हैं। हमारे समय में वोटों की राजनीति का यही अर्थ बनता है। वोटों के लिए सारे मूल्य और सिध्दान्त ताक पर रख दिये जाते हैं।
यदि बिल्कुल ऐसा न भी हो तो राजनीतिक संगठन अक्सर विभिन्न मौकों पर ऐसे समझौते करते हैं जो विसंगतिपूर्ण लगते हैं। समाजवाद से लेकर साम्यवाद तक की विचारसरणि में इस प्रकार के समझौते किये गये कि इन विचाारधाराओं से जुड़े मूल्यों का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया। साम्यवाद किस प्रकार रूष में स्आलिनवाद में बदल गया इसकी कहानी बड़ी अजीब है। भारत में लोहियावाद कैसे जातिवाद में बदल गया और अम्बेडकरवाद किस प्रकार ब्राहम्ण दलित गठजोड़ में बदल गया इसे बताना बहुत कठिन नहीं। मैं यह नहीं कहता कि किसी विचार या विचारधारा को लेकर जड़ता या कट्टरता होनी चाहिये। मेरा सिर्फ यह कहना है कि ऐसे समझौते नहीं होने चाहिए जिससे विचारधारा में अन्तर्निहित मूल्य ही गायब हो जायँ।
इस बात को हम अनेक ऐतिहासिक सन्दर्भों में साफ रेखांकित कर सकते हैं। कुछ बर्षों पहले भाजपा सरकार के सन्दर्भ में यह देखा गया कि दक्षिणपंथी सांस्कृतिक संगठनों और राजनीतिक पार्टी के बीच का अन्तराल स्पष्ट था। सांस्कृतिक संगठन राजनीतिज्ञों से संतुष्ट न थे। इस बात को हम स्वाधीनता की लड़ाई के दौर में प्रेमचनद के लेखन और कांग्रेसी राजनीति के बीच के अन्तरों में देख सकते हैं। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत लोग अक्सर परिवर्तनों को पहले देख लेते हैं।
मैं यहाँ यह तो नहीं कहना चाहता कि साहित्य को राजनीति से अलग देखा जाय। हमारे आज के दौर में यह विल्कुल संभव नहीं। मगर साहित्य की अपनी अस्मिता का प्रश्न इसीलिए महत्वपूर्ण है।
यदि बिल्कुल ऐसा न भी हो तो राजनीतिक संगठन अक्सर विभिन्न मौकों पर ऐसे समझौते करते हैं जो विसंगतिपूर्ण लगते हैं। समाजवाद से लेकर साम्यवाद तक की विचारसरणि में इस प्रकार के समझौते किये गये कि इन विचाारधाराओं से जुड़े मूल्यों का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया। साम्यवाद किस प्रकार रूष में स्आलिनवाद में बदल गया इसकी कहानी बड़ी अजीब है। भारत में लोहियावाद कैसे जातिवाद में बदल गया और अम्बेडकरवाद किस प्रकार ब्राहम्ण दलित गठजोड़ में बदल गया इसे बताना बहुत कठिन नहीं। मैं यह नहीं कहता कि किसी विचार या विचारधारा को लेकर जड़ता या कट्टरता होनी चाहिये। मेरा सिर्फ यह कहना है कि ऐसे समझौते नहीं होने चाहिए जिससे विचारधारा में अन्तर्निहित मूल्य ही गायब हो जायँ।
इस बात को हम अनेक ऐतिहासिक सन्दर्भों में साफ रेखांकित कर सकते हैं। कुछ बर्षों पहले भाजपा सरकार के सन्दर्भ में यह देखा गया कि दक्षिणपंथी सांस्कृतिक संगठनों और राजनीतिक पार्टी के बीच का अन्तराल स्पष्ट था। सांस्कृतिक संगठन राजनीतिज्ञों से संतुष्ट न थे। इस बात को हम स्वाधीनता की लड़ाई के दौर में प्रेमचनद के लेखन और कांग्रेसी राजनीति के बीच के अन्तरों में देख सकते हैं। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत लोग अक्सर परिवर्तनों को पहले देख लेते हैं।
मैं यहाँ यह तो नहीं कहना चाहता कि साहित्य को राजनीति से अलग देखा जाय। हमारे आज के दौर में यह विल्कुल संभव नहीं। मगर साहित्य की अपनी अस्मिता का प्रश्न इसीलिए महत्वपूर्ण है।
Subscribe to:
Posts (Atom)