साहित्य और संस्कृतिकर्म की अवस्थिति को यदि सूक्ष्मतापूर्वक देखें तो वह राजनीति की अपनी अवस्थिति से अलग केन्द्रित मिलेगी। राजनीतिक लोगों की प्राथमिकताएँ भिन्न प्रकार की होती हैं। अपनी व्यावहारिक अपरिहार्यताओं के चलते वे तमाम साहित्यिक/सांसकृतिक मूल्यों को अनदेखा कर देते हैं। हमारे समय में वोटों की राजनीति का यही अर्थ बनता है। वोटों के लिए सारे मूल्य और सिध्दान्त ताक पर रख दिये जाते हैं।
यदि बिल्कुल ऐसा न भी हो तो राजनीतिक संगठन अक्सर विभिन्न मौकों पर ऐसे समझौते करते हैं जो विसंगतिपूर्ण लगते हैं। समाजवाद से लेकर साम्यवाद तक की विचारसरणि में इस प्रकार के समझौते किये गये कि इन विचाारधाराओं से जुड़े मूल्यों का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया। साम्यवाद किस प्रकार रूष में स्आलिनवाद में बदल गया इसकी कहानी बड़ी अजीब है। भारत में लोहियावाद कैसे जातिवाद में बदल गया और अम्बेडकरवाद किस प्रकार ब्राहम्ण दलित गठजोड़ में बदल गया इसे बताना बहुत कठिन नहीं। मैं यह नहीं कहता कि किसी विचार या विचारधारा को लेकर जड़ता या कट्टरता होनी चाहिये। मेरा सिर्फ यह कहना है कि ऐसे समझौते नहीं होने चाहिए जिससे विचारधारा में अन्तर्निहित मूल्य ही गायब हो जायँ।
इस बात को हम अनेक ऐतिहासिक सन्दर्भों में साफ रेखांकित कर सकते हैं। कुछ बर्षों पहले भाजपा सरकार के सन्दर्भ में यह देखा गया कि दक्षिणपंथी सांस्कृतिक संगठनों और राजनीतिक पार्टी के बीच का अन्तराल स्पष्ट था। सांस्कृतिक संगठन राजनीतिज्ञों से संतुष्ट न थे। इस बात को हम स्वाधीनता की लड़ाई के दौर में प्रेमचनद के लेखन और कांग्रेसी राजनीति के बीच के अन्तरों में देख सकते हैं। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत लोग अक्सर परिवर्तनों को पहले देख लेते हैं।
मैं यहाँ यह तो नहीं कहना चाहता कि साहित्य को राजनीति से अलग देखा जाय। हमारे आज के दौर में यह विल्कुल संभव नहीं। मगर साहित्य की अपनी अस्मिता का प्रश्न इसीलिए महत्वपूर्ण है।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


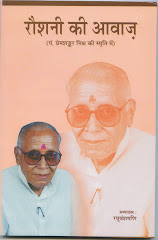


No comments:
Post a Comment