ईश्वर, सत्ता और कविता 2
ईश्वर और धर्म को लेकर प्रचलित मानववादी दृष्टि का हिन्दी कविता में अभाव नहीं। गांधीवाद के दौर मेें इस व्यापक दृष्टि की राजनीति भी बड़ी व्यापक थी जिसका सैध्दान्तिक प्रतिफलन 'सर्वधर्म समभाव' में देखा गया। धर्म निरपेक्षता का यह व्यापक तौर पर स्वीकृत रूप था और यह रूप उस समय के साहित्य मेंे पर्याप्त दृष्टिगोचर है। सांप्रदायिकता के विरुध्द लड़ने का यह भी एक शस्त्र रहा। अपने व्यापक परिप्रेक्ष्य के चलते यह एक सकारात्मक विजन भी बना रहा जिसके तहत मनुष्य को ईश्वर में और ईश्वर को मनुष्य में देख पाने की अवधारणा विकसित हुई। यह विजन इतना पुराना है कि इसकी परिपाटी भक्ति युग के सूफी और निर्गुण कवियों तक जायेगी। यदि थोड़ी जबर्दस्ती की जाय तो वेद से भी प्रारंभ किया जा सकता है - अर्थात कविता के प्रारंभ से ही प्रारंभ।
लेकिन इन मानववादी कवियाें की तुलना वैदिक अथवा भक्ति युग के कवियो से करना गलता होगा। ईश्वर की सम्पूर्ण सत्ताा और उसके आगे निरा समर्पित रहने वाला भक्तिभाव इन कवियो में नहीं। न ही यह ईश्वर उनकी कविता का केन्द्रीय विङ्ढय बनता है जैसा कि भक्ति युग के साहित्य में है। नवजागरण पर चल रही सारी खींचा-तानी के बाद भी यह स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि ईश्वर प्रत्यय सम्बन्धी दार्शनिक सोच के मामले में भक्ति कवि, सन्त अगस्ताइन जैसे यूरोपियन मध्ययुगीनों से बहुत आगे नहीं। मगर ये मानवतावादी कवि तो आधुनिकता में पाँव डाले हुए हैं। भक्तियुग की अन्तिम परछायीं हिन्दी साहित्य में निराला की कविता में दिखलायी पड़ती है और वहीं से उससे मुक्त होने का मार्ग भी दृष्टिगोचर होता है। वैसे निराला स्वयं भक्ति के कवि तो कतई नहीं। भक्ति है भी तो छायावाद और आधुनिकता के फार्मे में। अत: इस पूरे विश्लेङ्ढण में निराला से पहले के समय में जाने की जरूरत नहीं महसूस होती।
इस मानववादी दृष्टि की विशेङ्ढता यह है कि इस दार्शनिक अवस्थिति में ईश्वर की सत्ता मनुष्य की सत्ता से जुड़ जाती है। हरिजन, दलित, मजदूर, किसानों में ईश्वर की प्राप्ति इसी अर्थ मे है और रवीन्द्रनाथ टैगोर ऐसी कविताएं लिखने वाले एकमात्र कवि नहीं। ऐसी कविताएं हिन्दी में कम नहीं जिनमें मनुष्य को ईश्वर का रूप बतलाया गया हो और उसकी अवहेलना करके होने वाली ईश्वर भक्ति को पाखण्ड और ढोंग बताया गया हो। ईश्वर की इस मानवीय सत्ता के दर्शन की आवश्यकता हमारे समय में साम्प्रदायिकता के बरक्स बार-बार दिखाई दी और धर्मनिरपेक्षता के समर्थकों द्वारा बार-बार पीछे जाकर इन कवियों में अपनी परंपरा तलाशने की बेचैनी इसी का प्रतिफलन है। यह देखने की बात है कि टैगोर एक तरफ ईश्वर को सामान्य जनता में तलाशते हैं तो दूसरी तरफ साम्प्रदायिकता के अंधकार को भाई-भाई के बीच हो रहे अज्ञानतापूर्ण अनुचित संघर्ङ्ढ के रूप में देखते है। ये दोनाें विचार दार्शनिक संस्तर पर नाभिनाल बध्द हैं।
राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से प्रादुर्भूत साम्प्रदायिक वैमनस्य के दौर मे इस दृष्0श्निV की ओर पुनर्वापसी स्वाभाविक थी। अनिल सिंह अपनी बहुचर्चित कविता 'अयोध्या' में उसे इस प्रकार रखते हैं।
'' मनुष्; रहते हैं इस शहर में
जिनमें रहता है भगवान
और चूंकी भगवान मनुष्; में रहता है
इसलिए वह अल्लाह भी हो सकता है''
फिर मनुष्; और उसका सामान्य नागरिक जीवन ईश्वर से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि-
''इतना ही यथार्थ है यह शहर जितना यह कि
आदमी का कलेजा काटकर उसकी जगह
शिवलिंग रख देने से वह मर जायेगा''
ईश्वर और मनुष्य की सत्ताा का एकाकार होना मानववादी कविता की एक प्रमुख विशेङ्ढता है। यह भी कहा जा सकता है कि इस कविता में मनुष्य ही ईश्वर हो जाता है। आगे चलें तो यह तथ्य सामने आता है कि मनुष्य के तिरस्कार पर ईश्वर और उसकी भक्ति ही निरर्थक हो जाती है। ऐसे में उसके प्रति भक्ति या श्रध्दा का कोई महत्व नहीं। बाह्याडम्बरों पर हुए आक्रमण इसी के चलते हैें। देखें तो ईश्वर और धर्म के प्रति यही सोच भारत मेें धर्मनिरपेक्षता का मूल बनती है और जिसके कुछ तत्व भक्ति युग में प्राप्त होते हैं। मनुष्य के कारण ही तो ईश्यर का अस्तित्व है वगर्ना धर्म का सारा ताना-बाना बेकार है। आध्यात्म के अखण्ड भाव में पूरे विश्व का समा जाना जरूरी है और मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे।
इस मानववाद की अभिव्यक्ति हमारे समय की साम्प्रदायिकता विरोधी हिन्दी कविता में तरह-तरह से हुई। नवल शुक्ल स्वयं को ईश्वर से अधिक पाते है क्योंकि ईश्वर युगों में पृथ्वी की सुधि लेते हैं जबकि कवि (मनुष्य) ''किसी भी जगह जनम लेकर'' पूरे ब्रह्माण्ड के बारे में सोचता है और ''अपनी क्षमता से अधिक रहने की कोशिश करता'' है। साम्प्रदायिकता के इस विकट दौर से पहले आने वाले कवि सर्वेश्वर के लिए-
'' इस दुनिया में
आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है
न ईश्वर
न ज्ञान
न चुनाव
न संविधान
इसके नाम पर कागज पर लिखी कोई भी इबारत
फाड़ी जा सकती है
और जमीन के भीतर गाड़ी जा सकती है''
केदारनाथ सिंह की कविताओं में ईश्वर का जिक्र एक मुहावरे के रूप में आता है। ऐसा सिर्फ केदारनाथ सिंह की कविता में नहीं अपितु बहुत से अन्य कवियों की भी कविताओं में है। वहां यह 'ईश्वर' एक भाव बोधक शब्द भी है, जो कविता से बाहर जीवन में घनघोर प्रचलन रखता है। इस अर्थ में यह शब्द 'ईश्वर' के दार्शनिक अथवा धार्मिक अर्थ सन्दर्भों से बिल्कुल अलग अस्तित्वमान है। 'हे राम' या 'राम नाम सत्य है' या 'खुदा कसम' जैसे वाक्यांशाें की तरह यह भाङ्ढा में विद्यमान है। यह एक जटिल प्रश्न है कि यह सत्ताा भाङ्ढा के इस प्रकार के स्वतंत्र लगने वाले प्रयोगों मेें किस प्रकार लगातार क्रियाशील करती है? इस लगातार बरकरार भाङ्ढायी तत्व में क्या कहीं दार्शनिक प्रत्ययों को भी वैधता तो नहीं प्राप्त होती? कैन्टरबरी के एनसेल्म ने ईश्वर के अस्तित्वमान होने का प्रमाण देते हुए कहा था कि 'ईश्वर' शब्द का होना ही उसके अस्तित्वमान होने का सबूत है। यह सत्ताा शब्दों के माध्यम से बनी रहती है। मेरे एक उर्दू पढ़ाने वाले मित्र ने बताया था कि किस प्रकार प्रारंभिक कक्षाओं में भाङ्ढा ज्ञान कराते समय ही बच्चों को शब्दों के माध्यम से ईश्वर और धर्म की घुट्टी पिला दी जाती है। लेकिन ईश्वर को गंभीरतापूर्वक न लेने वालों के बीच भी ईश्वर शब्द बना रहता है और प्रयोग से बाहर नहीं होता। यही वजह है कि ईश्वर संबन्धी कविताओं के गहरे अर्थों तक पहुंचने की जरूरत महसूस होती है।
मुहावरे की ही तरह ही ईश्वर के प्रति प्रार्थना के शिल्प में लिखी गयीं कविताएं किस प्रकार प्रार्थना की सीमा से बाहर निकलती है उसका उदाहरण है निराला की वे अन्तिम कविताएं जो सिर्फ प्रार्थनाएं न होकर स्वातंत्रोत्तर भारत की बदलती परिस्थितियाें में एक संवेदनशील कवि के मोहभंग की विशिष्ट कोटि की अभिव्यक्ति है। इस विङ्ढय पर कवि एवं आलोचक केदारनाथ सिंह ने एक बहुत प्रभावशाली लेख लिखा है। निराला अपनी इन कविताओं में ईश्वर के संदर्भ को अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर सूक्ष्म राजनीतिक अर्थ प्रदान करते हैैं।
'जय तुम्हारी देख भी ली
रूप की गुण की, सुरीली।
वृध्द हूँ मैं, ऋध्दि की क्या,
साधना की, सिध्दि की क्या?
खिल चुका है फूल मेरा,
पखड़ियाँ हो गयीं ढीली।
चढ़ी थी जो ऑंख मेरी,
बज रही थी जहाँ भेरी,
वहाँ सिकुड़न पड़ चुकी है,
बढ़ रही है रेख नीली।
आग सारी फुक चुकी है,
रागिनी वह रुक चुकी है,
याद करता हुआ जीवन,
जीर्ण जर्जर आज तीली।'
यही प्रार्थना का सबवर्जिव काव्य प्रारूप किस प्रकार ईश्वर के प्रति नकारात्मक रुख अख्तियार करता है यह यदि देखना हो तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 'ईश्वर' पर लिखित कविता देखने योग्य होगी। 'गर्म हवाएं' संग्रह में आयी यह कविता ऐसी अन्य कविताओं से घिरी है जो कवि के अपने व्यक्तिगत दु:खों, सामाजिक मोहभंग और व्यथित चुनावों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। संग्रह 'धीरे-धीरे' जैसी राजनीतिक कविता से प्रारंभ होता है जिसमें सर्वेश्वर एक 'क्रांतियात्रा' को 'शवयात्रा' में बदलते हुए देखते हैं। पत्नी की मृत्यु पर लिखी गयी एक अत्यन्त ही भावपूर्ण कविता के बाद आती है प्रार्थना कविताओं की ऋृंखला जिनमें कवि ईश्वर से शक्ति नहीं मांगता (प्रार्थना-1) 'दुर्गम पथ' मांगता है जिस पर उसके 'थके चरण' हों (प्रार्थना-2), अपनी सीमाओं का ध्यान और दुर्बलताओं का अभियान मांगता है (प्रार्थना-3)। पर अपनी कविता 'प्रार्थना-4' में वह ईश्वर का लगभग निङ्ढेध करता है।
'यही प्रार्थना है प्रभु तुमसे
जब हारा हूं तब न आइये।'
कवि अपने शौर्य की तो सराहना चाहता है, मगर वह ईश्वर के चरणों में नहीं गिरना चाहता। वह जानता है कि संसार में दु:ख की ऑंखें बहुत बड़ी है और उसके एक अश्रु की आयु के सामने कल्पचक्र अस्वीकार्य है। और इन प्रार्थनाओं के बाद आती है कविता 'ईश्वर'। सर्वेश्वर की यह कविता निश्चित रूप से दु:ख से भीगी हुई है। व्यक्तिगत दु:ख और मोहभंग से घिरी हुई यह कविता ईश्वर को एक ठोस रूप में प्रस्तुत करती है जो एक व्यापारी या बॉस की तरह 'बहुत लम्बी जेबों वाला कोट' पहनकर आता है और कवि की माँ, पिता, पत्नी और बच्चे को खिलौनों की तरह जेब में रखकर चला जाता है। कवि के लिए दुनियाँ छोड़ जाता है, जिसमें उसे बहलाने के लिए और बहुत से खिलौने हैं। आगे कवि लिखता है,
'मैंने सुना है
उसने कहीं खोल रखी है
खिलौनो की दूकान,
अभागे के पास
कितनी जरा सी पूँजी है
रोजगार चलाने के लिए।'
एक खिलौने के व्यापारी के रूप में ईश्वर का अवमूल्यन उसे हास्यास्पद बना देता है। ईश्वर की इतनी ठोस उपस्थिति सिर्फ उसके लम्बे कोट की वजह से बन पड़ी है, जो प्रभु की इमेज को इस कविता में सुनिश्चित करता है। यह सर्वेश्वर की प्रार्थना श्रृंखला की कविताओं में उपस्थित पारंपरिक प्रार्थनाभाव की बची-खुची संभावनाओं को भी ध्वस्त कर देता है और उनमें निहित दूसरे प्रतिरोधी भावों को आलोकित करता है। यह प्रश्न भी उठता है कि वह जो कुछ भी है- ईश्वर है भी या कोई और। सर्वेश्वर की ये कविताएं उस अस्पष्ट भूमि पर खड़ी है, जहाँ ईश्वर सत्ता का प्रतीक बनता दिखाई देता है। ईश्वर की सत्ता के प्रति प्रार्थना के ही शिल्प में व्यंगाात्मक सूक्ष्म कटाक्ष भरे प्रयोग किस प्रकार प्रभावपूर्ण हो सकते हैं इसका एक उदाहरण है शमशेर बहादुर सिेह की द्वारा भजन के शिल्प में प्रस्तुत यह कविता:
हरि मोरी आड़, हरि ही मोरी आड़॥
हरि मोरी झाँकी, हरि ही केंवाड़॥
हरि जमुना-मंथन मोरे, हरि ही
थाम्हे दुख के पहाड़॥
हरि संग ज्ञान-ध्यान मोहे मधुऋतु
हरि बिन सकल उजाड़॥
मज्जा-भेद बसे हरि अंतर
हरि संबल मोरे हाड़॥
जग बाड़व में जनम-जनम लौं
झोंक्यों कितने भाड़॥
तब आयो समसेरु मुकति को
परलौ मास असाढ़॥
हरि मोरी आड़, हरि ही मोरी आड़॥
सांप्रदायिक उन्माद के भीषण दौर से पूर्वं, अर्थात 1990 से पहले के समय की समकालीन हिन्दी कविता में ईश्वर की उपस्थिति की तुलना मेें बाद की कविताओं में उसकी उपस्थिति काबिले गौर है। स्वप्निल श्रीवास्तव की कविताओं मे ईश्वर की उपस्थिति एक वैचाारिक द्वंद्व का परिणाम है। 'ईश्वर एक लाठी है' कविता इस अर्थ में ध्यातव्य है। यहां कवि अपने पिता जैसे बूढे लोगाें के लिए ईश्वर के निहितार्थ को समझने की कोशिश करता है। इस कविता में यदि पिता के ईश्वर में विश्वास के प्रति सहानुभूति है तो उस विश्वास की व्यर्थता का भी एहसास है। ईश्वर पिता के लिए एक ऐसी लाठी है जिसे वे अक्सर तान देते है। उन्होंने इस लाठी को जिन्दगी भर मजबूत रखने की कोशिश की है, मगर उन्हें लाठी में घुन के चालने की आवाज सुनायी देती है। अपनी जीवन भर की आस्था के बाद भी वे यह नहीं जान सके हैं कि ईश्वर आखिर किस कोठ की लाठी है। स्वप्निल श्रीवास्तव की इस कविता के तमाम निहितार्थ निकलते हैं, विशेषरूप से इस कारण कि कवि के काव्यानुशासन में कविता के अर्थ एक दिशा में चलते हुए भी विभिन्न संस्तरों पर खुलते है। एक आस्तिक पिता के द्वंद को यह बखूबी रेखांकित करने वाली कविता है जिसके लिए ईश्वर एक ऐसा सहारा है जो कमजोर होता जा रहा है, मगर जिसे त्याग पाना उसके तर्क स्वभाव में कहीं दूर-दूर तक नहीं।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


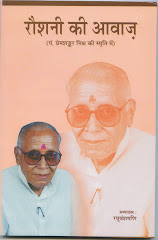


4 comments:
'ईश्वर सत्ता और कविता' पर विचार करते हुए आपने स्वप्निल श्रीवास्तव की कविता 'ईश्वर एक लाठी है' पर अपना जो मत प्रस्तुत किया है, उसके सन्दर्भ में विनम्रतापूर्वक मैं अपना असन्तोष दर्ज़ करता हूँ।
भारतीय और विशेष रूप से, हिन्दू परम्परा में ईश्वर की जो संकल्पना रही है, उससे हटते हुए यह उसका एक सर्जनात्मक ऐहिक रूपान्तरण है। पारम्परिक और प्रचलित ईश्वरबोध का एक सजग प्रत्याख्यान इस कविता में है, लेकिन यदि उसकी तीव्र खण्डनात्मकता का पता हमें इस कविता में ऊपरी तौर पर नहीं लगता तो इसकी वजह कविता की वह बुनावट है, जो अपने अर्थ-संश्लेष में कई स्तरों को साथ लेकर चलती है। ऐसा लगता है कि ईश्वर के होने को लेकर कविता की पहली पंक्ति में प्रकट तौर पर जो विधेयात्मक कथन है, उसको आपने उसके व्यंग्यार्थ से अलग करते हुए ईश्वर के अस्तित्व से जोड़ दिया है।
कविता की सीधी प्रस्तावना है कि एक वृध्द होते जा रहे पिता के लिए उसकी लाठी ही ईश्वर है। उसके जीवन से और कोई भी वस्तु इतना गहरा तादात्म्य नहीं बना पाती जितना कि यह लाठी, और जो वास्तव में अब उनका तीसरा पैर हो गई है। इस पूरी कविता में एक वृध्द होते पिता के वर्तमान जीवन को उसके तादात्म्य-अंशों में देखने की कोशिश है। दुर्भाग्य या सौभाग्य से, इस तादात्म्य-अंश में ईश्वर कहीं नहीं है। यह एक ठेठ लौकिक जीवन का तादात्म्य है - जिसकी पारस्परिकता शाश्वत भले ही न हो, लेकिन अपनी क्षणभंगुरता में भी एक दूसरे को सम्भालती और समर्थन देती है। एक वृध्द होता पिता और दूसरी तरफ एक वृध्द होती लाठी! लाठी के वृध्द होते जाने को स्वप्निल उसके भीतर घुनों के चलने से व्यंजित करते हैं और साथ ही नींद में पहुँचने का एक हल्का 'सर्रियलिस्टिक' बिम्ब भी है जो पिता के अवचेतन में उस लाठी की उपस्थिति को, क्षीणता को लेकिन उन दोनों की सम्बन्धपरकता को बहुत जीवन्त और आत्मीय ढंग से प्रत्यक्ष करती है। यह ईश्वर नहीं है जो अशक्त पिता को संभालता है, यह दुनिया की एक दूसरी निरन्तर नष्ट होती वस्तु है, जो एक नष्ट होते पिता को अपना समर्थन सौंपती है। और यही इस कविता की मार्मिकता है। कवि ने इस लाठी को एक जीवन्त इकाई बनाने की कोशिश की है - और कई बार तो वह उस वृध्द होते पिता की अभिव्यक्ति भी बन जाती है। विपत्ति में तने हुआ पिता का चेहरा और उसकी तनी हुई लाठी लगता है एक ही व्यक्ति की दो मुद्राएँ हैं! एक ऐसी मुद्रा जो सिर्फ पिता की ही हो सकती है, सुन्दर और मजबूत भी - 'क्या दुनिया में होगी किसी के पास / इतनी सुन्दर मजबूत लाठी!'
स्वप्निल की इस कविता में ईश्वर का यह प्रत्याख्यान सैध्दान्तिक या दार्शनिक स्तर पर नहीं है और यही इस कविता की सफलता है। 'ईश्वर' शब्द में जो शक्तिमत्ताा है, जीवन देने की प्रतीकात्मकता है, ढाढस और साहस देने का जो परम्परित विश्वास है, उन सबको पूर्वनिर्धारित संकेतों से हटाकर कविता में इसे 'लाठी' में स्थानांतरित कर दिया गया है। ईश्वर शब्द को बनाये रखते हुए इसकी अवधारणा में हमारे ऐहिक अनुभवों के सन्दर्भ में एक बड़ा परिवर्तन! पिता के जीवन और ज्ञान का यह लाठी जहाँ एक हिस्सा है, वहीं ईश्वर उससे बहिष्कृत है। वह कभी नहीं जान सके कि ईश्वर किस कोठ की लाठी है। लाठी सफल ईश्वर है और ईश्वर एक असफल व अनुपयोगी विचार!
मुझे आश्चर्य है कि आपने इसे 'एक आस्तिक पिता के द्वन्द्व को बखूबी रेखांकित करने वाली कविता' के रूप में पढ़ा है और साथ ही 'जिसके लिए ईश्वर एक ऐसा सहारा है, जो कमजोर होता जा रहा है और इसे त्याग पाना उसके तर्क-स्वभाव में कहीं दूर-दूर तक नहीं है।' पिता की आस्तिकता केवल जीवन और उसकी सहजता में है और उसके तईं द्वंद्व तो पूरी कविता में कहीं नहीं है। आलोचक को यह द्वन्द्व क्यों दीखता है, समझ में नहीं आया, कहीं यह आलोचक का अपना तो 'द्वंद्व' नहीं?
मैं स्पष्टत: नास्तिक हूँ। अत:आलोचना में मेरा कोई अन्तर्द्वन्द्व नहीं हो सकता है।
कविता में पिता के नास्तिक होने का कोई प्रमाण नहीं है।
ईश्वर का सुन्दरतम लाठी होना स्वयम् में पिता के आस्तिक होने की ओर संकेत है। लाठी के प्रति शंकालु होना उनका अन्तर्द्वन्द्व है। उसका आधार भैितिक जगत है जिसके तर्क ईश्वर के अस्तित्वमान होने के विरुध्द जाते हैं।
फिलहाल अच्छी कविताओं की कई व्याख्याएँ होती हैं। यही सिध्द हुआ।
प्राय: गॉंव में जब लाठियों की तुलना की जाती है और लोग लाठियों को हाथ में लेकर देखते हैं व उसकी मजबूती व मारक शक्ति की तुलना करते हैं तो यह सवाल बार बार उठता है कि यह किस कोठ (बाँसों का कोठ)की लाठी है जो इतनी मजबूत है या फिर इतनी कमज़ोर है। कविता में पिता को अपनी लाठी की शक्ति पर पूरा भरोसा है, जिसे हम एक तरह के गर्व में परिणत होते देखते हैं। लेकिन जब कविता की अंतिम पंक्ति कहती है कि ईश्वर किस कोठ की लाठी है, तो यह स्पष्ट होता है कि कवि ईश्वर की अशक्तता पर व्यंग्य कर रहा है। पिता ईश्वर को एक कमजोर लाठी मानते हैं और इसीलिए उन्हें यह अचरज है कि ईश्वर आख्रिर किस कोठ की लाठी है जो इतनी कमजोर है। इसलिये अगर ईश्वर को कमजोर और अशक्त मानने में भी एक तरह की आस्तिकता सम्भव हो तो हम यह मान सकते हैं कि कविता का पिता आस्तिक है।
रघुवंशजी आपको धन्यवाद कि आपने समय निकालकर टिप्पणी पर अपना जवाब सामने रखा. ईश्वर के सुन्दरतम लाठी होने की व्यंजना यहाँ लाठी का सुन्दरतम ईश्वर होना है जिसके रूट को हम लोकेट कर सकते हैं. लेकिन ईश्वर को पिता की दृष्टि में कैसे लोकेट करेंगे जो अपने अनुभव में जीवन के आखीर तक यह नहीं जान पाते कि वह आखिरकार किस कोठ की लाठी है! लाठी के प्रति वो शंकालु कहाँ है? यह बात उसके अवचेतन में है कि ठीक उसकी ही तरह यह लाठी भी जर्जर हो रही है और वह भी इसलिए कि मर्त्य जीवन की रागमयता उसे उस वस्तु से जोड़ती है जो उसके जीवन के बेहद करीब है - ईश्वर के विकल्प के रूप में! जागरण में जितना विश्वास उसे अपने प्रति है उतना ही लाठी के प्रति भी! इसमें एटर्नल नहीं क्षणभंगुर चीजों पर विश्वास है - उनके होने पर भी और न होने पर भी.
Post a Comment