कविता का परिवेश
रघुवंशमणि
जिस दौर में आज हम कविता की चर्चा कर रहे हैं वह सापेक्षित दृश्टि से तेज परिवर्तनों का समय है। जो परिवर्तन पहले सौ-पचास सालों में होते थे अब वे दो-चार सालों में सम्पन्न हो जाते हैं। आज हम जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रह रहे हैं, शयद उसकी कल्पना हम स्वयं 1970 के आसपास नहीं कर सकते थे। तकनीकी के तीव्र विकास ने जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये है। 1970 के आसपास गॉवों तक ट्रांजिस्टर/रेडियो की भी पहॅुंच नहीं थी। आज वहीं पर विभिन्न मीडियारूप अपने विभिन्न लुभावने रूप-रंगों के साथ पहुँचे हुए हैं। सूचना क्रान्ति ने लोगों को छपे शब्दों के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे साधन दिये हैं जिनकें द्वारा अभिव्यक्ति और संप्रेशण संभव हुए हैं। ऐसे में निष्चित रूप से कवित की हमारे समय में अवस्थिति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। यह मुद्दा हमें स्वाभाविक रूप से कविता की भूमिका से लेकर, कविता की आलोचना और मूल्यांकन के प्रष्नों तक ले जायेगा।
प्रत्येक काल में लोग अपने समय में होने वाले परिवर्तनों के प्रति इस प्रकार की बातें करते रहे हैं। प्रेमचन्द ने भी अपने समय में हो रहे सापेक्षिक रूप से तेज परिवर्तनों की बात की थी। हर युग के विचारषील लोगों को अपना समय पिछले कालों से अधिक तेज परिवर्तनों वाला लगा है। लेकिन यह एक तथ्य है कि विगत बीस-तीस वर्शों में ही परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं कि पिछले समय से गहरा अलगाव महसूस हो। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है इसके भौतिक प्रमाण मौजूद हैं। रेडियो, ट्रांजिस्टर से टी.वी., आकाषीय चैनल, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, टेलीफोन की भौतिक उपस्थिति इसके कुछ प्रमाण है। पारंपरिक मीडियारूपों में भी रूपगत परिवर्तन स्पश्टत: दृश्टिगोचर हुए है। इसी कारण हमारे इस दौर के परिवर्तनों को अभूतपूर्व कहा जा रहा है। यह बात दीगर कि आने वाले समय में परिवर्तन और भी तेज हों, और हमारे बाद की पीढ़ी को हमारा ही समय पिछड़ा हुआ लगे। यह भी संभव है कि ये परिवर्तन किसी ऐसी दिषा मेें फैले कि जीवन षैली पर इसका सीधा प्रभाव कम रहे और आने वाला जीवन इतनी उथल-पुथल से न भरा हो। कुछ लोग इस दौर को संरचनात्मक समायोजन के संक्रमण काल के रूप में भी देखते हैं जिसमें परिवर्तन तेज गति से होते हैं। इस संरचनात्मक समायोजन के बाद संभवत: इस परिवर्तन की गति थोड़ा मंद हो।
फिलहाल विभिन्न मीडिया रूपों मेें कविता क्ी उपस्थिति का सवाल काफी परेषान करने वाला हो सकता है। विषेशकर यदि हम उस पारंपरिक रूमानी सोच के तहत कविता पर विचार करना प्रारंभ करें जिनके तहत कवि, ' भावी का द्रश्टा' और 'विप्लव का स्रश्टा' होता था; या जो 'षाष्वत मूल्यों' की सृश्टि करता था, अथवा जिसके पास 'ईष्वरीय षक्ति' या 'प्रतिभा' होती थी जो पूर्व संस्कारों से प्राप्त होती थी। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को इस प्रकार के भ्रम न होंगे। तथापि 1970 के दशक में कविता की भूमिका की तुलना में यदि आज की कविता को रखें तो यह भूमिका घटी हुई ही लगेगी। कविता के पाठकों की घटती हुई संख्या निरंतर चिन्ता का विशय बनी रही है। इसी सापेक्ष कविता का प्रभावक्षेत्र भी सीमित हुआ है।
कविता को यदि 'मुफलिसों की अंजुमन' तक न भी पहुंचाया जा सके तो उसे कम से कम 'पढ़ी लिखी जनता' तक तो पहुंचाया ही जाना चाहिए। मगर सवाल यह है कि कविता का माध्यम क्या है? कविता स्वयं तो अपना माध्यम होती नहीं। कविता को यथाषक्ति पाठकों तक पहॅुंचाने का कार्य लघु पत्रिकाओं ने ही किया है। मगर हिन्दी के प्रकाशकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं क्योंकि वे अक्सर लाभ के अर्थषास्त्र के चलते कविताओं को पाठकों तक पहुँचाने के बजाय पुस्ताकालयों तक पहुंचाते हैं। डॉ. मैनेजर पाण्डेय ने ठीक ही कहा है कि हिन्दी के प्रकाशक वास्तव में हिन्दी के अंधकारक हैं। इधर हिन्दी कवियों के कविता संग्रहों के संस्करणों की प्रतियाँ भी काफी कम होती गयीं है। कुछ संग्रहों के प्रकाशन संस्करण 500 प्रतियों तक भी सीमित रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हिन्दी में कविताओं के पाठक कई कारणों के चलते कम हुए हैं।
मेरे एक मित्र अक्सर पूछते हैं कि यदि समकालीन हिन्दी कविता का मामला कुछ हजार लोगोें तक ही सीमित है तो फिर उसे लेकर ज्यादा उछल-कूद करने की क्या जरूरत? अगर कविता क्षेत्र में उठने वाले विवाद कुछ ही लोगों तक सीमित है तो फिर उसे ज्यादा महत्व क्यों दिया जाय? कविता को लेकर उठने वाले और उठाये जाने वाले इस प्रकार के प्रष्न अक्सर सिनिकल/नकारात्मक तरीके से सामने आते हैं और उन पर अंग्रेजी की एक कहावत के अनुसार टब के पानी के साथ-साथ बच्चे को भी फेंक देने का आरोप लगाया जायेगा क्योंकि कविता के पाठक कितनें भी कम क्यों न हुए हों, वह चर्चा का विशय बनी रहती है। समाज के एक संकुल में ही क्यों न सही वह गंभीरतापूर्वक समझी जाती है। लेकिन इस तर्क को कविता के पक्ष में आत्ममुग्ध तरीके से या 'संतोशधन' के रूप में नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए।
कविता की इस भौतिक स्थिति के प्रति चिन्ता ऐसा नहीं है कि हिन्दी जगत में व्यक्त नहीं हुई । आलोचकों में तो यह चर्चा रही ही, इसके प्रति कवियों में भी एक सजगता दिखाई देती है। अश्टभुजा षुक्ल और संजय चतुर्वेदी जैसे कवियों ने अपना रास्ता बदलकर नयी षैली अपनायी जो जनसामान्य के लिए ग्राह्य हो। जनगीतों के मार्ग तो प्रषस्त ही रहे। नयी कविता की कठिन और दुर्भेद्य षैली की तुलना मे समकालीन हिन्दी कविता सरलता की ओर बढ़ी है। अज्ञेयवादियों की षैली की तुलना में आज की कविता की षैली काफी सरल है। मगर कविता से कम सम्पर्क रखने वाले लोगों में कविता की कठिनाई का मिथक लगातार बना हुआ है। इसका एक बड़ा कारण यही है कि कविता को पढ़ी-लिखी हिन्दी जनता तक व्यापक रूप से पहुंचाने का कोई प्रभावी और व्यापक माध्यम नहीं है। कविता को जनता तक पहुंचा सकने वाले मंचों का अभाव है। इन प्रष्नों के खड़े होने पर हमेषा एक नवजागरण्ा की माँग की जाती है और हिन्दी जनता को कोसा जाता है। लेखक संघों और साहित्यिक संस्थाओं की गंभीर भागीदारी हो सकती है। जनसंस्कृति मंच के कुछ कवियों ने 'युध्द के विरुध्द कविता' के तहत कुछ समयपूर्व ऐसा प्रयास किया था जो सफल भी था। कई अवसरों पर कविता को लेकर जब भी जनता में जाना पड़ा है तो देखा गया है कि उसका प्रभाव अब भी काफी है। कविता को जनता के बीच ले जाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत है।
(2)
कविता के लिए जैसी भी भौतिक परिस्थितियां हैं उन्हीं के तहत समकालीन हिन्दी कविता को देखना होगा। कविता का यह भौतिक यथार्थ कविता की भूमिका के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। हिन्दी कविता कम लोग पढ़ते हैं इस तथ्य से ही कविता की सीमा को निर्धारित करना फिर भी खतरनाक होगा। कविता के लक्ष्य पाठकों की चर्चा में भी यह तथ्य नहीं भुलाया जाना चाहिए कि कविता के पेषेवर आलोचकों और नियमित पाठकों के अतिरिक्त एक यादृच्छिक पाठक वर्ग भी रहता है जो हमेषा महत्वपूर्ण होता है। फिर मुक्तिबोध के जनता के साहित्य के बारे में व्यक्त यह विचार नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जनता के बारे में लिखा गया साहित्य भी जनता का ही साहित्य है।
इन सारे द्वन्द्वों के बीच मुख्यधारा की कविता की बात बिडम्बनापूर्ण लगती है क्योंकि समकालीन हिन्दी कविता स्वयं मुख्यधारा से अलग हैं। मुख्यधारा में तो फिल्मी गीत, ग़जलें और बाजारू संगीत आयेगा जिसका धन्धा अभी भी लाभप्रद है। हिन्दी में कविता लिखकर यष:प्रार्थी तो हुआ जा सकता है पर धनपषु नहीं। समकालीन हिन्दी कविता (जैसा कि बार-बार कहा जाता रहा है) प्रतिरोध और विकल्पों की कविता है और विकल्पों की यह तलाष जारी रहनी चाहिए क्योंकि इन विकल्पों के ठोस, सार्थक और परिवर्तनकारी रूप अभी समाज/संस्कृति में दिखलाई नहीं पड़ते। समकालीन हिन्दी कविता विभिन्न संस्तरों पर लिखी जा रही है और विभिन्नताएं ऐसी हैं कि किसी भी आलोचक को परेषानी में डाल दे। ये कविताएँ अपने वर्चस्व विरोध और सत्ताा प्रतिरोध मे ही अपनी इयत्ताा तलाषती है। पूरी कविता के लिए किया गया सामान्यीकरण 'समकालीन' स्वयं में तमाम तत्वों का एक समुच्च है जिसे पारिभाशित करने में सैकड़ों पन्ने काले किये जा चुके है। यहाँ यदि कई पीढ़ियाँ एक साथ सृजनरत हैं तो एक ही पीढ़ी के कई कवि कई-कई तरह से लिख रहे हैं। इसलिए मुख्यधारा का कोई भी सवाल अपने जवाब मे बेहद सामान्यीकृत और भोथड़ा होगा। उम्रदराज होते कवियों जैसे उदय प्रकाश, स्वप्निल श्रीवास्तव, ज्ञानेन्द्रपति, राजेश जोषी और विनोद कुमार षुक्ल मे ही समानता की तलाश कितनी कठिन होगी।
समकालीन हिन्दी कविता का यही वह यथार्थ है जो आलोचकों के लिए एक चुनौती बनता है। कवि की अपनी अवस्थिति कविता मे अन्तर करने योग्य तत्व पैदा कर देती है। गुजरात के दंगों पर राजेश जोषी, देवी प्रसाद मिश्र और विश्णु खरे की कविताएं अपना अलग-अलग स्वभाव रखती है। यहीं पर देवीषंकर अवस्थी का यह कथन सार्थक होता है कि कविता को समाजषास्त्र या राजनीति की ही दृश्टि से नहीं देखा जाना चाहिए-उसका अन्तर्ग्रथन भी अध्ययन की विशयवस्तु है। हिन्दी आलोचना पर ऐसा न करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता । समकालीन हिन्दी कविता की इसी विभिन्नता के चलते आलोचक अपना 'स्टांस' बदलते रहते है।
अक्सर विचार-विमर्ष के दौरान 'मुख्यधारा' पद द्वारा वामपंथ के साहित्य की ओर संकेत होता है। हिन्दी कविता के सन्दर्भ मेंं भी 'मुख्यधारा' पद का यह एक अभिप्रेत हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह इंगित करना जरूरी होगा कि समकालीन हिन्दी कविता को किसी 'वाद' के तहत हो रही कविता नही कहा जा सकता । यह बात दीगर की उद्देष्य की एकता के चलते समानताएँ दिखाई दे सकती है। सरोकार एक जैसे होने पर कविताओं की दिषा एक जैसी हो जाती है। अभी कुछ वर्श पहले 'सहमत' द्वारा प्रकाषित असद जैदी द्वारा सम्पादित 'दस बरस' का संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें अषोक वाजपेयी से लेकर कुंवर नारायण तक की कविताएँ थीं जो स्वयं को वामपंथी कहना पसंद नहीं करेंगे। कुल मिलाकर यह एक प्रजातांत्रिक सहयोग ही है जिसमें तमाम दिषाओं और विचारों के कवि सरोकारों की एकता के चलते एक स्थान पर खडे दिखाई देते हैं। समकालीन हिन्दी कविता से जुड़े इस तथ्य को साम्प्रदायिकता विरोधी हिन्दी कविता के प्रसंग में प्रमाणित किया जा सकता है।
फिर भी इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि आज की हिन्दी कविता अतिषय राजनीतिक है और यह उसकी पहचान का एक प्रमुख तत्व है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में हिन्दी कविता कभी भी इतनी राजनीतिक नहीं थी जितनी की आज है। ऐसे में किसी एक राजनीतिक विचार को (वामपंथ) को मुख्यधारा मानकर कलंकित करना एक तरह का हिन्दुस्तानी मैकार्थीवाद होगा जो कोई स्वस्थ प्रजातांत्रिक बात नही। हिन्दू पुनरुत्थान के दौर मे इस प्रकार की सेंसरषिप के भगवे प्रयास हो चुके ही। यह बताना जरूरी नहीं कि ये सभी प्रयास फासीवाद के ही रूप रहे हैं।
साम्प्रदायिकता के उभार का हिन्दी कविता पर गहरा असर पड़ा। साम्प्रदायिकता विरोधी कविता साम्प्रदायिक फासीवाद के उभार के दौर में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाषित हुई और कुछ पत्रिकाओं ने समय-समय पर इन कविताओं को विषेशरूप से स्थान दिया। चन्दौसी से प्रकाषित होनी वाली पत्रिका 'परिवेष' ने 1992 के बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद अपना साम्प्रदायिता विरोधी अंक ही प्रकाषित किया। इसके बाद से कई पत्रिकाओं ने साम्प्रदायिता विरोधी कविताओं को विषेशरूप से स्थान दिया। इन कविताओं से गुजरते हुए हम हिन्दी कविता में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित कर सकते है। दिसम्बर 1992 से पहले और उसके बाद लिखी गयी तमाम कविताएँ परिवर्तन के दो तथ्यों की ओर संकेत करती है। एक तो यह कि जो कवि पहले से कविताएँ लिख रहे थे उन्होंने साम्प्रदायिकता के प्रष्न को अपने लिए महत्वपूर्ण माना और उन्होंने इस विशय पर प्रमुखता से कविताएँ लिखीं। दूसरा यह कि नये उभरते कवियों ने इस विशय को तत्काल अपनी विशयवस्तु के रूप में चुना। ये कवि इस दौर की उपज थे या थोड़ा पहले से लिख रहे थे। इस क्षोभकारी घटना और इससे जुड़ी साम्प्रदायिक हिंसा ने दोनों पीढ़ियों के कवियों की संवेदना को गहराई से झकझोरा । हिन्दी की समकालीन कविता मे यही वह बिन्दु है जहाँ हम एक विषिश्ट प्रकार के मानववाद की वापसी देख सकते हैं। यह मानववाद, साम्प्रदायिकता का विरोध करने में व्यापक जमीन की प्राप्ति के लिए बना। राजनीति में यदि यह धर्मनिरपेक्ष षक्तियों के ढीले-ढाले गठजोड़ के रूप में दिखायी दिया तो साहित्य में हम इसे मानवीय भूमि पर समेकित होते देख सकते हैं। अषोक वाजपेयी जैसे साहित्य के स्वराज की बात करने वालों से लेकर अतिवाम समर्थकों तक ने इस मुद्दे पर लिखना जरूरी समझा।
(3)
भूमण्डलीकरण और बाजारवाद के विरोध मे हिन्दी मे बहुत सी कविताएँ लिखी गयीं मगर कविता पर उन दोनों आर्थिक परिवर्तनों का कैसा प्रभाव पड़ा यह देखना बाकी है। भूमण्डलीकरण और बाजारवाद ने जिस प्रकार के व्यवसायवाद को बढ़ावा दिया है उसका प्रभाव अब हिन्दी साहित्य पर स्पश्ट परिलक्षित होने लगा है। मूल्यों और नैतिकताओं के स्थान पर अब आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत सम्बन्ध अधिक महत्वपूर्ण हो गये है। सर्जनात्मकता में विष्वास कम और सफलता की सीढ़ियों पर विष्वास अधिक बढ़ा है। पुरस्कार लोभ, व्यक्तिगत राजनीति और जोड़-तोड़ ने हिन्दी कविता जगत मे भी दम मारा है। बाजारवाद के दौर में अवसरवाद तेजी से बढ़ा है। कविता धन तो नहीं मगर यष कमाने का एक आसान जरिया नज़र आने लगी है। इस सन्दर्भ में मैं अपने मित्र अश्टभुजा षुक्ल के एक महत्वपूर्ण लेख 'काव्यम् यशसे' की ओर इंगित करना चाहूंगा जो जयपुर से प्रकाषित होने वाली पत्रिका 'कृतिओर' में छपी थी।
भूमण्डलीकरण और बाजारवाद की एक विषेशता यह भी है कि वह जहाँ भी अवतरित होता है जनान्दोलनों को कमजोर करता है, उन्हें नश्ट करता है। इनके नीच प्रवाह में पतित लोग मूल्यों और विचारों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रचालित होते हैं। हिन्दी कविता में कैरियरिज्म की प्रछन्न प्रवृत्तिा बढ़ती लग रही है जो कि बेहत खतरनाक है। कविता के मूल्यांकन मेें इस ओर आलोचक की दृश्टि जानी ही चाहिए। उत्तार संरचनावादी कृति और कृतिकार को अलग-अलग करके देखने की बात करते हैं और इस सिलसिले में रोलाबार्थ के निबन्ध 'डेथ ऑफ आथर' में व्यक्त विचार सिध्दान्त सूत्र बने।
रोलांबार्थ अपने निबन्ध 'द डेथ ऑफ आथर' में पाठ के लिए लेखक की अनावष्यकता का जिक्र करते हैं और भाशा को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन एक ही समय मे एक ही प्रकार की भाशा में लिखी जा रही रचनाओं की वैचारिक अवस्थितियाँ कैसे निर्धारित होगी यदि रचनाकार के अस्तित्व से इंकार कर दिया जाय। हिन्दी जगत में अभी हम इतने इतिहास विहीन या स्मृतिविहीन नहीं है। समकालीन कविता में रचनाकार के जीवन और उसकी कविता के सम्बन्धों मे प्रामाणिकता की प्राप्ति होगी। इस अर्थ मे हमें रचनाकार को पुनर्जीवित करना पड़ेगा।
साहित्य के इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जब रचनाकार के जीवन ने उनकी कृतियों के अर्थ बदल दिये हैं। रचनाकार का जीवन किस प्रकार उसके साहित्य के मूल्यांकन के लिए एक प्रकार की कसौटी बनता है इसके उदाहरण्ा निराला, मुक्तिबोध जैसे कवि हैं। निराला की महाप्राणता उनके जीवन और कृतित्व दोनों के चलते है। मुक्तिबोध की विपन्नता में भी जाग्रत उनके स्व कें षब्द हमारी आत्मा के गुप्त स्वर्णाक्षर बन चुके है। क्या एजरा पाउण्ड और विन्डहम लीविस को पढ़ते समय उनके फासीवादी जुड़ावों को भुलाया जा सकेगा? पॉल डी मान के अपने सम्बन्ध उनकी आलोचना के छद्मों की पोल खोल देते हैं। क्या अटल विहारी वाजपेयी की कविताओं का मूल्यांकन करते समय यह भुलाया जा सकेगा कि उन्हीं के प्रधानमंत्रित्वकाल में गुजरात के भयानक दंगे हुए जिसका उन्होंने समय रहते षमन नहीं किया?
आज के इच्छाधारी साहित्य और साहित्यकारों के दौर में मेरी बातें कुछ लोगों को थोड़ा पुरानी और घिसी-पिटी लग सकती है। उन लोगों के लिए वीरेन डंगवाल की ये पक्तियाँ छोड़ रहा हूँ।
''मजे का बखत है तो इसमें हैरानी क्या है?
हमें भी कैलेन द्यो कुछ मज्जा परेसानी क्या?''
'कुछ कद्दू चमकाये मैंने'
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


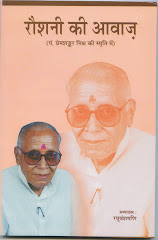


3 comments:
जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ आपका यह लेख किसी पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ है. अगर ऐसा है तो क्या कृपापूर्वक आप पत्रिका का नाम बता सकते हैं?
काफी लंबा लेख है ये खासतौर पर नेट पर पढ़ी जा सकने की सुविधा को ध्यान में रखें तो. पढ़ तो लिया है मैंने लेकिन डूब कर नहीं पढ़ सका!
आपकी ढेर सारी चिंताओं में मैं अपने को साझा करता हूँ. अच्छा लिखा है आपने!!
यह लेख मैं परिवेश में पढ़ चुका था
ब्लाग पर भी देखना इसे सुखद रहा
Post a Comment