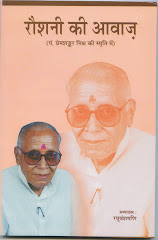आर. के. सिंह की कुछ अंग्रेजी कविताओं के अनुवाद
1.
वह पागल घोषित है
पाॅंव बॅंधे हैं उसके
गली में सरकती है
वह आगे पीछे
नंगी भूखी वह
ठिठुरती है दिसम्बर में
नाली के पास सिकुड़ी
फुटपाथियों की उपेक्षिता
कागज, लकड़ी और चीथड़ों से
आग जलाने की कोशिश है
पुल के नीचे चाय की चुस्कियाॅं लेते
मैं राजघाट की घंटियाॅं सुनता हूॅं
तीर्थयात्री ट्रेन पकड़ने की जल्दी में हैं।
2.
दो सूखे वृक्षों के बीच अनन्त सौंदर्य सी खड़ी
दुपहरी में गुजरतेे मछुवारों को देखती
उसकी आॅंखें भी तो मछलियाॅं हैं
पर परवाह किसे है उनकी
गिरकर शांत होती हैं फड़फड़ाती पत्तियाॅं
लपटों के शांत होने पर देखती है
टीलों के उच्चावच पर अपनी टूटी चूड़ियाॅं
और एक बिलखता गुलाब सफेद साड़ी में
छिपा लेती है वह
3.
चेहरे पर जर्द पर्त
राख में तलाशती अंगुलियाॅं
पिछवाड़े बागान के करीब ही
बिनती हैं जले हुए कोयले
कल का खाना बनाने के लिए
4.
ग्ंगा यमुना का संगम
एक समलैंगिक मिलाप है
सुन्दर परन्तु बंजर
मेरे मित्र को पता है
स्वर्ग का रास्ता
इन सर्पीली नदियों से होकर नहीं जाता
5.
सूरज के फैलते मकड़जाली चक्र मेरे
मेरे अस्तित्व और चीजों को धुंधलाते हैं
सुबह से शाम तक मेरे चारो तरफ
मिथक स्वयं को दोहराता है
मेरे अंदर की उभरती रोशनी
कागजी भगवान का आभामण्डल
चारो तरफ सभी कुछ आन्दोलित करती
जीवन और मृत्यु का समीकरण है
इस वक्त का सशंकित सन्नाटा
षडयन्त्र है एक गंभीर दृश्य को आभामण्डित करने का
भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने में
अंधभावनाओं और लघुदृष्टियों की पूर्णता में
6.
यह नहीं कि कुछ पैसे मैं
रिक्शे पर खर्च नहीं कर सकता
नहीं खरीद सकता कार या स्कूटर
मैं जुड़ा रहा चाहता हूॅं
धरती और धूल से
अपने भार के साथ
अकेले चलना चाहता हूॅं
मेरे कन्धे पर सब्जियाॅं और सामान
चालीस साल पहले जैसी लटकी हैं
सोचता हूॅं बिना किसी शर्म के
स्वाभिमान और पसीने के साथ
दूरियाॅं तय कर सकता हूॅं
और कह सकता हूॅं खुद से
देखो मैं उनसे जुदा हूॅं
पैसे से होने दो उनका मूल्यांकन
जिसको वे अपनी टांॅगों के बीच या सपनोें में
छिपाकर रखते हैं
मुझे मेरे कामों से जाना जाय
मेरी मेहनत से जिसने किसी का अपकार नहीं किया
और कल जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊ
कि खड़ा न रह सकूॅं अपने पैरो पर, चल न सकूॅं
तो याद करूॅंगा कि जमा कर रखे थे मैंने
अपने पैर जमीन पर
और उन सबको जाना था
जिन्होंने बेदिली से अपना हाथ बढ़ाया था
वे किसी को शाप न दें अगर
उनके गिरने पर ध्यान न दे कोई
7.
जब फूल सूख जाएॅंगे
शहद के लिए मण्डराती
मक्खियों को कौन जीवित रखेगा
या उन हाथों को महसूसेगा
जो नारंगी के बागों में लगे
छत्तों को संवारते हैं
वे तब मिलकर
अपने स्वर्णिम दिनों को
याद कर सकती हैं
या इस टोने को
खत्म करने के लिए
कोई राग गुनगुना सकती हैं
या जिस भी वजह से
धुवांसे सन्नाटे में
उनका छत्ता जला हो
लेकिन पता है मुझे अब
मधुमक्खियाॅं नहीं लौटेंगी
नग्न वृक्षों की ओर
8.
जाति बदलना संभव न था
उसने अपना धर्म बदल डाला
फिर भी वे न बदले
न ही बदली उनकी संकीर्ण दुनिया
भेड़िये, लोमड़ी और कौए
उस प्रबोधन की परेशानी को
न बदल सके आसमान के साथ
जो देवताओं का पर्दा है
पिंजरा अभी भी भागता फिरता है
एक पंछी की तलाश में
और वह सूरज की आशा में
अकेली लड़ाई लड़ता है
9.
मौन फुटपाथ है
ध्यानियों की शरणस्थली
दूधिया सन्नाटे में
गुजरती सुन्दरियाॅं
पानी में नग्न होतीं
सिकुड़ती चमड़ी
कार्तिक में गंगा पर
आदि ईश्वर हॅंसता है
उनकी नंगी पीठ के पीछे
घायल कर देने वाली शीत में
ऊॅं वासनाओं के लिए
सुविधाजनक है
और अश्वपति नहीं अब बस
दो श्वेत चन्द्रवृत्तों के पीछे
जेट से भागते लटके हैं वे
10.
इच्छाओं को त्याग दूॅं तो भी नहीं खत्म होता यह सब
दुःख का न होना निर्वाण की कुंजी नहीं
व्यतीत को प्रेम न करने और वासनाओं
और नये मानसिक भ्रमों और भयों के जंजाल में
अहसास की खुजली, बदलती गिरावट
अस्तित्व के द्वीप की धुॅंधलाती रौशनी में
जीवन बस जमता जाता, रुके तालाब की दुर्गन्ध
फिर भी खिलता है आशा का कमल
11.
मैने उपवास नहीं रखा
मेरे लिए नहीं है नौरोज़
न होली ही है
अब मैं हिन्दू नहीं रहा
बहुत पहले इसाइयों ने भी
मेरी आस्था और प्रेम पर संदेह किया था
मुस्लिम इतने कट्टर हैं कि
एक सेकुलर को अस्वीकार कर दें
अब मैं अकेला देखता हूॅं
रंगों की त्रासदी
मैं उत्सव मनाता हूॅं
भिन्नता और आत्मा की स्वतंत्रता का
पर वे मेरे जन्म पर सवाल उठाते हैं
और मुझे ढोंगी बताते हैं
12.
मैं यीशू तो नहीं
पर सूली पर चढ़ने की
पीड़ा समझता हूॅं
एक सामान्य आदमी की तरह
सब झेलता जो उन्होंने झेला था
वही जीवन जीता
कभी विनती करता और रोता
प्रेम के अभाव में भी
आगे अच्छे दिनों की आशा करता
घटती सामथ्र्य, असफलता
बोरियत और अनकिये अपराधों के
दोशारोपणों के साथ
मैं जीसस नहीं हूॅं
मगर मैं सूॅघ सकता हूॅं
हवा में जहर और धुॅंवा
मनुष्यता के लिए अनुभव करता हूॅं
उन्हीं की तरह सलीब ढोता
अपने स्वप्नों को पुनः जीता
मैं यीशू तो नहीं
पर सूली पर चढ़ने का
दर्द समझता हूॅं
13.
यह मकान ढह सकता है कभी भी
इसकी दीवारें फटी हैं
नींव पर दरारें खुली हैं
पर कोई परवाह नहीं करता
वे चुप्पी साधे रहते हैं
सतही चिप्पियों की सुरक्षा में
और धीरज रखने की बात करते हैं
स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं छद्म
अपनी अधमता को रहस्यमय बनाते
विवेक और भविष्य की चिन्ता दबाते
चहारदीवारी के बीच मास्टरों की
चुप्पियाॅं खरीदते
14.
हम कहाॅं पहुॅंचेंगे आखिर
ताबूत में यात्रा करते
या इन्द्रधनुषी सिंहद्वार के परे
लंगर डालने की कल्पना करते
सुनहरी और चमकती राख
मरजीवों को फिर जीवित नहीं करेगी
मिथकों और कहानियों में खोये
हमे वापस लाना होगा
जीवन तत्वों का संतुलन
नये सूरज बनाने के लिए
और चन्द्रमाओं के लिए
गुफाओं को रौशन करेें
जो नये भविष्य की शुरुवात करें
15.
यदि दुनिया नहीं हुई
मेरी नौजवानी की सोच जैसी
तो मैं क्या करूॅं। मैं था
निर्भर अपने पिता पर
स्वनिर्मित मैं
धाराओं के विरुद्ध पढ़ न सका
आसमान और उसके मजबूत इलाकों को
गंगा की बालू पर बने निशान
इन्द्रधनुष की तरह धुॅंधला गये
समय की बरसात
पैरों में चुभती है
दाॅंत के खोड़र
और अंधत्व करते हैं आक्रान्त
और कामचिन्ताएॅं सताती हैं
निद्रा और स्वप्नहीन रातों को
मेरे गंजे होते सिर के गिरते बाल
उस हॅंसी को प्रतिबिम्बत करते हैं
जिन पर अब ध्यान नहीं देता
अब मैं नहीं करता
चालाक और अविश्वसनीय
मित्रों को बेपर्दा
अपने अस्तित्व और भविष्य
पर खीजता नहीं और
प्रभाव नहीं बना पाता
फिर भी सुनिश्चित है जब मैं विराम लूॅंगा
तो बहुत बुरा तो नहीं रहेगा
मेरी दृष्टि फिर भी रहेगी ठीक
ताजी हवा में साॅंस लेता रहूॅंगा
16.
अकेले में रहना
द्वीप बनाता है
घुलती मिलती परछाइयों को
पानी में देखना
पुनर्मिलन की आशा जगाता
तारों के टूटने पर
ज्वार की तरफ आॅंख मूदकर
नया झूठ बुनना है
17.
फौलादी बहाव के साथ
बहता हुआ पानी
पत्थर को भेदता है
उन्हें सितारों की शक्ल देता
सूरज और चाॅंद भी नहीं पा सकते
वैसा तीखापन
चट्टानों का विलाप
बदलता है नदी के गीत में
18.
क्या वे स्वयं को या अपनी सच्चाई को
देखते हैं अन्तर्दर्पण में
बहुत घृणा और क्रोध उपजाते
मनुष्यों और घरों को जलाते हैं
कुछ नहीं सीखते कभी मगर
साम्प्रदायिकता का पत्ता फेकते, अधिकारों के लिए
जो किसी ईश्वर ने नहीं दिया उन्हें। उनकी
अधम राजनीति सन्नाटे की विकृति है
अंग्रेजी से अनुवाद रघुवंशमणि
.......................... ........................... .