डायरी
शान्ति की मीनार पर मंडराती चीलें
इधर फिल्म परजानियाँ देखने का अवसर मिला। यह फिल्म तो काफी पहले आ चुकी थी, मगर मैं इसे देख नहीं सका। कुछ तो इस कारण की मेरे नन्हे शहर फैज़ाबाद में यह फिल्म लगी नहीं। फिर इसका काम्पैट डिस्क उपलब्ध नहीं हुआ। हिन्दी के युवा कवि और मेरे मित्र भाई विशाल श्रीवास्तव के सौजन्य से जब इस फिल्म की डी.वी.डी. प्राप्त हुई तो देखने का मौका मिल ही गया। इधर आयी तमाम फिल्मों की तरह यह फिल्म भी अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का मिला जुला काम है।
यह फिल्म गुजरात के दंगों पर आधारित होने के नाते चर्चा में रही और जब इसे देखने का उपक्रम कर रहा था तो यह बात दिमाग में थी कि कहीं बाम्बे जैसी मसालेदार फिल्म न देखने को मिल जाय जिसमें दंगों की कुछ क्लिप्स का इस्तेमाल करके राट्रीय एकता का पाठ पढ़ा दिया गया हो। मगर आखिर मणिरत्नम और इस फिल्म के निर्देशक राहुल ढोलकिया में कुछ तो फर्क होगा ही। फिल्म ने निराश नहीं किया। फिल्म की कहानी इसे मेलोड्रामेटिक होने से बचा लेती है। कहानी के केन्द्र में मुस्लिम समुदाय न होकर पारसी समुदाय है जो मुस्लिम लोगों के बीच रहता है। यह परिवार चार सदस्यीय है जिसमें परजान नाम का एक बच्चा भी है। उसके पिता सायरस यानि नसीरुद्दीन शाह हैं जो सिनेमा चलाते हैं। उसकी माँ शहनाज/सारिका है जो घर का काम करती है। परजान की एक मासूम बहन भी है जिसे वह परजानियाँ नाम के जगह के बारे में बताकर खेल खेलता है।
एक बुजुर्ग गाँधीवादी हैं जिनके पास एलन नाम का एक अमेरिकी गाँधी पर शोध करने आता है। वह जबर्दस्त शराब पीता है और गालियाँ बकता है। छोटू अखबार बेचनेवाला। चाय बेचनेवाला आसिफ मुस्लिम है जो कहता है कि बिगड़े नौजवान देश के मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं।
ये सारे लोग गुजरात में होने वाले दंगे से प्रभावित होते हैं। जब दंगा होता है तो सायरस फिल्म चला रहा होता है। वह वापस लौटता है तो पूरा मोहल्ला नष्ट हो चुकता है। भागदौड़ में परजान नहीं मिलता। बाकी सारी फिल्म भर बाप, माँ और बहन परजान को खोजते रहते हैं। उन्हें विश्वास है कि परजान उन्हें जरूर मिलेगा। मगर बाद में यह विश्वास टूटने लगता है। अंत में अपने ख्याल में पिता अपने पुत्र की लाश को टावर आफ साइलेंस पर पड़ा देखता है जिसकी ओर चीलें उतर रही हैं।
फिल्म का एक प्रभावशाली दृश्य वह है जिसमें दंगों के पीड़ित लोग दंगाइयों के डर के मारे बयान नहीं देते। मगर एक बार जब डर टूटता है तो सभी अपने-अपने कष्ट बताने लगते हैं।
फिल्म में नसीरुद्दीन शाह का अभिनय तो प्रभावकारी है ही, मगर ध्यान आकृष्ट करती है सारिका जो लम्बे समय बाद इस फिल्म में दिखाई दी है। भावप्रवण अभिनेत्री होने के बाद भी बम्बई ने सारिका के लिए खराब फिल्में ही दीं। कुछ फिल्मों में तो उसे अंग प्रदर्शन के लिए ही रखा जाता था। कमाल हसन से विवाह के बाद तो वह फिल्म जगत से गायब ही हो गयी थी। मगर लगता है कि अपनी दूसरी पारी में वे कुछ अच्छी फिल्में देंगी। फिल्म की कहानी और कहानी के साथ निर्देशक का वर्ताव ऐसा है कि यह एक सीधी सपाट प्रचार फिल्म न बन कर मानवीय पीड़ा का एक वृत्तांत बन जाती है।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)





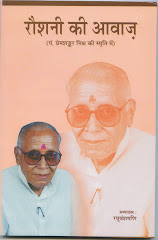





No comments:
Post a Comment