व्याख्यान
समकालीन कविता की भाषा
सम्मानित अध्यक्ष मंडल के सदस्यगण और दोस्तो,
सबसे पहले मैं केदारनाथ अग्रवाल सम्मान समिति के प्रति, और विशेष तौर पर भाई श्रीप्रकाश मिश्र और नरेन्द्र पुण्डरीक के प्रति, अपना आभार व्यक्त करना चाहॅूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ बाँदा के प्रबुध्द श्रोताओं के समक्ष अपने विचार रखने का एक अवसर प्रदान किया है. नीलेश रघुवंशी को केदारनाथ अग्रवाल सम्मान और श्रीराम त्रिपाठी को डाँ रामविलास शर्मा सम्मान प्रदान किये जाने के अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहूँगा.
काव्यभाषा कविता का एक तत्व है, मगर एक मात्र तत्व नहीं। ठीक वैसे ही जैसे भाषा का एक तत्व है भाषा, मगर वह भाषा का एक मात्र तत्व नहीं। जिस प्रकार भाषा के ऐतिहासिक, सामाजिक,और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हैं, वैसे ही काव्यभाषा के भी हैं।
अरस्तू ने साहित्य को शब्दों के माध्यम से होने वाला अनुकरण कहा था तो वह जिसकी अनुकृति है वह भाषा के बाहर ही है, भले ही उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में मात्र भाषा में ही होती हो। यह बात समकालीन कविता के बारे में भी उतनी ही सही है जितनी कि अरस्तू के युग की कविता के बारे में अथवा किसी भी युग की कविता के परिप्रेक्ष्य में। परिप्रेक्ष्य के अभाव में कविता कहाँ खड़ी होगी? शून्य की भीत्ति कोई भी लिखावट संभव नहीं, यह एक कल्पित अवधारणा मात्र हो सकती है।
शास्त्रीय शब्दावली में यह सवाल इस तरह पूछा जा सकता है कि कविता के मामले में काव्यार्थ कहाँ से प्राप्त होता है? निश्चित रूप से समय के परिप्रेक्ष्य ही कविता को अर्थ देते हैं और भाषा का अस्तित्व भी इतिहास और समय सापेक्ष ही है। कविता के सामान्य पाठकों से लेकर विदग्ध आलोचकों तक को 'वाक्' और 'अर्थ' को मिलाकर जिस वस्तु की प्रतिपत्ति होती है उसकी प्रक्रिया का सम्बन्ध इतिहास और समय से अवश्य होता है। 'वाक्' और 'अर्थ' के बीच होता क्या है? किसी पृष्ठ पर अंकित काले अक्षर समकालीन कविता में बदलते ही क्यों हैं? वे किसी और युग की कविता क्यों नहीं हो जाते? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो हमें कविता की भाषा से सम्बन्धित ठोस प्रश्नों की ओर ले जायेंगे। शब्द और अर्थ के बीच ढेर सा व्यापार वह है जिसकी जानकारी हमें कविता की समझ की ओर ले जाती है। अपने समय की घटनाएं, उनका संदर्भ, कवि की उपस्थिति, समाज संस्कृति, राजनीति वगैरह। और यह विश्व परिप्रेक्ष्य हमें कविता का अर्थ अर्जित कराता है।
काव्यभाषा ही वह अन्तिम या सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार नहीं जिसके द्वारा कविता के संघटन को समझने की चेष्टा की जा सकती हो। ऐसे और भी बहुत से तत्व हैं- ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि जिनके अभाव में कविता का संघटन को नहीं समझा जा सकेगा। कम से कम समकालीन कविता के संघटन को तो बिलकुल नहीं। अत: र्सिॅ भाषा के आधार पर कविता के बारे में कुछ कहना उपयुक्त न होगा। काव्य भाषा के अध्ययन को लेकर भी आलोचकीय सतर्कता जरूरी हैं क्योंकि महज भाषा का अध्ययन संभव है कि समकालीन कविता के काव्यार्थ के तमाम महत्वपूर्ण पक्षों से वंचित कर दे। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा इस बात का है कि ऐसा अध्ययन किसी गहरे आलोचकीय पूर्वाग्रहों की ओर लेजाय जो कविता को समझने के सामान्य विवेक को ही धुंधला करे या नष्ट ही कर दे।
इसी कारण काव्य भाषा पर विचार करते समय कविता के अन्य तत्वों का भी ध्यान बना रहना चाहिए जो कविता के अर्थ को अनुकूलित करते हों। इस इतिहासबध्दता से आलोचक का सरोकार होना ही चाहिए खासकर समकालीन कविता के अध्ययन के सिलसिले में बीते हुए समय की कविता का निर्वचन इस इतिहासबद्वतासे परे जाता है तो इसका कारण सीधा यह है कि आज वह अपने तात्कालिक समय से अलग हटकर पढ़ी जा रही है। कविताओं की बदलती व्याख्याएँ स्वयं इस इतिहास बद्वता का प्रमाण हैं।
काव्यभाषा के अध्ययन के सिलसिले में भी यह ऐतिहासिकता देखनें योग्य है। भाषा के अध्ययन के तरीके बदलते रहे हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में गुण, अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि कुल मिलाकर भाषा को ही देखने के तरीके रहे हैं। आज की कविता के लिए, उसके अध्ययन के लिए यदि ये शस्त्र बहुत कारगर नहीं बचे तो उसके ऐतिहासिक कारण हैं। काव्यभाषा के संदर्भ में व्यक्तिगत अभिरूचि के भी तत्व किसी पाठक अथवा आलोचक के लिए महत्वपूण्र् ा हो सकते हैं जिसके उदाहरण मिलते ही हैं। मगर इन तत्वों को एक सीमा से आगे खींचने के अपने आलोचकीय खतरे हैं।
इसी संदर्भ में हम काव्यभाषा के निर्वचन की सापेक्षिक स्वतंत्रता का सवाल उठा सकते हैं। किसी कवि की विशिष्ट भाषा को लेकर विभिन्न समयों या एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार बन ही सकते हैं। कबीर की काव्यभाषा को लेकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार अलग अलग थे ही।हमारे समय में भी एक ही प्रकार की काव्यभाषा को लेकर अलग अलग विचार दिखाई दे सकते हैं।
कविता की सापेक्षिक स्वतंत्रता के साथ कविता के मूल्यांकन की भी सापेक्षिकता दुर्निवार है। यह ऐतिहासिक अनिवार्यता किसी भी प्रकार के काव्य मूल्यांकन की सीमा होगी। सवाल यह उठता है कि ऐसे में एक आलोचक की क्या भूमिका होगी? ऐसे में कविता की आलोचना क्या एक प्रकार का 'डिटर्मिनिज्म' होगी ? मूल्यांकन की सापेक्षिकता मूल्यांकन की सीमा भी होगी । आलोचक की महत्तर भूमिका इस बात मे निहित होती है कि वह कविता के साथ चलते चलते कितना वस्तुनिष्ठ हो सकता है । यहाँ वस्तुनिष्ठता का मतलब उस प्रयोगिक वस्तुनिष्ठता से कतई नहीं जो वैज्ञानिक प्रयोगों में वांक्षित होती है। यह 'डिसइन्टरेस्टेड इन्डिवर' इस बात में है कि आलोचक किसी कृति के पाठ के सिलसिले में उसकी जो पुर्नरचना करता है वह मूल के कितनी करीब है। यह एक आदर्श ही है क्योंकि अक्सर विचारकों / आलोचकों की अपनी अवस्थिति भी उसके पाठ और मूल्यांकन को गहराई से प्रभावित करती है। अक्सर वह रचनाके मूल से निर्वचन की दूरी भी तय करती है।
इस प्रकार विषय और माध्यम के साथ निर्वचन भी उपस्थित होता है और माध्यम की मीमांसा दरकार होती है। भाषा और कथ्य के बीच बनते संबन्ध निश्चित तौर पर अघ्ययन की विषय वस्तु हैं । अत: भाषा का प्रश्न अपनी महत्ता बनाये रखता है। भाषा कविता में सिर्फ विषयवस्तु को पाठक तक पहुँचाने का साधन भर नहीं रहती वह और भी बहुत कुछ उद्धाटित करती है। आलोचक द्वारा काव्यभाषा के अध्ययन का महत्व इसमें निहित है कि वह कविता की रचनाप्रक्रिया और सम्प्रेषण प्रक्रिया में भाषा की भूमिका को रेखांकित कर सके। ऐसी आलोचना प्रक्रिया विश्लेषणात्मक होने के साथ साथ सर्जनात्मक होने के लिए मजबूर है।
समकालीन कविता के संदर्भ में यह मजबूरी ज्यादा बड़ी है क्योंकि यह कविता किसी अखंडता अथवा ऐकांतिकता की अवधारणा में निर्मित न होकर समय के साथ होते संवाद और टकराहट की प्रक्रिया का परिणाम है। इसलिए समकालीन कविता के आलोचक के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वह अपनी व्याख्याओं के लिए मूल कृति के निकटतम रहे। आलोचनात्मक अतियों क िबीच उसे कविता के साथ रहना होगा। जाहिर है कि यह भी आलोचना की स्वायत्तता न होकर उसकी सापेक्षिक स्वायत्तता है। यह अतियों के बीच संतुलन की चेष्टा है जो किसी संवाद की ओर ले जा सकती है। उदाहरण के लिए स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की अतियों के बीच आलोचना की एक सार्थक भूमिका हो सकती है?
भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भाव, विचार अथवा सामाजिक स्थिति की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन इस भाषा के माध्यम को कथ्य से बिल्कुल काटकर अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार कथ्य अथवा विषयवस्तु को माघ्यम से के बिना नहीं जाना जा सकता है, उसी प्रकार माध्यम की उपलब्धि भी बिना विषयवस्तु के कैसे होगी? भषा यदि कविता का फार्म बनाती है तो कन्टेन्ट के बग़ैर वह अमूर्त ही रहेगी। कविता के निर्वचन के लिए दोनों की आवश्यकता होगी। दोनों को एक दूसरे द्वारा ही समझा जा सकता है और हम उन दोनों के द्वारा तीसरे तक पहुँचते हैं। यह तीसरा क्या है? संभवत: यही सारी आलोचना का उद्देश्य है।
आलोचना में विसंगतियाँ अक्सर इसी त्रिकोणीय असंतुलन के कारण होती है। जिन पर कुछ प्रकाश डॉ नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक 'कविता के नये प्रतिमान' में डाला था। (देखें पृष्ठ 102)। नामवर जी का यह ऐतिहासिक विवेचन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह उनका बहुत पहले का विमर्श है। इतने समय बाद उसमें काफी कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है।
फैज़ाबाद में रहने वाले हिन्दी के प्रसिध्द आलोचक डॉ रमाशंकर तिवारी कहा करते थे कि हिन्दी के अधिकांश आलोचक कविता के चारो तरफ तलवार भाँजते हैं। वे कविता के भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं करते हैं। वास्तव में अपने रूपकात्मक वक्तव्य के द्वारा वे इस ओर इंगित करना चाहते थे कि हिन्दी के आलोचक कविता की अंदरूनी संरचना और उसकी भाषिक प्रकृति से दो चार नहीं होना चाहते। यह एक महत्वपूर्ण बात है। भाषा के अध्ययन के द्वारा हम ऐसी चीजों तक पहुँच सकते है, जिन तक कवि के जीवन चरित, उसके परिवेश, और सरोकारों के अध्ययन द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता। इन बाह्य साक्ष्यों का अघ्ययन सरल भी है और इस कारण आलोचकगण सुविधापूर्वक स्वयं को वहीं तक सीमित कर देते हैं। वास्तव में भाषा और कविता के बाह्य साक्ष्यों को एक साथ रखकर ही कविता की एक पूरी समझ विकसित हो सकती है।
कविता के बारे में कोई भी संतुलित निर्णय तभी दिया जा सकता है जब हम भाषा, कथ्य और संदर्भ को एक साथ प्रस्तुत कर सकें। यह निश्चित है कि भाषा के माध्यम से हम कविता के प्रभावशाली होने अथवा न होने का मूल्यांकन कर सकते हैं। भाषा के तत्वों द्वारा ही हम कविता में उपस्थित कवि के अनुभव की सही व्याख्या कर सकते हैं। उसकी शक्ति को भी सही-सही माप सकते हैं। कवि की अवस्थिति को भी इसी प्रकार पुष्ट किया जा सकता है। मगर यदि यह सब कथ्य और सन्दर्भ को त्याग कर भाषा अध्ययन की ऐकांतिकता में होता है तो उसके खतरे बने रहते हैं।
अज्ञेय ने तारसप्तक में अपना एक प्रसिद्व वक्तव्य दिया था कि कविता ही कवि का परम वक्तव्य है। कवियों के लिए इसका कुछ भी अर्थ रहा हो, आलोचना के लिए इसका सीधा अर्थ यह निकलेगा कि कविता से ही कवि की ओर यात्रा होनी चाहिए, न कि कवि से कविता की ओर। अर्थात कविता के अध्ययन में भाषा की सर्जनात्मकता महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थनिष्पत्ति का वह प्रस्थान बिन्दु है। लेकिन इस सिध्दान्त की अति ने रचना के क्षेत्र में रहस्यवादी भाषा को प्रश्रय दिया। आलोचना में इसकी अति ने रूपवाद की ओर उन्मुख किया जिसके अन्तर्गत 'कविता का व्योम' और 'व्योम की कविता' जैसी संरचनावादी टीपें प्रचलित हुईं। रचना के मामले में भाषा के अभिनव प्रयोगों का महत्व कम नहीं होता क्योंकि अक्सर रहस्यवादी लगने वाली भाषा यथार्थोन्मुखी होती है और यह तथ्य आलोचना के सामने चुनौती बनती है। केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी और यहाँ तक कि देवीप्रसाद मिश्र तक की कुछ कविताएँ भाषा के स्तर पर सरलीकृत आलोचना के लिए खतरा पैदा करतीं हैं। मुक्तिबोध की कविताओं को लेकर तो आलोचकीय गलतफहमियों ने जोरदार बहसों को जन्म दिया ही था।
आलोचना का भाषा से जूझना एक बात है और भाषा तक सीमित रहना बिल्कुल दूसरी बात। पहली क्रिया द्वन्द्वात्मकता कि ओर ले जाती है और दूसरी स्वांतर्ग्रथित सरंचनावाद, कलावाद अथवा रूपवाद की ओर। हिन्दी आलोचना का यह सौभाग्य ही है कि मदन सोनी और वगीश शुक्ल जैसे चन्द आलोचकों को छोडकर हमें ऐसे कम ही आलोचक मिलते हैं जो इस दिशा में प्रवृत्त हुए। रचना के संदर्भ में यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि नयी भाषा का अन्वेषण, नये अनुभवों या नई वास्जविकताओं की ओर जाना भी होता है और नये गीतों को नये वाद्ययंत्रों की आवश्यकता होती है। समकालीन कविता की एक सीमा यह है कि अक्सर पुराने अनुभवों को दुहराकर सुविधाजनक कविता बना ली जाती है और कवियों की भाषा एक जैसी लगती है। अक्सर कोई विषय या कोई खास तरह का फार्म अथवा किसी खास तरह की भाषा प्रचलन की तरह आती है और परिदृश्य को उबाउ बना देती है।
काव्यसंदर्भ अक्सर काव्यभाषा के साथ मिलकर नया अर्थालोक पैदा करते हैं। यह बात सिर्फ भाषा को पकड़ने से नहीं समझ में आती। उदाहरण के लिए स्वप्निल श्रीवास्तव की कविता साधु में भाषा के प्रयोग को शब्दों की प्रकृति में नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकी भाषासीधी खड़ी बोली ही है। मगर परिप्रेक्ष्य का आश्रय लें ता ेयह ऐसी अभिव्यक्ति भंगिमा को लेकर आती है जो आध्यात्मिकों की है जो संसार को मायाजाल समझते हैं। मगर कविता की विषयवस्तु है विस्थापन और यह स्वयं में ऐसे काव्य संदर्भों को लेकर चलती है जिसके चलते भाषा में नया रंग उभरता है। इस कविता की संरचना अपने संदर्भ के चलते दूसरी तरह से पाठक में उतरती चलती है। कविता का अलग प्रभाव इस प्रकार का है कि विस्थापन की विषयवस्तु से आगे निकलकर कविता व्यापक प्रश्नों को घेरती है।
'साधु
पृथ्वी से विदा हो रही
है शान्ति
आसमान से रंग
जमीन से गंध
-----------
बुरे लोग प्रतिष्ठित हैं
अच्छे लोग दुखी और संतप्त'
बेहद राजनीतिक कविताओं के इस दौर में यह ध्यातव्य है कि किस प्रकार एक कवि अपनी कविता की भाषिक संरचना से एक जैसी लगने वाली भाषा को बिल्कुल ही नया शेड देता है और प्रभावशाली शिल्प निकाल लेता है। 'साधु' कविता में न केवल संतों की भाषा है बल्कि डामेटिक मोनोलॉगके शिल्प में दूसरे भावों का भी आत्मभाव है जिसके लिए कभी परकाया प्रवेश जैसे रहस्यमय पद प्रयुक्त होता था। यदि स्वप्निल की कविताओं में जड़ से उखड़े और गायब होते लोगों की दुनियॉ के पीड़ाजनक अनुभव हैं तो वे दूसरे के दर्द को आत्मसात कर पाने के कारण है जो कवि में 'सफरर' अर्थात दुख झेलने वाले को सर्जक से अलग करती है। ऐसा अलग होना गहरी संपृक्ति के बाद ही संभव है।
इसी प्रकार की सर्जनात्मक दूरी को हम एक दूसरी कविता के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं जिसकी भाषा दिखने में समकालीन कविता में सामान्यत: प्रयुक्त होने वाली भाषा से बिल्कुल अलग न होते हुए भी अपना अलग प्रभाव रखती है। यह कविता भी डामेटिक मोनोलॉग के शिल्प में है लेकिन यह एक बच्चे को जन्म देती मजदूरनी को संबोधित है। 'बाई दरद ले' शीर्षक इस कविता में कवि ऐसी मजदूरनी को संबोधित करता है जिसके नसीब में 'पत्थर तोड़ने वाले दिन थे' अब वह वलात्कार के बाद माँ बनने जा रही है।
'बाई! तुझे दरद लेना है
जिन्दगी भर पहाड़ ढोये तूने
मुश्किल नहीं है तेरे लिए
दरद लेना
जल्दीकर होश में आ
वरना उसके सिर पर जोर पड़ेगा
पता नहीं कितनी देर बाद रोए
या न भी रोए
फटी ऑंख से मत देख
भूल जा जोर जबर्दस्ती की रात
अंधेरे के हमले को भूल जा बाई'
आगे यह कविता बताती है कि स्त्री का धर्म बरदाश्त करना है। पृथ्वी कितना दर्द सहती है, तभी सब कुछ हरा भरा रहता है। 'आकास पाताल में अट नहीं सकता / इतना है औरत जात का दुख'। स्त्री जाति की सीता ने कहा था कि धरती फट जाय। कविता की भाषा में खड़ी बोली के बीच बीच में देशज शब्दों के प्रयोग बेहद प्रभावशाली हैं। वे हमें शिष्ट और सामान्य स्त्री दोनों के अनुभव जगत में ले जाते हैं। सीता का संदर्भ स्त्री के दुख को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। यहाँ सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि उसका परिप्रेक्ष्य भी 'भावार्थ' की ओर ले जाता है। आलोचकगण इस घिसे पिटे शब्द के प्रयोग के लिए मुझे क्षमा करेंगे। फिलहाल कविता की अंतिम पंक्तियाँ :
'बाई! दरद ले
सुन बहते पानी की आवाज
हाँ ऐसे ही देख उपर हरी पत्तियाँ
सुन उसके रोने की आवाज़
जो अभी होने को है
जिन्दा हो जायेगी तेरी देह
झरने लगेगा दूध
दो नन्हे होठों के लिए
बाई! दरद ले'
चन्द्रकांत देवताले की इस कविता में व्यंग्यार्थों के इतने शेड्स हैं कि गिनना कठिन। क्या यह कविता सिर्फ को सम्बोधित है? फिर कविता की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग भर कितने संस्तरों पर अथोत्पत्ति करता है? धरती पर जीव का आना सृष्टि है और असके लिए कवि स्त्री को दुख भूल कर तैयार होने के लिए कहता है। मगर क्या इस नये आने वाले से दुख कम होगा? पीड़ा और दुख में सीझी यह कविता किसी भी स्त्री विमर्श की तेज तर्रार कविता से अधिक प्रभावकारी है। 'बाई ! दरद ले' की पुनरावृत्ति में ही पूरी कविता नयी अर्थकान्ति प्राप्त करती है जिसके कई संस्तर हैं। विवशता है तो रुदन और आक्रोश भी। 'दरद' शब्द भर पूरी कविता को अलग अर्थालोक से भर देता है। यह सब भाषा के उस परिप्रेक्ष्य से संभव होता दिखाई देता है जिसे जीवन में भाषा के प्रयोगों से ही प्राप्त किया जा सकता है।
कविता में भाषा के अभिनव प्रयोगों का यह अर्थ नहीं कि बिल्कुल अलग दिखाई देने वाली भाषा का उपयोग किया जाय, जबर्दस्ती गाँव देहात के शब्द ठॅँस कर नवीनता का बोध कराया जाय। कोई एक शब्द भी कविता को नये भावान्वेषण की ओर ले जा सकता है बशर्ते कवि को उस शब्द के परिप्रेक्ष्य का भान हो और वह उसे सर्जनात्मक रुप देने में समर्थ हो।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)





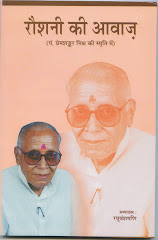





No comments:
Post a Comment