साक्षात्कार
डॉ. रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान से पुरस्कृत युवा आलोचक रघुवंशमणि से योगेश श्रीवास्तव की बातचीत-------------------------------------------------
योगेश श्रीवास्तव: आप अध्यापन के साथ-साथ आलोचनाकर्म से भी गहरे जुड़े हैं, दोनों के बीच एक अदद तारतम्य होता है। उसके बारे में आपको क्या कहना है?
रघुवंशमणि: आप जो बात कह रहे हैं वह सामान्यत: स्वीकृत है। लोग यह मानते हैं कि साहित्य का अध्यापन, आलोचना कर्म में सहायक होता है। यह बात एक हद तक सही भी है। परन्तु हिन्दी क्षेत्र के अधिकांश विश्वविद्यालयों के साहित्य विभागों के पाठयक्रम बहुत ही पारम्परिक हैं जो विद्याथियों में साहित्य की एक रूढ़ समझ पैदा करते हैं। अध्यापकगण इसी पाठयक्रम के प्रसारक हैं और इसी में रचे बसे रहते हैं। इस कारण एक आलोचक के लिए यह पाठयक्रमित ज्ञान महज एक पृष्ठभूमि भर का काम करता है। आगे का रास्ता उसे स्वयं तैयार करना होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।
समकालीनता से संवाद किये बगैर आलोचना में स्वस्थ दृष्टि का विकास संभव नहीं। आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालयों से निकलने वाले लोग बड़ी रूढ़ रचनात्मकता और आलोचनात्मकता के साथ बाहर आते हैं। साहित्य के पारंपरिक अध्ययन से हम केवल साहित्य की परंपरा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मगर एक आलोचक को, या कहिए कि एक रचनाकार को भी, इससे आगे जाना होता है। एक बात जरूर है कि आलोचनाकर्म आपको एक बेहतर अध्यापक बनाता है। अध्यापक ही क्या एक बेहतर नागरिक बनाता है। बस आलोचनाकर्म और जीवन में सचाई होनी चाहिये।
योगेश श्रीवास्तव: आज पत्र-पत्रिकाओं के बीच सार्थक साहित्य के लिए जगह कम हो रही है, आलोचनाकर्म के लिए तो और भी जगह कम हो रही है। ऐसे में आलोचना को लेकर आप क्या सोचते हैं?
रघुवंशमणि: आपने बिल्कुल सही बात कही है। इसका एक कारण तो सीधे-सीधे बढ़ती हुई व्यावसायिकता है। अखबार और पत्रिकाएँ रंगीन हो गयीं हैं और तकनीकी दृष्टि से उन्नत। मगर उनमें प्रकाशित होने वाली सामग्री उसी तुलना में निहायत सतही होती गयी है। होना तो इसका उल्टा चाहिये था। तकनीकी उन्नति के साथ विषय और सामग्री संजीदा होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखबारों में चित्रों को प्रमुखता से छापा जाता है। मतलब आप यह निकाल सकते हैं कि ये अखबार और पत्रिकाएँ देखनें की चीज होते जा रहे हैं, पढ़ने की चीज नहीं। इस तरफ अखबार के मालिकों और सम्पादकों को ध्यान देना चाहिए।
लेकिन ऐसी भी पत्रिकाएँ और अखबार मौजूद हैं जो गंभीर सामग्री प्रकाशित करते हैं। वहाँ आलोचना के लिए अधिक स्पेस है। आपने गौर किया होगा कि हिन्दी में अच्छी आलोचना सामग्री वहीं प्रकाशित होती रही है। इसीलिए साहित्य प्रेमियों और गंभीर पाठकों में लघु पत्रिकाओं का अधिक आकर्षण बना है। लोग उन्हें अधिक गंभीरतापूर्वक पढ़ते हैं। मैं समझता हॅूं कि लधु पत्रिका आन्दोलन का हमारे समय में इसी अर्थ में बहुत अधिक महत्व रहा है। समाज को आलोचना की आवश्यकता पड़ती ही है इसलिये इसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में सदैव बना रहेगा।
योगेश श्रीवास्तव: इधर के आपके आलेखों को पढकर लगता है कि आप माक्र्सवादी आलोचना के प्रभाव में हैं। आप किसी भी पुस्तक को परखने के लिए किन अवधारणाओं और किन प्रत्ययों को लेकर चलते हैं?
रघुवंशमणि: देखिये किसी भी आलोचक को एक खँाचे में बाँध कर देखना उचित नहीं। आलोचना का काम जितना ही खुला रहे उतना ही ठीक। दरअस्ल माक्र्स का मामला यह है कि वह आधुनिक युग के चिन्तन में सूर्य के समान है। हम खिड़की दरवाजे बंद कर लें तो भी सूर्य का प्रकाश घर में घुस ही आता है। मेरे जैसा आलोचक तो खिड़की दरवाजे बंद कर ही नहीं सकता।
एक गैरमाक्र्सवादी निर्देशक और आलोचक पीटर ब्रुक ने लिखा है कि हम माक्र्सवाद से बच ही नहीं सकते क्योंकि जब भी हम साहित्य अथवा साहित्येतर संदर्भ में ऐतिहासिक, आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं, हम माक्र्सवादी हो जाते हैं। यही कारण है कि माक्र्सवाद की चर्चा न करने वाले आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के लेखन में भी हमें माक्र्सवाद के तत्व मिल ही जाते हैं। यद्यपि वे स्पष्टत: माक्र्सवादी नहीं थे। और तो और माक्र्स से पहले पैदा हुए डॉ. जॉनसन की पध्दति माक्र्स जैसी है। माक्र्सवादी चिन्तन पध्दति की व्यापकता बहुत अधिक है।
जहाँ तक मेरा सवाल है मैं माक्र्सवादी चिन्तन पध्दति से बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन रूढ़ माक्र्सवाद से, स्टालिनवाद वगैरह से, मैं दूरी रखता हॅूं। अन्य चिन्तकों को पढ़ते समय मैं दिमाग की खिड़की खुली रखता हूँ।
हर पुस्तक या कृति अपने में एक संरचना होती है जिसके व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक निहितार्थ होते हैं। इसलिए प्रत्येक पुस्तक के प्रति एक जैसे निकष का प्रयोग गलत होता है। मैं आलोचना की एक लचीली पध्दति की खोज में लगा रहता हूँ। मुझे लगता है कि बढ़िया पुस्तकें हमसे अलग तरह से संवाद करती हैं। एक आलोचक को इस संवाद की पध्दति को पकड़ने का प्रयास करना होता है। उक्ति है कि जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो वह भी हमें पढ़ती है। यह रचना की ओर से एक चुनौती होती है एक आलोचक के लिए। अत: पूर्वनिधारित पध्दतियाँ अक्सर बहुत कारगर नहीं सिध्द होतीं।
योगेश श्रीवास्तव: आप कविता के पाठक हैं और आपकी पहचान आरंभ में कवि के रूप में हुई थी। तब इससे इतर आप आलोचना लेखन के प्रति क्यों आकर्षित हुए।
रघुवंशमणि: यह सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं कवि के रूप में ही हिन्दी जगत में पाठकों के समक्ष आया था। अभी भी मैं कभी-कभार कविताएँ लिखता हूँ। वैसे मैं आलोचना कर्म को रचना कर्म का अपवर्जी नहीं मानता। लेकिन आलोचना की ओर आने के कुछ स्पष्ट कारण थे। प्रारंभ में मैं कुछ बढिया कविताएँ, कहानियाँ लिखना चाहता था। इस प्रकार की योजनाएँ मैने बनायीं भी थीं। मेरी कविताएँ कुछ पत्रिकाओं में प्रमुखता से छपी भी थीं। मगर बीच में कुछ ऐसे प्रश्न सामने आये जिनसे जूझना बहुत जरूरी लगा और इसलिए रास्ता बदल गया। साम्प्रदायिक उभार के दौर में वैचारिक प्रतिरोध का कार्य सर्जनात्मक लेखन से ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। यही वजह थी कि वैचारिक गद्य की ओर मुड़ा। फिर मित्रों सम्पादकों ने ऐसा पकड़ा कि कविता की ओर वापस जाना संभव नहीं हुआ। लेकिन इसका पश्चाताप नहीं है। कभी समय रहेगा तो कविता की ओर अवश्य वापस जाना होगा। कविता लिखने का अपना अलग अनुभव होता है। फिर मैं अपनी कविताओं के प्रति बहुत संजीदा हूँ।
योगेश श्रीवास्तव: आपने अपनी आलोचना दृष्टि विकसित करने में समकालीन आलोचना दृष्टि से कितना लिया और उसमें क्या मौलिक जोड़ने का आपका इरादा है।
रघुवंशमणि: मैं समझता हूँ कि समकालीन आलोचना से मेरा संवाद बहुत ज्यादा रहा है। यद्यपि मैं पोलेमिक्स में कम फॅंसता हॅू, मगर संवाद वैचारिक और समझदारी के स्तर पर बहुत ही व्यापक रहा है इससे बिल्कुल इंकार नहीं। डॉ. नामवर सिंह, डॉ. परमानन्द श्रीवास्तव, डॉ. मैनेजर पाण्डेय, जैसे वरिष्ठ आलोचकों की आलोचना से काफी प्रभावित रहा हूॅ। डॉ. रामविलास शर्मा जी अब नहीं हैं मगर वे भी काफी कुछ सिखा गये हैं। कम उम्र के आलोचकों को भी पढ़ता रहा हूँ। समकालीन पश्चिमी आलोचना से भी काफी कुछ मिला है। सब मिलाकर मेरी आलोचना की समझ को आकारित करते हैं। आलोचना की परंपराओं से जो कुछ मिला है उसके बारे में कुछ बता पाना बहुत कठिन है। कुल मिलाकर बहुत कुछ आत्मसात किया है और कभी-कभी लगता है कि अपना कुछ भी नहीं। अज्ञेय ने जैसा अपनी एक कविता में लिखा है कि अपना तो कुछ भी नहीं, या फिर जैसा अरुण कमल कहते हैं कि 'अपनी केवल धार'।
मौलिक जोड़ने का प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है। मै बहुत सोच समझकर और योजनाबध्द होकर कार्य नहीं करता। जो प्रश्न परेशान या उत्तेजित करते हैं उन्ही पर कुछ लिखता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे मनुष्य और सजग नागरिक बनने की ही प्रक्रिया में हमारा लेखन भी होना चाहिये। वह चाहे रचना हो या आलोचना। कुछ लोग लिखते कुछ हैं और होते कुछ और हैं, मुझे ऐसा लेखन समझ में नहीं आता। अच्छा नागरिक या अच्छा मनुष्य होना एक ऐसा वृहत्तर लक्ष्य है जिसके अन्तर्गत ही सब कुछ होना चाहिये। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपना मूल्यॉ।कन पसंद करूॅगा। इसी के पीछे सब कुछ चलना चाहिये। बाकी चीजों को तो समय निर्धारित करेगा। लेकिन यही तो समस्या है कि लेखन और व्यवहार में दो फाँक है। डॉ. रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल इसीलिए प्रेरणास्रोत रहेंगे कि उन्होंने अपने लेखन को व्यवहार का एक हिस्सा बनाकर दिखाया।
मैं टुकड़ों में काम करता हूँ और यह मेरी विवशता है। यदि जोड़ जुड़ाकर कुछ महत्वपूर्ण सामने आया तो आप देखेंगे। आशा है कि मैं समकालीन हिन्दी कविता पर जल्द ही कुछ व्यवस्थित काम प्रस्तुत करूॅंगा। वह मौलिक है अथवा नहीं इसका मूल्याँकन तो आप सब ही करेंगे।
योगेश श्रीवास्तव: आप कवि और आलोचक होने के साथ-साथ अध्यापक भी हैं। अध्यापक की आलोचना दृष्टि स्वत: विकसित हो जाती है। पाठयक्रम को पढाने के लिए तब आप कैसे अपनी स्वतंत्र आलोचना दृष्टि विकसित करते हैं?
रघुवंशमणि: ऐसा सुनिश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि हर अध्यापक की आलोचना दृष्टि विकसित ही होगी। हमारी शिक्षा व्यवस्था में स्वार्थो के इतने फंदे हैं कि आलोचना की ऑंखें फूट जाती हैं, दृष्टि नष्ट हो जाती है। लोग अपने कैरियर को ही सब कुछ मान लेते हैं। परीक्षक बनना, कापी जाँचने की राजनीति करना, नम्बर बढ़वाना, रिश्तेदारों की नियुक्ति कराना, टयूशन पढ़ाना ऐसे कार्य हैं जो आलोचना दृष्टि तो क्या सामान्य दृष्टि को भी अन्धा कर देते हैं। अन्य जगहों पर जो भ्रष्टाचार है वह शिक्षाजगत में भी है। यह भ्रष्टाचार एक ऐसा मायोपिया है जो पूरे समाज को ग्रसता जा रहा है।लोगों को अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में आप ही कहें कि क्या आलोचना दृष्टि विकसित होगी? छात्रों को भी लोग 'इग्जामिनेशन प्वाइंट' से पढ़ाने लगे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अध्यापक की आलोचना दृष्टि स्वत: विकसित होगी, मेरे क्ष्याल से ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, जैसा मैने कहा कि आलोचनात्मक दृष्टि विकसित होने से आप बेहतर अध्यापक हो सकते हैं। आप पुरानी रचनाओं के प्रति भी नई और बेहतर दृष्टि विकसित कर पाते हैं।
योगेश श्रीवास्तव: अंग्रेजी भाषा के शिक्षक होने के नाते अंग्रेजी की आलोचना दृष्टि आपकी अपनी आलोचना पध्दति को कितना प्रभावित करती है?
रघुवंशमणि: विजयदेवनारायण साही कहा करते थे कि अंग्रेजी आलोचना का प्रभाव कम होता है, वह बोझ अधिक होती है। हम अक्सर अंग्रेजी आलोचना को पश्चिमी आलोचना का पर्याय मान लेते हैं जो ठीक बात नहीं है। मैं उस पश्चिमी आलोचना की बात करता हूँ जिसके लिए अंग्रेजी भाषा एक सूत्र का काम करती है। इसीलिए मैने कुछ अनुवाद भी किये हैं जो अब 'समय में हस्तक्षेप' शीर्षक से पुस्तकाकार उपलब्ध हैं। हमें अब पूरी विश्व आलोचना को एक सूत्र में पिरोया हुआ देखना चाहिए। अब हमें आसानी से यह जानकारी मिल जाती है कि दुनिया के किस हिस्से में कैसी आलोचना लिखी जा रही है। इसे तकनीकी ने संभव किया है। इसका परिणाम और प्रतिफलन है हिन्दी में होने वाले अनुवाद। आप देख रहे हैं कि वे प्रभूत मात्रा में उपलब्ध हैं।
अंग्रेजी कवि टी. एस. एलिएट ने कवियों के लिए एक बात लिखी थी कि उन्हें होमर से लेकर अपने समय तक की कविता की परंपरा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। यह बात आलोचकों पर भी लागू होती है। हमें पश्चिमी आलोचना का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन उस परंपरा की अंधभक्ति तो ठीक नहीं। उसके प्रति आलोचनात्मक दृष्टि आवश्यक है। हमें पश्चिमी आलोचना की ओर इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे समाज में पश्चिमी समाज के बहुत से तत्व लगातार आ रहे हैं।
लेकिन मैं यह भी कहूँगा कि यदि हमें अरस्तू से टेरी इगलटन तक की जानकारी होनी चाहिए तो भरत मुनि से लेकर नामवर सिंह तक की आलोचना परंपरा का भी ज्ञान होना चाहिए। अब आप समझ ही गये होंगे कि मेरी आलोचना पर अंग्रेजी आलोचना का कैसा प्रभाव है।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)





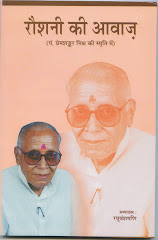





No comments:
Post a Comment