ईश्वर, सत्ता और कविता (4)
बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में ईश्वर के प्रति कविता में भाव बदलते गये हैं। भारतीय जनता पार्टी की धर्म को राजनीतिक हथकण्डे के रूप में अपनाने की नीति का सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ा । आस्तिक लोगों के ड्राइंग रूमों में आशीर्वाद देने की मुद्रा में अनामिका मोड़े खड़े राम के स्थान पर समुद्र को धमकाते धनुङ्ढ हाथ में ताने हुए राम के चित्र दिखाई देने लगे। संघी भाइयों के यहां तो ये चित्र अनिवार्यत: मिलने लगे जिसकी कलाकारी इस बात मे थी कि राम का क्रोध उनकी शक्तिशाली मांसपेसियों में झलकने लगा। भारत के सांप्रदायिक परिप्रेक्ष्य में यह बहुत स्पष्ट था कि 'जलधि जड़' मुसलामान ही थे। अभिवादन के लिए प्रयुक्त होने वाला राम का नाम आक्रामक और हिंसक 'जै श्रीराम' के भयानक उद्धोष मेंं बदल गया। ईश्वर के इस घटिया और स्थूल राजनीतिक प्रयोग ने किसी भी प्रकार के दार्शनिक उदात्ता के लिए स्पेस नहीं छोड़ा।
उत्पात के प्रारंभिक दौर में आयी मानबहादुर सिंह की कविता 'समकालीन ईश्वर की लाचारी' एक दूसरी अवस्थित से लिखी गयी कविता है । इस कविता का रचनाकाल वह समय है जब सांप्रदायिकता की गरज उतनी तेज नहीं थी इस कारण यह कविता अधिक महत्व की हो जाती है । यह कम पढ़ी गयी और लगभग अचर्चित कविता ईश्वर के दुरुप्योग और हिंसा से भरे माहौल में ईश्वर की लाचारी को दर्शाती है। इस मायने में ईश्वर के साथ 'समकालीन' पद का प्रयोग वाकई अर्थपूर्ण है। बाद में लिखी गयी वीरेन डंगवाल की कविता 'दुश्चक्र में स्रष्टा' से इस कविता को मिला कर देखा जा सकता है। यह कविता ईश्वर के पक्ष से प्रस्तुत एक अंधाधुंंध मोनोलाग है या कहें कि विवश ईश्वर का प्रलाप। यहां ईश्वर के मनुष्यता के विरोध में हुए प्रयोंगों को भर्त्सनात्मक ढंग से प्रदर्शित किया गया है।
वीरेन डंगवाल की कविता में 'दुश्चक्र में स्रष्टा' अपनी विडम्बनात्मक अभिव्यक्तियों के चलते महत्वपूर्ण है और इसी कारण उसने हिंदी के पाठकों और आलोचकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। कविता मे उपस्थित यह व्यंग्य और विडम्बना का स्वर कविता के अंत तक पहुंचते-पहुचते आक्रोश में बदल जाता है। 'दुश्चक्र में स्रष्टा' कविता का प्रारंभ भगवान के कारीगरी के कमाल के जिक्र के साथ होता है। समकालीन घटनाक्रम के सापेक्ष यह जिक्र व्यंग्य और विडम्बना के स्वर के साथ है।
'अरे, कुत्ते की उस पतली गुलाबी जीभ का ही क्या कहना!
कैसी रसीली और चिकनी टपकदार, सृष्टि के हर
स्वाद की मर्मज्ञ
और दुम की तो बात ही अलग
गोया एक अदृश्य पंखे की मूठ
तुम्हारे मुखड़े पर झलती हुई'
ईश्वर के शानदार कृत्यों का यह विडम्बनापूर्ण वर्णन इस शिकायत के साथ समय के यथार्थ तक पहुंचता है कि भगवान ने अपना कामयाब कारखाना बंद कर दिया है और अब जो कुछ भी इस तथाकथित ईश्वरीय सत्ता के नाम पर है वह बुरा ही बुरा है। क्या अच्छे और आश्चर्यजनक कार्य सम्पन्न करने वाला ईश्वर कहीं विलुप्त हो गया है? आखिर समकालीन तबाहियों के बीच 'रहमानुर्रहीम' या 'करूणानिधान'ईश्वर के अस्तित्व के कोई चिन्ह क्यों नहीं दिखाई पड़ते?
'बाढ़ें तो आयी खैर भरपूर, काफी भूकंप, तूफान
खून से लबालब हत्याकांड अलबत्ता हुए खूब
खूब अकाल, युध्द एक से एक तकनीकी चमत्कार
रह गयी सिर्फ एक सी भूख, लगभग एक सी फौजी
वर्दियां जैसे
मनुष्य मात्र की एकता प्रमाणित करने के लिए
एक जैसी हुंकार, हाहाकार!
प्रार्थना गृह जरूर उठाये गये एक से एक आलीशान!
मगर भीतर चिने हुए रक्त के गारे से
वे खोखले आत्माहीन शिखर-गुम्बद-मीनार
उंगली से छूते ही जिन्हें रिस आता है खून!
आखिर यह किनके हाथों सौंप दिया है ईश्वर
तुमने अपना इतना बड़ा करोबार?'
वीरेन डंगवाल की यह कविता ईश्वर के अस्तित्व और उसके कार्यों को लेकर प्रचलित मान्यताओं और परंपरागत विचारों से प्रारंभ होकर उन्हीं को प्रश्नांकित करती है।इयवर की अनुपस्थिति इस बात में है कि अब उसका इस विश्व पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।पर सवाल यह हुआ कि यदि इस पर उसका नियंत्रण नहीं तो फिर नियंत्रण है किसका। क्या ईश्वर की कोई वास्तविक सत्ता है भी या यह महज एक परंपरागत असत्य है? क्या ईश्वर नयी क्रूर सत्ताओं सा डर कर भाग गया है? शायद उसका इन क्रूर सत्ताओं से कोई परोक्ष-अपरोक्ष समझौता हो गया हो? कुल मिलाकर कवि के लिए ईश्वर असहनीय हो गया है। यही कानण है कि कविता आक्रोश के ऐसे बिन्दु पर समाप्त होती है जहाँ ईश्वर संबंधी सारी पारंपरिक अवधारणाएँ नष्ट हो जाती हैं।
'अपना कारखना बंद करके
किस घोसले में जा छिपे हो भगवान?
कौन सा है आखिर, वह सातवाँ आसमान?
हे, अरे, अबे, ओ करूणानिधान!!'
युवा कवि पंकज चतुर्वेदी की कविता 'ईसा, बुध्द, हज़रत मुहम्मद के लिए' ईश्वर और पैगम्बरों के नाम पर होने वाली हिंसा और मारकाट का खुलासा करती हुई उसके राजनीतिक प्रयोगों को रेखांकित करती है। भारत ने बुध्द पूर्णिमा के दिन पोकरण में परमाणु विस्फोट किया था तो संकेत का संदेश था 'बुध्द मुस्काराये'। यह विडम्बनापूर्ण संदेश इस ओर ले जाता है कि मनुष्य को नष्ट करने के ङ्ढडयंत्र में ईश्वर का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ ईश्वर की सत्ताा नगण्य है और महत्वपूर्ण है अमरीका, भारत ओर पाकिस्तान की शासन सत्तााएं जो बुध्द, ईसा और हजरत मोहम्मद का इस्तेमाल कर रहे है। यह यूं ही नहीं है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता और इस्लामिक बम के साथ-साथ हटिंगटन की पुस्तक भी आ पहुंची है। धर्म और नस्ल को वैधता देने मे ईश्वर कहीं न कहीं उपस्थित होता है।
ऋतुराज के कविता संग्रह 'लीलामुखारविन्द' में ईश्वर की उपस्थिति अनेक ठोस रूपों में दिखलाई पड़ती है। यह उसका कोई भक्तियुगीन साकार रूप नहीं है, मगर है कुछ वैसा ही। वह कहीं न होते हुए भी सर्वत्र उपस्थित है। सभी प्रकार के पापाचारों में वह शरीक है। यही वह लीला है जो सत्ता और शक्ति के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाकलापों में अन्तर्निहित है। ऋतुराज सत्ता के विभिन्न प्रकार के चेहरों के खेल में उसकी उपस्थिति पाते है- यही है 'लीला मुखारविन्द'। कविता 'ईश्वर चरितम्' में ईश्वर न होते हुए भी परेशानी का कारण है, क्योंकि वह तमाम सत्ता प्रतिष्ठानों और शक्ति केन्द्रों के लिए उपकरण बन गया है। प्रात: काल में बजने वाले भजनों से लेकर रात्रि तक, हर समय उसकी उपस्थिति है।
'हत्यारा हत्या करता है ईश्वर के नाम पर
हत्यारे के पक्ष में ईश्वर गवाही देता है
क्योंकि हर अपराध में उसका हाथ होता है।'
यह सब कुछ होते हुए भी ईश्वर नाम का यह 'मुख्य अभियुक्त अदृश्य' रहता है। इस प्रकार वह निराकार और साकार दोनों है। वास्तव मे यह सत्ता प्रतिष्ठानों का वह वर्चस्वी भ्रष्ट रूप है, जो ईश्वर का इस्तेमाल करता है। यहां ईश्वर तलवार भी है और ढाल भी। और कहीं-कहीं तो वह अदृश्य सत्ताानायक है जो स्वयं ही ईश्वर बन बैठता है। यह विडम्बना ही है। अपने समय के सांप्रदायिक और वर्चस्वी शक्तियाें को देखें तो वे ईश्वर सदृश ही हैं। यह ईश्वरत्व तो धरती पर ही साकार है और उसके ठोस रूप खूंखार और डरावने हैं।
''उनके हाथों में खून सनी छडे थी'
चाकू तेजाब की बोतलें भी
अनगिनत हाथ थे जैसे तुम्हारे ही हाथ हों वे''
'श्री ईश्वरचरितम्' कविता में ईश्वर इतना अधिक है कि कवि की नींद हराम है। वह ईश्वर को कोसता है। उसकी उपस्थिति अमानवीय है। ईश्वर के नाम पर सुबह से ही धूम-धड़ाका है। यह ढोंग तो है ही। अपने कुकर्मों को वैधता प्रदान करने का शक्तिपाठ है। ईश्वर ही वह प्रत्यय है जिसके द्वारा हत्याओं को वैधता दी जा सकती है। ईश्वर अदृश्य मुख्य अभियुक्त है। कविता की विडम्बना इस बात में है कि मुख्य अभियुक्त का दो अर्थ है। एक तो ईश्वर जो दिखाई नहीं देता और चारों तरफ है और दूसरी अर्थ है वह सत्ताा जो हर जगह शक्ति के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करता है। अपने दौर में राम के नाम पर हुए उत्पातों से जुड़ी दक्षिणपंथी शक्ति सत्ताा के सापेक्ष कविता का अर्थ बहुत साफ होता है। ईश्वर, धर्म और सत्ताा के इस क्रूर और अमानवीय गठजोड़ को यह कविता अपनी चिंता का विङ्ढय बनाती है।
सत्तााएं सदैव प्रत्ययों की मदद से शासन करती हैं और उन्हें अपनी वैधता सिध्द करने के लिए इस प्रकार के उपादानों की सदा ही आवश्यकता रहती है। यह किसी धर्म अथवा नस्ल की श्रेष्ठता से लेकर स्वतंत्रता तक का मुद्दा हो सकता है। बुश जैसे सत्तााधीश यदि इराक की जनता को मुक्त कराने के नाम पर आक्रमण को वैधता प्रदान करते हैं तो हिन्दू राष्ट्र और हिन्दुत्व की श्रेष्ठता का मुखौटा सत्तााछद्म पर पर्दे का काम करती है। इसी प्रकार 'देयर इज नो गाड बट अल्लाह' भी अपना काम करता है। ईश्वर सत्तााओं को किस प्रकार से वैधता प्रदान करता है इसका हमारे समय में इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि राम के नाम पर साम्प्रदायिकता के नंगे नृत्य को भी वैधता दी जाय। गुजरात के दंगों को उदार हिन्दुओं की स्वाभाविक प्रक्रिया कह कर बच चला जाय। हिन्दुओं की उदारता भी तो इसी बात द्वारा सिध्द की जाती है कि यहाँ असंख्य देवी-देवता है। अस्ल में इन देवी-देवताओं के पीछे सत्ताा एक ही है जिसके हजारों हाथ कहीं अदृश्य से प्रकट होकर जीवन घुस आते हैं और विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं।
मानववादी कविता से अलग इस नये तौर की कविता दृष्टि की महत्ताा इसी में है कि वह मनुष्य और ईश्वर की सत्ता को एक नहीं देखती। यह ईश्वर की अद्वितीय और सर्वशक्तिमान सत्ताा के प्रति भी मुग्ध नहीं। यह तो और पीछे की बात है। वह दरअस्ल ईश्वर को वर्चस्वी सत्ताा के एक प्रतिनिधि के रूप में देखती है जिसके विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते रहे हैं-खासकर भरतीय राजनीति में।
हिन्दी कविता में ईश्वर के प्रत्यय का यह इस्तेमाल अर्तक्य के विरोध में आता है। हमारे समय में उसकी एक ऐतिहासिक उपस्थिति है जिसे सांप्रदायिकता और फासीवाद के विरुध्द खड़े होते हुए देखा जा सकता है। यही कारण्ा है कि इन कविताओं मेें ईश्वर की चर्चा महज एक दार्शनिक प्रत्यय के रूप में नहीं है। यहाँ वह धर्म के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिफलनों मेें रेखांकित किया गया है। जाहिर तौर पर यह महज एक आस्था का प्रश्न नहीं बनकर रह जाता। इसके विभिन्न आयाम दिखलाई देते हैं। समाज संस्कृति में ईश्वर के प्रत्यय द्वारा एक मनुष्यता विरोधी वर्चस्वी व्यवस्था अथवा सत्ता की स्थापना का यहाँ स्पष्ट विरोध देखा जा सकता है।
प्रकृति और सामान्य जीवन की कविता लिखने वाले नरेन्द्र पुण्डरीक ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार कर पाते क्योंकि वह इश्वरीय सत्ता, आततायी सत्ता की समर्थक है ऐसे में ईश्वर की प्रार्थना के लिए शब्द कहां से आयेंगे।
''कैसे चुपचाप रोज
मेरे सपनों का रौंदता हुआ
आकाश से गुजर जाता है
इन्द्र का हाथी,
बताओ तुम्हारी सरोकारहीन
प्रार्थनाओं के लिए
कहां से जुटाऊं शब्द ईश्वर''
सत्ता और शक्ति के केन्द्र्र ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं और राम लोगों के हृदय से बाहर कैद में रह जाते हैं- अयोध्या को लेकर चलती राजनीति की कैद में। 'कैसे छीने गये राम' कविता में ऐसे विवश और शक्तिहीन ईश्वर का क्या किया जाय। इस फालतू ईश्वर के बारे में यदि जानकारियां हों भी तो किस काम की।
''ईश्वर के पास न कोई हुनर है
न जानकारी
न वह रस्सी बर सकता है
न गांठ सकता है जूते
खटिया बुनना
बर्तन बनाना
मिट्टी तैयार करना
जैसे छोटे-छोटे काम भी
ईश्वर के बस में नहीं थे''
(ईश्वर के बारे में उसके पास पर्याप्त जानकारी थी।)
ऐसे ईश्वर का एक मेहनतकश के लिए क्या महत्व हो सकता है? सत्ता के लिए जो शोषण और उत्पीड़न का शस्त्र है वह आखिर एक मजलूम के लिए कितना अर्थपूर्ण होगाा। जाहिर सी बात है कि वह नकारात्मक ही होगा।
'ईश्वर अन्न के दाने के
भीतर वैठी पाई है
ईश्वर लकड़ी के भीतर
बैठी घुन है'
(जो इस धरती के खिलाफ है)
वह जीवन में संघर्षरत व्यक्ति के लिए भय है जिसका प्रयोग ब्राह्मणवादी पुरोहिती व्यवस्था सदियों से करती रही है। वह सत्ता के तरफ से फैलाया गया 'राज रोग' है। नरेन्द्र पुण्डरीक द्वारा प्रयुक्त शब्द 'राज रोग' के निहितार्थ गहरे और बहुआयामी हैं। अन्तत: ईश्वर वह सब कुछ है जो मनुष्यता के विरुध्द है अर्थात 'जो इस धरती के खिलाफ है।'
नरेन्द्र पुण्डरीक की ईश्वर संबंधी यह कम चर्चित कविता श्रृंखला विचारधारा के मामले में एक गंभीर हस्तक्षेप करती है। वह प्रगतिशीलता के नास्तिक दर्शन के रास्ते को वैसे ही रेखाकित करती है जैसे नागार्जुन की कविता। मगर यह बिल्कुल बदले हुए संदर्भों में ऐसा करती है। सीतामढ़ी के सांप्रदायिक दंगे का जिक्र करती उनकी कविता में ईश्वर निश्चित तौर पर हमारे समय के संदर्भ में हैं। सीतामढ़ी के सामान्य लोगों के सामान्य स्वप्न थे और उनकी इच्छाओं और संघर्षों में ईश्वर कहीं नहीं था।
'फिर भी वे मारे गये
ईश्वर के नाम पर
उनके जलाये गये घर
ईश्वर के नाम पर
ईश्वर जो कभी था ही नहीं
इस दुनिया में
केवल उसके होने को लेकर
क्यों मारे गये लोग''
यहां कविता में उपस्थित सीतामढ़ी भारत का कोई भी शहर हो सकता है और साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने वाले लोग कहीं भी ईश्वर के नाम पर दंगा करा सकते थे। ईश्वर ही उनके लिये वह माध्यम है जिसका इस्तेमाल वे मनुष्य के विरुध्द करते है, सामान्य जीवन का विध्वंस करते हुए।
'कुछ शब्द थे
जो ईश्वर की शक्ल से
बहुत कुछ मिलते जुलते थे
वे उतने ही घृणित
अपवित्र
और धारदार थे
जितना कि ईश्वर
इस वक्त इन शब्दाें से
सीतामढ़ी क्या
तरबूज की तरह
पूरी दुनिया काटी जा सकती है।'
हिन्दी जगत अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में निहायत ही परंपराग्रस्त रहा है। केवल कुछ लेखकों, संस्कृतिकर्मियों के होने से यह सिध्द नहीं होता कि सब कुछ क्रान्तिकारी है। परंपरा अभिविन्यस्त होने में सुरक्षा और मान्यता दोनों मिलती रही है। यही कारण है कि धर्म और ईश्वर की पुनरुत्थानी स्वीकृति यहां की संसदीय राजनीति में प्रतिफलित हुई। ऐसे में ईश्वर की सत्ताा को परंपरा के प्रवाह की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके प्रति शंका, प्रश्न अथवा विद्रोह को परोक्षत: एक पूरी सत्ताा के प्रति होने वाले विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। हिन्दी कविता में इधर उभरते ईश्वर को सिर्फ आज की तात्कालिक सांप्रदायिकता विरोधी राजनीति से अलग एक विशिष्ट ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मेें देखने पर उसका स्पष्ट अलगाव दिखाई पड़ता है। यह बात भी सच है कि इस प्रतिरोध की अपनी एक परंपरा है, ठीक वैसे ही जैसे कूपमंडूकता और जाहिल परंपरावाद की परंपरा है ही। इसी विवेक से जुड़ी प्राश्निकता की यह ईश निन्दक परंपरा रेखांकित करने योग्य है, भले ही यह धारा अल्पसंख्यक और गौण ही क्यों न हो।
ईश्वर और सत्ताा का प्रश्न हिन्दी कविता में विशिष्ब्ट तौर पर सांप्रदायिकता के सापेक्ष ही सामने आया, मगर वास्तव मेें यह सिर्फ सांप्रदायिकता के उभार भर से जुड़ा एक प्रश्न नहीं। यह उस पूरे अतार्किक के विरुध्द आवाज उठाने की बात है जो तरह-तरह से भारतीय समाज में रचा-बसा है। संस्कृति की अनेकों दैनन्दिन की गतिविधियों में यह अतार्किक विद्यमान रहता है और तमाम महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्नों को पृष्ठभूमि में ढकेलता है।
यदि ईश्वर का प्रत्यय हिन्दी के इन कवियों के लिए सिर्फ एक दार्शनिक प्रत्यय नहीं, तो वह राजनीतिज्ञों के लिए जिस प्रकार एक नीतिगत प्रश्न है वैसा भी नहीं। संसदीय राजनीति में धर्म और ईश्वर के कुटिल प्रयोग होते रहे हैं। सांप्रदायिक दक्षिणपंथी दल उसका सीधा इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितो के लिए करते रहे है। यहाँ तक कि टकराव और दंगों के रास्तों को भी नहीं छोड़ा गया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रकरण और गुजरात के दंगों के उदाहरण स्थूल और स्पष्टत: रेखांकित करने योग्य हैं, जिसका विरोध इस दौर की हिन्दी कविता ने जोरदार ढंग से किया। मगर धर्म निरपेक्ष राजनीति ने ईश्वर और धर्म की स्पष्ट आलोचना से बचने का ही प्रयास किया। यहॉ वोट प्राप्त करने के लिए यह एक मजबूरी थी। इस प्रकार के प्रयोग सभी राजनीतिक दलों नें किये हैं बस थोड़ा अलग अलग ढंग से।इस पगकार के 'हितसाधन' या 'स्वार्थसिध्दि' से समकालीन कवियों को कोई वास्ता नहीं रहा है हाँलांकि ऐसे कवियों की कविताएँ निहायत राजनीतिक रही है। यह तथ्य सीधी संसदीय राजनीति और नागरिक जीवन से जुड़ी राजनीति के फर्क को तो साफ रेखांकित करता ही है। कविता के सरोकार के व्यापकतर घेरे बनते हैं। यही कारण है कि कविता भक्तियुगीन सर्वशक्तिमान ईश्वर से मनुष्ब्श् में व्याप्त ईश्वर तक पहुँचकर रूक नहीं जाती। वह ईश्वर के एक छोटे से औजार के रूप् में परिवर्तित हो जाने के तथ्य कोउजागर करती है। इस अर्थ में समकालीन हिन्दी कविता हमारे हिन्दी समाज में छाये एक आध्यात्मिक रहस्यवाद का विखंडन करती है।
''लोग कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर ईश्वर
क्या वह बना सकता है एक ऐसा बड़ा ढोका
जिसे वह दाँत पीसकर स्वयं ही न उठा सके''
Subscribe to:
Post Comments (Atom)





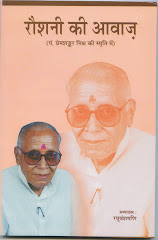





1 comment:
बहुत अच्छा विचारोत्तेजक लेख है. बधाई!
Post a Comment