ईश्वर, सत्ता और कविता
(1)
आपातकाल के पश्चात्, प्र्रकाशित हुए अपने कविता संग्रह 'हजार हजार बाहों वाली' में जनकवि नागार्जुन की एक कविता थी 'कल्पना के पुत्र हे भगवान'। अपने शीर्ङ्ढक को सार्थक करती हुई यह कविता ईश्वर के अस्तित्व पर लिखी गयी उस कालखंड की एक महत्वपूर्ण कविता थी। कल्पनाजनित ईश्वर को संबोधित करती यह कविता कुछ इस प्रकार प्रारम्भ होती है-
''कल्पना के पुत्र हे भगवान
चाहिए मुझको नहीं वरदान
दे सको तो दो मुझे अभिशाप
प्रिय मुझे है जलन प्रिय संताप
चाहिए मुझको नहीं यह शान्ति
चाहिए संदेह उलझन भ्रांति''
आस्था के स्थान पर संदेह की माँग करती यह कविता बेहद चुनौतीपूर्ण है। संग्रह में दिये गये विवरण के अनुसार इस कविता का रचना समय 1946 है। उस समय के पारंपरिक समाज को देखते हुए यह तथ्य इस कविता के ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ा देता है। पारंपरिक तौर पर ईश्वर से होने वाली आस्था की माँग के बरक्स अनास्था की मॉग करने वाली यह कविता एक प्रकार का वैचारिक साहस थी। बरबस ध्यान खींच लेने वाली बाबा की यह कविता या तो आश्चर्य मिश्रित उत्साह के साथ पढ़ी गयी या फिर भयाक्रांत निन्दाभाव से। वह दौर हमारे आज के अभी-अभी गुजरे फासीवादी दौर के दु:स्वप्न से बिल्कुल अलग था, वगर्ना संघी भाई लाठी लेकर नागार्जुन को खोजते और बाबा अपनी खास मुद्रा में कोई अटपटा सा उत्तर देते। फासीवादियों को केवल गर्मी और उत्तेजना से मतलब होता है, जिसे वे विचार के लोहे में ढालकर हथियार के तौर पर जनता में ट्रांसफर कर अपना उल्लू सीधा करते है। उन्हें कविता अथवा किसी भी कला के अर्थ, भाव या अभिव्यक्ति की सूक्ष्मताओं से कुछ खास लेना देना नहीं होता। यदि ऐसा न होता तो वे बर्बर दंगाइयों में क्यों तब्दील होते और पिछले तीस वङ्र्ढों का भारतीय इतिहास आदमीयत के खून से सराबोर न होता।
इस कविता के सिलसिले में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे कविता के पेशेवर पाठकों तक ने उस सूक्ष्मता में नहीं देखा जिस सूक्ष्मता मेें यह कविता अपने पाठ की अपेक्षा रखती है। इसे नागार्जुन की 'प्रतिबध्द हॅू' या फिर 'प्रतिहिंसा स्थायीभाव है' वाली सीधी कविताओं की ही तरह देखा गया। नागार्जुन की यह कविता अपनी अभिधा में ईश्वर को सम्बोधित है जिसको वह स्वयं कल्पना का पुत्र बतलाती है। जिसके अस्तित्व पर ही शंका है या जिसके न होने पर पूरा विश्वास है, उसे संबोधित करने का औचित्य सिध्द करना थोड़ा विचित्र लगेगा। इस कविता के निहितार्थ को कविता की बाद की पंक्तियों में तलाशने पर ही कविता के वास्तविक मंतव्य से मिला जा सकेगा और वह भी कविता के व्यंग्यार्थ में। कविता में 'निन्दा' और 'पाप' करने का जी खोल अभिशाप माँगा गया है। जो सुनिश्चित तौर पर किसी नैतिक वरदान की अभिलाङ्ढा रखने वालों के लिए अच्छा खासा धक्का साबित होगा, पर कविता का वास्तविक केन्द्र वह स्थान है जहांॅ कवि पारंपरिक तौर पर ईश्वर के सामने कान पकड़कर नाक नहीं रगड़ना चाहता।
''बाप-दादों की तरह रगडू न मैं निज नाक
मंदिर की देहली पर पकड़ दोनों कान''
यह साफ है कि यहाँ ईश्वर की सर्वशक्तिमान सत्ता से इन्कार है। नागार्जुन की यह कविता सिर्फ कल्पना सृजित ईश्वर के दार्शनिक विरोध तक ही सीमित नहीं अपितु ईश्वर की अवधारणा से जुड़ी तमाम परंपरागत और अविवेकी बातों का भी प्रतिकार थी जिन्हें आस्था, धर्म और नैतिकता के नाम पर लादा या स्वीकार किया जाता रहा है। ये सभी बातें हमारे समय के मनुष्य को उसकी वास्तविक समस्याओं से दूर ले जाती हैं,
'सड़ गमी है ऑंत
दिखाए जा रहे है दांत''
नागार्जुन समाज में धर्म और ईश्वर के नाम पर पैदा किये जाने वाले भय का प्रतिकार करते है। इस धर्मभीरुता अथवा पारंपरिक कायरता के प्रतिवाद के संदर्भ मे वे धर्म के वर्चस्व को नहीं स्वीकार करते। वे धर्म के इस प्रतिगामी पक्ष की ओर संकेत करते है, जब वे लिखते है कि 'छोड़कर प्रासाद खोजूं खोह/कह रहा है पूर्वजों का मोह'।
इस प्रतिकार भाव को ध्यान में रखें तो यह कविता हिन्दी साहित्य में अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। नागार्जुन की कविता के सामान्य पाठक को भी यह बात अवश्य आकर्ङ्ढित करती है कि वहां व्यर्थ के आध्यात्म के लिए स्पेस लगभग नहीं है। अपने सारे प्रकार-प्रकार के सर्जनात्मक मुद्रा-मुखौटों के उपरांत भी नागार्जुन की कविता विवेक सम्मतता की ही विजय का धर्मनिरपेक्ष उद्धोङ्ढ है। यहां मैं धर्मनिरपेक्षता को महज ईश्वर विरोध तक सीमित करने का कोई उपक्रम नहीं कर रहा। धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित तौर पर एक अधिक व्यापक प्रत्यय है। इतनी व्यापक कि इतिहास के प्रवाह में वह धर्म से लेकर विज्ञान तक में विकसित होती दिखायी दे। यहाँ मैं उस अवस्थिति की चर्चा कर रहा हूं, जो इधर लिखी गयी हिन्दी कविता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और जहां से एक पूरे कालखंड में लिखी गयी ढेर सारी कविताओं का निर्वचन संभव है।
अपनी दूसरी कविता 'थकित-चकित-भ्रमित-भग्नमन' में वे ईश्वर को एक सहारे के रूप में भी स्वीकार करने से इन्कार करते हैं। यद्यपि वे जानते है कि बहुतों के लिए ईश्वर जैसे 'समर्थ' का सहारा स्फूर्ति देता है। फिर वृध्दावस्था के डूबते के लिए तो तिनके का सहारा ही बहुत होता है। वृध्दावस्था में बहुत से प्रगतिशील तार्किकजन ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं, क्योकि बुढ़ापे के कमजोर तन-मन को आस्था का कोई आश्रय चाहिए होता है। इसके अतिरिक्त फिर सुविधा के भी तो अपने तर्क होते ही होते हैं जो मनुष्य को ललचाते हैं।
'सुख-सुविधा और ऐश-आराम के साधन
डाल देते हैं दरार प्रखर नास्तिकता की भीत मेें
बड़ा ही मादक होता है, 'यथास्थिति' का शहद
बड़ी ही मीठी होती है 'गतानुगतिकता' की संजीवनी'
नागार्जुन की यह कविता अपने अंतिम पड़ाव में स्वयं से और अपने जैसे तमाम तार्किकों से यह प्रश्न करती है कि क्या जीवन के अंतिम दौर में उन्हें किसी धार्मिक मठ की शरण लेनी पड़ेगी? इस प्रश्न की भाङ्ढायी नकार और व्यंग में नागार्जुन अपनी स्पष्ट अवस्थिति और दृढ़ निश्चय की ओर ही संकेत करते है।
' तो क्या मुझे भी बुढ़ापे में 'पुष्टई' के लिए
वापस नहीं जाना है किसी मठ के अन्दर '
यह एक रोचक प्रश्न हो सकता है कि क्या नागार्जुन अपनी इस कविता में निराला की अन्तिम कविताओं की ओर संकेत कर रहे हैं जिनमें निराला ईश्वर के प्रति प्रार्थनाभाव की कविताएं लिखते हैं। संभवत: यह नागार्जुन का संकेत नहीं, लेकिन हिन्दी के कई आलोचकाें ने निराला के इस अन्तिम दौर के भागवतवाद पर टिप्पणियाँ की हैं। लेकिन निराला के अन्तिम दौर की प्रार्थनापरक कविताएं इस तरह सरलीकृत नहीं हैं और उनकी जटिलता में निराला के जीवन, उनके नैराश्य, पत्नी प्रेम, मृत्यु छाया और उनका अपना समय परोक्ष पढ़ा जा सकता है। यहां प्रार्थना महज आस्था की अभिव्यक्ति नहीं एक रचना प्रविधि भी है।
नागार्जुन की इस कविता के सापेक्ष हिन्दी की उस पहली दलित कविता का जिक्र जरूरी लगता है जिसमें ईश्वर को 'भगवनवा' कहा गया है, अथवा निराला के उस लघु उपन्यास का जिक्र जिसका नायक ईश्वर पर लाठी चला देता हैं। मगर ये दोनाें ही कृतियाँ नागार्जुन की इस कविता से थोड़ा अलग हैं। हिन्दी की प्रसिध्द ऐतिहासिक महत्व की पत्रिका 'सरस्वती' में प्रकाशित और यहां संदर्भित हीरा डोम की कविता अपने वक्तव्यों में पात्र अथवा कवि की विवशता और शिकायत को व्यक्त करती है जो अपनी जीवन स्थितियों से तंग है। यहां वर्ण व्यवस्था के प्रति आक्रोश पढ़ा जा सकता है । लेकिन देखें तो वास्तव में वही मुख्य बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्याेंंकि वर्ण व्यवस्था के प्रति यह आक्रोश ही उसे उद्वेलित कर ईश्वर की ओर ले जाता है और उसकी लानत-मलामत तक उतारता है। मगर वर्ण व्यवस्था की परिधि से बाहर खड़ा यह डोम ईश्वर की सत्ता से इन्कार नहीं करता। यहां ईश्वर के प्रति निङ्ढेध नहीं अपितु एक विडम्बना पूर्ण और विवश धिक्कार है। महाप्राण निराला की उपन्यासिका में यह प्रतिकिया दूसरे प्रकार की है। मगर दोनों जगह ईश्वर के प्रत्यय को सत्ता से प्रछन्नत: जोड़ा गया है- छल-छद्म और वर्ण व्यवस्था की सत्ताा। हीरा डोम की कविता में तो ईश्वर वर्ण व्यवस्था का पोङ्ढक लगता है। यहां चूकि संदर्भ कविता का है इसलिए निराला की उपन्यासिका का जिक्र छोड़ना पडेग़ा। इस लेख में हिन्दी कविता में ईश्वर के प्रत्यय का प्रयोग निराला के बाद के कवियों ने किस प्रकार किया है और उसके क्या व्यापक निहितार्थ हैं, यही मूल चर्चा का विङ्ढय है। इस प्रश्न के मौजू होने के ऐतिहासिक कारण हैं जो हिन्दी कविता के किसी भी सतर्क पाठक से छिपे नहीं है।
हमारे समय में धर्म का सांप्रदायिक और मनुष्य विरोधी स्वरूप काफी स्पष्ट हो गया है। बीसवीं शताब्दि के आखिरी दशकों से लेकर यदि नयी शताब्दी के प्रारंभिक वङ्र्ढो तक को ध्यान मे रखें तो धर्म को लेकर हुए उत्पातों में जितने निर्दोङ्ढ लोग मारे गये उतने किसी भी प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी मानवीय त्रासदी मेें नहीं मारे गये। यह सांप्रदायिकता विभिन्न प्रकार से उभरी और हिन्दू साम्प्रदायिकता का नग्न नृत्य इसका चरमोत्कर्ङ्ढ है। पंजाब के सिख आतंकवाद, कश्मीर के मुस्लिम आतंकवाद और हिन्दू सांप्रदायिकता की आग में अपनी जान खो देने वाले निर्दोङ्ढ लोगों की संख्या का आंकड़ा रख पाना कठिन है। सिर्फ एक गुजरात के दंगों में 6000 से अधिक लोगो के मारे जाने के आंकड़े है। यह संख्या कम अथवा अधिक हो सकती है और यह बहस का मुद्दा नहीं। मुद्दा यह है कि मनुष्य को सदाचार और मानवीयता का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाला धर्म आज राजनीतिज्ञों द्वारा किस प्रकार इस्तेमाल हो रहा है और धर्म तधा ईश्वर के ठेकेदार किस प्रकार इस अमानवीय कृत्य में लिप्त हैं और किस प्रकार इसे अपना मुद्दा बनाये हुए है। धर्म की राजनीति करने वाले लोग हत्याओं तर्क तलाशने में जुटे हुए है। स्वयं को सहिष्णु बताने वाले धर्मो के इस प्रकार सामने आने वाले हिंसक रूप किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए चिन्ता का विषय होंगें।
'किसी धर्मस्थल के
विवाद में
तीन हजार लोग बम से
दो हजार गोली से
और पाँच सौ
जलाकर मार डाले जाते हैं
चार सौ महिलाओं की
इज्ज़त लूटी जाती है
और तीन सौ शिशुओं को
बलि का बकरा बनाया जाता है
धर्म में
सहिष्णुता का
प्रतिशत ज्ञात कीजिए'
-अष्टभुजा शुक्ल
इस प्रकार की परिस्थितियाें में हिन्दी कविता में ईश्वर के प्रति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखलाई देती हैं। यह ईश्वर ही वह दार्शनिक प्रत्यय है जिसके इर्द-गिर्द धर्म का तानाबाना बुना हुआ है। यही वह दार्शनिक केंन्द्र है जिसके चारो ओर फैला प्रपंच धर्म के नाम पर होने वाली तमाम अमानवीय गतिविधियों को वैधता प्रदान करता है। एक प्रकार से यह सांप्रदायिकता को भी वैधता प्रदान करने वाला आधार है जिसकी जन्मभूमि के विवाद को राजनीतिक सीढ़ी बनाकर भाजपा के लिए केंद्र की सत्ता पर आसीन होना संभव हुआ। यह महज एक इत्तिाफाक नहीं कि ऐसे समय में ऋतुराज अपना संग्रह 'लीला मुखारविंद' उन नास्तिकों को समर्पित करते हैं जो ईश्वर अथवा धर्म में विश्वास नहीं करते मगर जो मनुष्यता के सुखद और बेहतर भविष्य के लिए संघष्र् ारत हैं, 'जो बिना निराश हुए अपने विवेक की दृढ़ता मेंं साहसपूर्वक संघष्र् ारत है। मानव जाति का सुखमय भविष्य ही जिनका परलोक है।' वैसे भी देखे तो इधर धर्म ओर नस्ल के नाम पर पूरी दुनिया में इतने दंगे और खून खराबे हुए हैं कि नीत्शे का यह वाक्य प्रासंगिक लगता है, ' ईश्वर मर चुका है और मैंने उसे दफन होते हुए देखा है.' ऋतुराज की तरह हर संवेदनशील और विवेकवान व्यक्ति इस साम्प्रदायिक उन्माद और उसके फासीवादी विस्तार के दौर में ईश्वर प्रत्यय और उससे जुड़े धर्म के हत्यारे प्रयोगों को प्रश्न के घेरे मेें रख सकता है। यदि इस दौर का सांप्रदायिक अमानवीय धर्म ही बचा है, तो इस धर्म के रास्ते पर न चलना ही वास्तविक धर्म होगा।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)





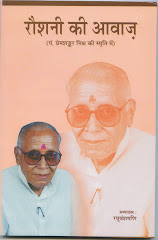





1 comment:
सभी धर्मों का नाश अवश्यंभावी है। बृहस्पति के अनुसार जो पैदा हुआ है वह मरेगा। धर्म भी मानव समाज के विकास की किसी न किसी अवस्था में उत्पन्न हुए हैं। उन का नाश कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह वृद्धावस्था में मनुष्य स्वयं भी कष्ट पाता है और औरों को भी देता है वैसा ही आचरण धर्म कर रहे हैं।
Post a Comment